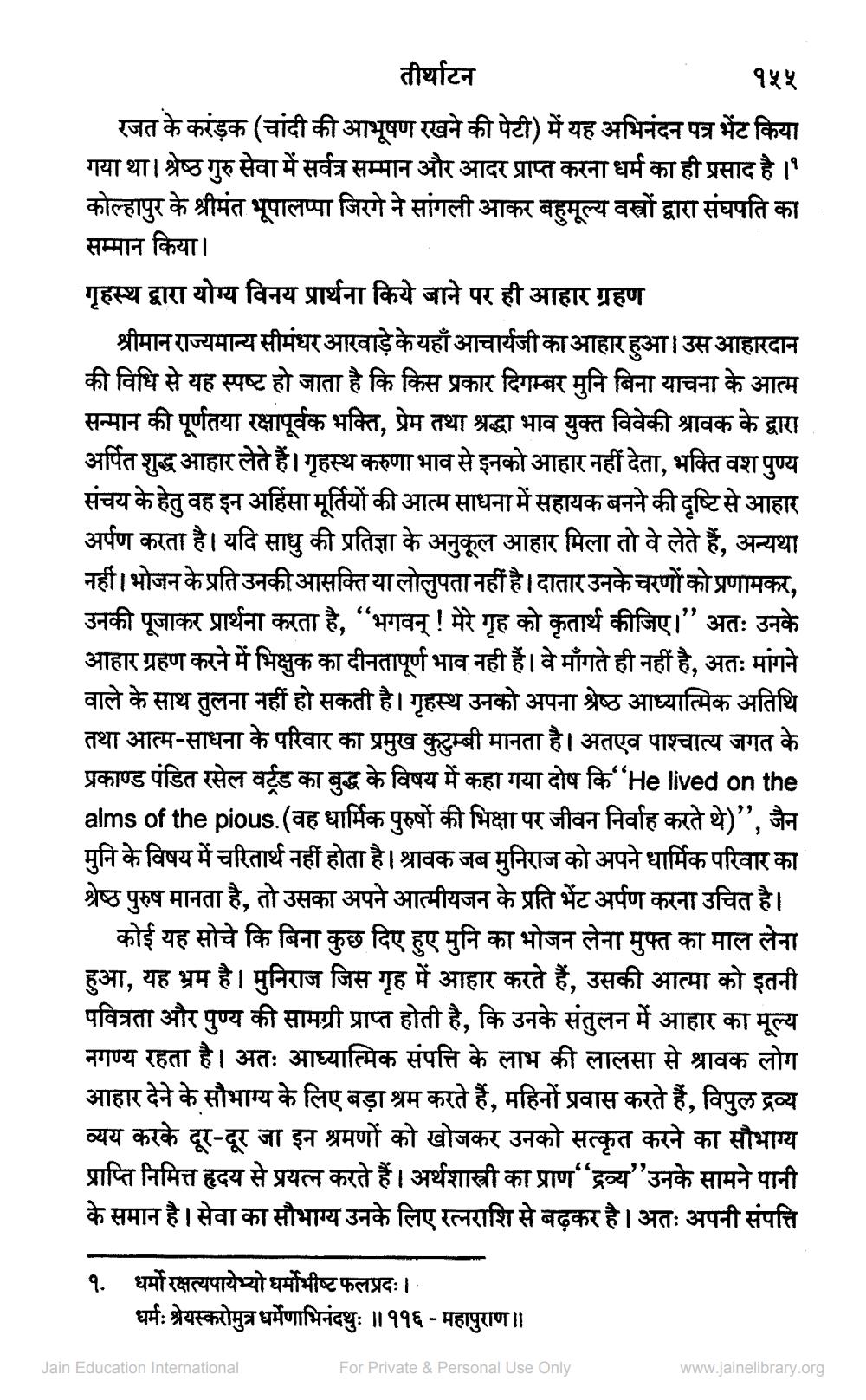________________
१५५
तीर्थाटन रजत के करंडक (चांदी की आभूषण रखने की पेटी) में यह अभिनंदन पत्र भेंट किया गया था। श्रेष्ठ गुरु सेवा में सर्वत्र सम्मान और आदर प्राप्त करना धर्म का ही प्रसाद है।' कोल्हापुर के श्रीमंत भूपालप्पा जिरगे ने सांगली आकर बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा संघपति का सम्मान किया। गृहस्थ द्वारा योग्य विनय प्रार्थना किये जाने पर ही आहार ग्रहण
श्रीमान राज्यमान्य सीमंधरआरवाड़े के यहाँ आचार्यजी का आहार हुआ। उस आहारदान की विधि से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार दिगम्बर मुनि बिना याचना के आत्म सन्मान की पूर्णतया रक्षापूर्वक भक्ति, प्रेम तथा श्रद्धा भाव युक्त विवेकी श्रावक के द्वारा अर्पित शुद्ध आहार लेते हैं। गृहस्थ करुणा भाव से इनको आहार नहीं देता, भक्ति वश पुण्य संचय के हेतु वह इन अहिंसा मूर्तियों की आत्म साधना में सहायक बनने की दृष्टि से आहार अर्पण करता है। यदि साधु की प्रतिज्ञा के अनुकूल आहार मिला तो वे लेते हैं, अन्यथा नहीं। भोजन के प्रति उनकीआसक्ति यालोलुपता नहीं है। दातार उनके चरणों को प्रणामकर, उनकी पूजाकर प्रार्थना करता है, “भगवन् ! मेरे गृह को कृतार्थ कीजिए।" अतः उनके
आहार ग्रहण करने में भिक्षुक का दीनतापूर्ण भाव नही हैं। वे माँगते ही नहीं है, अतः मांगने वाले के साथ तुलना नहीं हो सकती है। गृहस्थ उनको अपना श्रेष्ठ आध्यात्मिक अतिथि तथा आत्म-साधना के परिवार का प्रमुख कुटुम्बी मानता है। अतएव पाश्चात्य जगत के प्रकाण्ड पंडित रसेल वड का बुद्ध के विषय में कहा गया दोष कि "He lived on the alms of the pious.(वह धार्मिक पुरुषों की भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते थे)", जैन मुनि के विषय में चरितार्थ नहीं होता है। श्रावक जब मुनिराज को अपने धार्मिक परिवार का श्रेष्ठ पुरुष मानता है, तो उसका अपने आत्मीयजन के प्रति भेंट अर्पण करना उचित है।
कोई यह सोचे कि बिना कुछ दिए हुए मुनि का भोजन लेना मुफ्त का माल लेना हुआ, यह भ्रम है। मुनिराज जिस गृह में आहार करते हैं, उसकी आत्मा को इतनी पवित्रता और पुण्य की सामग्री प्राप्त होती है, कि उनके संतुलन में आहार का मूल्य नगण्य रहता है। अतः आध्यात्मिक संपत्ति के लाभ की लालसा से श्रावक लोग आहार देने के सौभाग्य के लिए बड़ा श्रम करते हैं, महिनों प्रवास करते हैं, विपुल द्रव्य व्यय करके दूर-दूर जा इन श्रमणों को खोजकर उनको सत्कृत करने का सौभाग्य प्राप्ति निमित्त हृदय से प्रयत्न करते हैं। अर्थशास्त्री का प्राण"द्रव्य" उनके सामने पानी के समान है। सेवा का सौभाग्य उनके लिए रत्नराशि से बढ़कर है। अतः अपनी संपत्ति
१. धर्मो रक्षत्यपायेभ्यो धर्मोभीष्ट फलप्रदः।
धर्मः श्रेयस्करोमुत्र धर्मेणाभिनंदथुः ॥ ११६ - महापुराण॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org