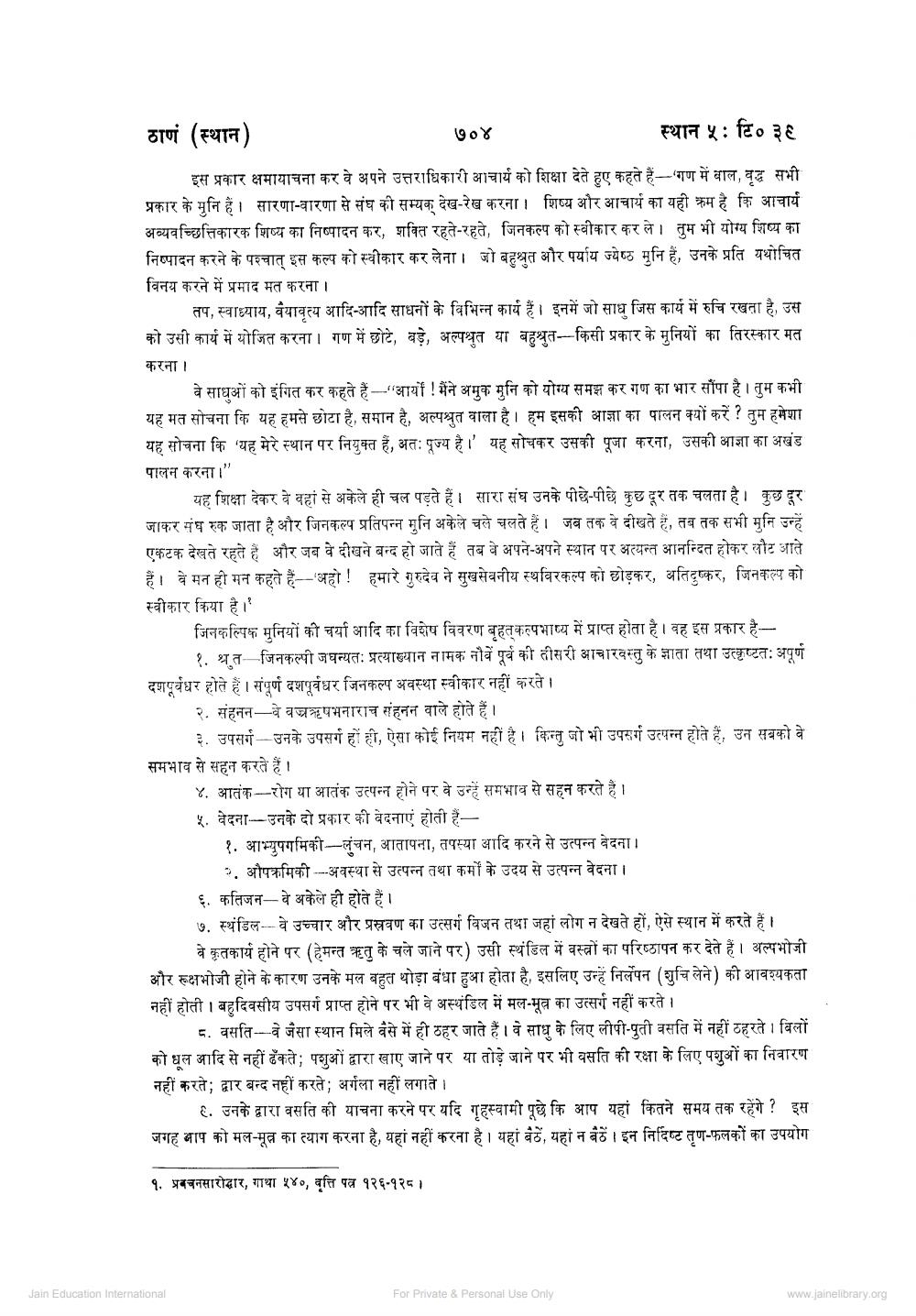________________
ठाणं (स्थान)
स्थान ५ : टि० ३६
इस प्रकार क्षमायाचना कर वे अपने उत्तराधिकारी आचार्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं— 'गण में बाल, वृद्ध सभी प्रकार के मुनि हैं । सारणा वारणा से संघ की सम्यक् देख-रेख करना । शिष्य और आचार्य का यही क्रम है कि आचार्य अव्यवच्छित्तिकारक शिष्य का निष्पादन कर, शक्ति रहते-रहते, जिनकल्प को स्वीकार कर ले। तुम भी योग्य शिष्य का निष्पादन करने के पश्चात् इस कल्प को स्वीकार कर लेना । जो बहुश्रुत और पर्याय ज्येष्ठ मुनि हैं, उनके प्रति यथोचित विनय करने में प्रमाद मत करना ।
तप, स्वाध्याय, वैयावृत्य आदि-आदि साधनों के विभिन्न कार्य हैं। इनमें जो साधु जिस कार्य में रुचि रखता है, उस उसी कार्य में योजित करना। गण में छोटे बड़े, अल्पश्रुत या बहुश्रुत --- किसी प्रकार के मुनियों का तिरस्कार मत
करना ।
७०४
साधुओं को इंगित कर कहते हैं-"आर्यो ! मैंने अमुक मुनि को योग्य समझ कर गण का भार सौंपा है। तुम कभी यह मत सोचना कि यह हमसे छोटा है, समान है, अल्पश्रुत वाला है। हम इसकी आज्ञा का पालन क्यों करें ? तुम हमेशा यह सोचना कि 'यह मेरे स्थान पर नियुक्त हैं, अतः पूज्य है।' यह सोचकर उसकी पूजा करना, उसकी आज्ञा का अखंड पालन करना।"
यह शिक्षा देकर वे वहां से अकेले ही चल पड़ते हैं । सारा संघ उनके पीछे-पीछे कुछ दूर तक चलता है। कुछ दूर जाकर संघ रुक जाता है और जिनकल्प प्रतिपन्न मुनि अकेले चले चलते हैं। जब तक वे दीखते हैं, तब तक सभी मुनि उन्हें एकटक देखते रहते हैं और जब वे दीखने बन्द हो जाते हैं तब वे अपने-अपने स्थान पर अत्यन्त आनन्दित होकर लौट आते हैं। वे मन ही मन कहते हैं अहो ! हमारे गुरुदेव ने सुखसेवनीय स्थविरकल्प को छोड़कर, अतिदुष्कर, जिनकल्प को स्वीकार किया है। '
जनकल्पिक मुनियों की चर्या आदि का विशेष विवरण बृहत्कल्पभाष्य में प्राप्त होता है। वह इस प्रकार है१. श्रुत – जिनकल्पी जघन्यतः प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व की तीसरी आचारवस्तु के ज्ञाता तथा उत्कृष्टत: अपूर्ण दशपूर्वधर होते हैं। संपूर्ण दशपूर्वधर जिनकल्प अवस्था स्वीकार नहीं करते ।
२. संहनन– वे वज्रऋषभनाराच संहनन वाले होते हैं।
३. उपसर्ग— उनके उपसर्ग हों ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु जो भी उपसर्ग उत्पन्न होते हैं, उन सबको वे समभाव से सहन करते हैं।
४. आतंक – रोग या आतंक उत्पन्न होने पर वे उन्हें समभाव से सहन करते हैं ।
५. वेदना उनके दो प्रकार की वेदनाएं होती हैं
१. आभ्युपगमिकी - लुंचन, आतापना, तपस्या आदि करने से उत्पन्न वेदना ।
२. औपक्रमिकी अवस्था से उत्पन्न तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न वेदना ।
६. कतिजन - वे अकेले ही होते हैं ।
७. स्थंडिल --- वे उच्चार और प्रस्रवण का उत्सर्ग विजन तथा जहां लोग न देखते हों, ऐसे स्थान में करते हैं ।
वे कृतकार्य होने पर (हेमन्त ऋतु के चले जाने पर ) उसी स्थंडिल में वस्त्रों का परिष्ठापन कर देते हैं। अल्पभोजी और रूक्षभोजी होने के कारण उनके मल बहुत थोड़ा बंधा हुआ होता है, इसलिए उन्हें निर्लेपन ( शुचि लेने की आवश्यकता नहीं होती । बहुदिवसीय उपसर्ग प्राप्त होने पर भी वे अस्थंडिल में मल-मूत्र का उत्सर्ग नहीं करते ।
८. वसति - वे जैसा स्थान मिले वैसे में ही ठहर जाते हैं। वे साधु के लिए लीपी पुती वसति में नहीं ठहरते। बिलों धूल आदि से नहीं ढँकते; पशुओं द्वारा खाए जाने पर या तोड़े जाने पर भी वसति की रक्षा के लिए पशुओं का निवारण नहीं करते; द्वार बन्द नहीं करते; अर्गला नहीं लगाते ।
Jain Education International
६. उनके द्वारा वसति की याचना करने पर यदि गृहस्वामी पूछे कि आप यहां कितने समय तक रहेंगे? इस जगह आप को मल-मूत्र का त्याग करना है, यहां नहीं करना है। यहां बैठें, यहां न बैठें। इन निर्दिष्ट तृण- फलकों का उपयोग
१. प्रवचनसारोद्वार गाथा ५४०, वृत्ति पत्र १२६-१२८ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org