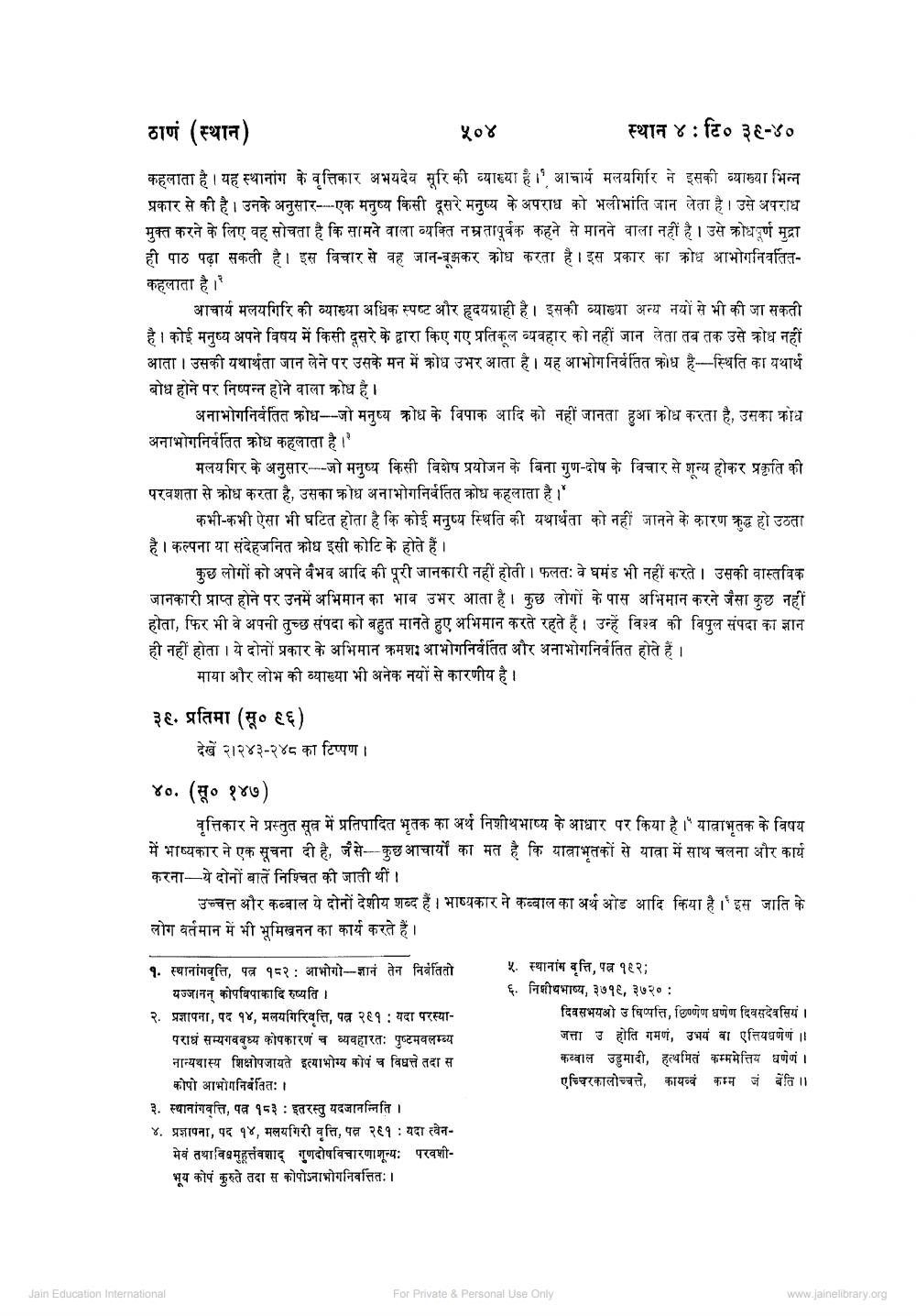________________
ठाणं (स्थान)
स्थान ४ : टि० ३९-४०
कहलाता है। यह स्थानांग के वृत्तिकार अभयदेव सूरि की व्याख्या है।' आचार्य मलयगिरि ने इसकी व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार----एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अपराध को भलीभांति जान लेता है। उसे अपराध मुक्त करने के लिए वह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति नम्रतापूर्वक कहने से मानने वाला नहीं है । उसे क्रोधपूर्ण मुद्रा ही पाठ पढ़ा सकती है। इस विचार से वह जान-बूझकर क्रोध करता है। इस प्रकार का क्रोध आभोगनिवर्तितकहलाता है।
आचार्य मलयगिरि की व्याख्या अधिक स्पष्ट और हृदयग्राही है। इसकी व्याख्या अन्य नयों से भी की जा सकती है। कोई मनुष्य अपने विषय में किसी दूसरे के द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार को नहीं जान लेता तब तक उसे क्रोध नहीं आता। उसकी यथार्थता जान लेने पर उसके मन में क्रोध उभर आता है। यह आभोग निर्वर्तित क्रोध है--स्थिति का यथार्थ बोध होने पर निष्पन्न होने वाला क्रोध है।
अनाभोगनिर्वतित क्रोध--जो मनुष्य क्रोध के विपाक आदि को नहीं जानता हुआ क्रोध करता है, उसका क्रोध अनाभोगनिर्वतित क्रोध कहलाता है।
मलय गिर के अनुसार---जो मनुष्य किसी विशेष प्रयोजन के बिना गुण-दोष के विचार से शून्य होकर प्रकृति की परवशता से क्रोध करता है, उसका क्रोध अनाभोगनिर्वतित क्रोध कहलाता है।
कभी-कभी ऐसा भी घटित होता है कि कोई मनुष्य स्थिति की यथार्थता को नहीं जानने के कारण ऋद्ध हो उठता है। कल्पना या संदेहजनित क्रोध इसी कोटि के होते हैं।
कुछ लोगों को अपने वैभव आदि की पूरी जानकारी नहीं होती। फलत: वे घमंड भी नहीं करते। उसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर उनमें अभिमान का भाव उभर आता है। कुछ लोगों के पास अभिमान करने जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी वे अपनी तुच्छ संपदा को बहुत मानते हुए अभिमान करते रहते हैं। उन्हें विश्व की विपुल संपदा का ज्ञान ही नहीं होता। ये दोनों प्रकार के अभिमान क्रमशः आभोगनिर्वतित और अनाभोगनिर्वतित होते हैं ।
माया और लोभ की व्याख्या भी अनेक नयों से कारणीय है। ३९. प्रतिमा (सू०६६)
देखें २।२४३-२४८ का टिप्पण। ४०. (सू० १४७)
वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र में प्रतिपादित भूतक का अर्थ निशीथभाष्य के आधार पर किया है। यात्राभूतक के विषय में भाष्यकार ने एक सूचना दी है, जैसे--कुछ आचार्यों का मत है कि यात्राभूतकों से यात्रा में साथ चलना और कार्य करना—ये दोनों बातें निश्चित की जाती थीं।
उच्चत्त और कब्बाल ये दोनों देशीय शब्द हैं। भाष्यकार ने कब्बाल का अर्थ ओड आदि किया है। इस जाति के लोग वर्तमान में भी भुमिखनन का कार्य करते हैं।
१. स्थानांगवृत्ति, पत्र १८२: आभोगो-ज्ञानं तेन निर्वतितो ।
यज्जानन् कोपविपाकादि रुष्यति । २. प्रज्ञापना, पद १४, मलयगिरिवत्ति, पत्र २६१ : यदा परस्या
पराधं सम्यगवबुध्य कोपकारणं च व्यवहारतः पुष्टमवलम्ब्य नान्यथास्य शिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोपं च विधत्ते तदा स
कोपो आभोगनिर्वतितः। ३. स्थानांगवत्ति, पत्र १८३ : इतरस्तु यदजानन्निति । ४. प्रज्ञापना, पद १४, मलयगिरी वृत्ति, पन्न २६१ : यदा त्वेन
मेवं तथाविधमुहूर्त्तवशाद् गुणदोषविचारणाशून्य: परवशीभूय कोपं कुरुते तदा स कोपोऽनाभोगनिवतितः ।
५. स्थानांम वृत्ति, पत्र १९२; ६. निशीथभाष्य, ३७१६, ३७२० :
दिवसभयओ उ धिप्पत्ति, छिपणेण धणेण दिवसदेवसियं । जत्ता उ होति गमणं, उभयं वा एत्तियधणेणं ।। कव्वाल उडमादी, हत्थमितं कम्ममेत्तिय धणेणं । एच्चिरकालोच्चत्ते, कायन्वं कम्म जं बैंति ।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org