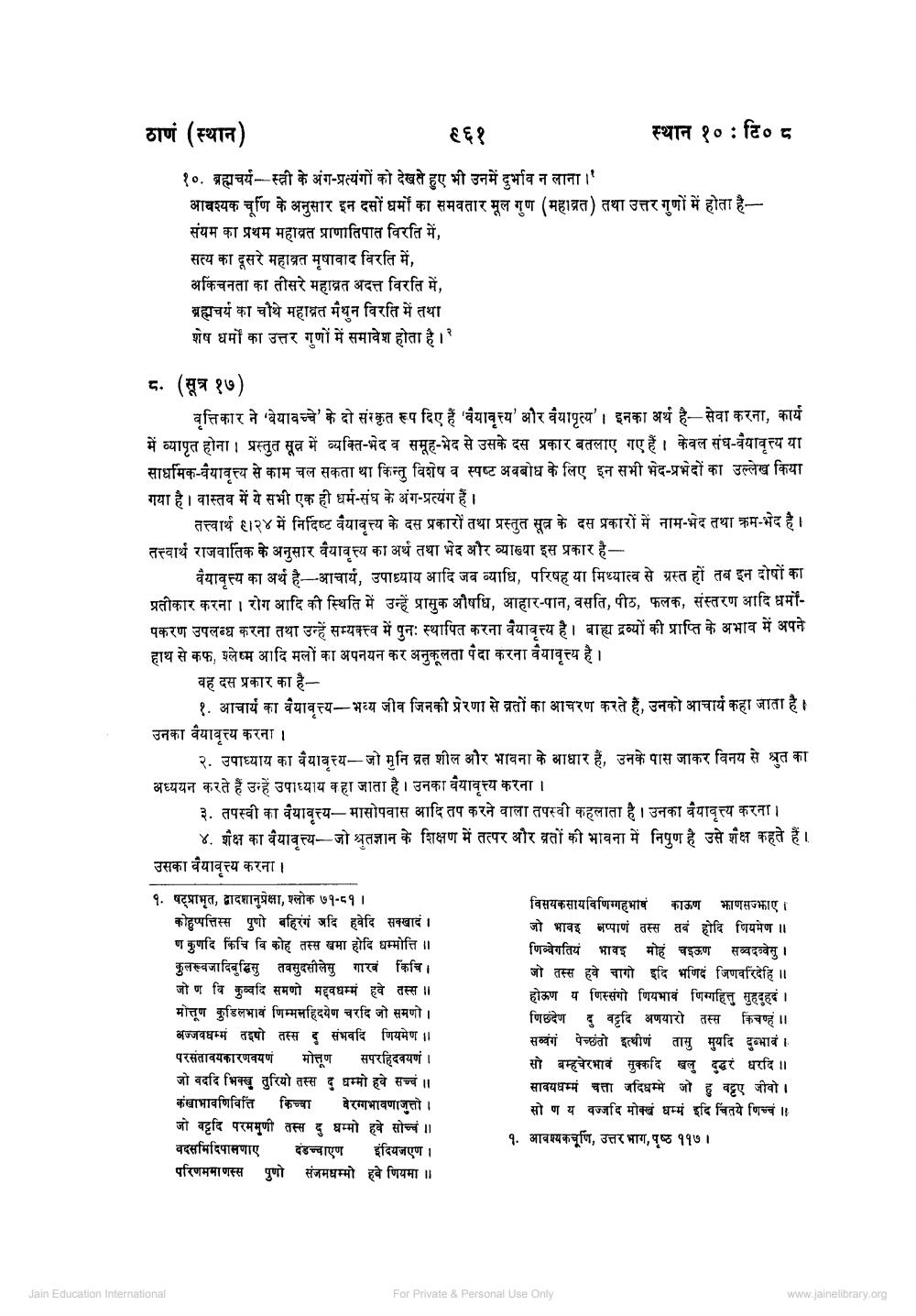________________
ठाणं (स्थान)
९६१
स्थान १० : टि०८
१०. ब्रह्मचर्य-स्त्री के अंग-प्रत्यंगों को देखते हुए भी उनमें दुर्भाव न लाना।'
आवश्यक चूणि के अनुसार इन दसों धर्मों का समवतार मूल गुण (महाव्रत) तथा उत्तर गुणों में होता हैसंयम का प्रथम महाव्रत प्राणातिपात विरति में, सत्य का दूसरे महाव्रत मषावाद विरति में, अकिंचनता का तीसरे महाव्रत अदत्त विरति में, ब्रह्मचर्य का चौथे महानत मैथुन विरति में तथा शेष धर्मों का उत्तर गुणों में समावेश होता है।
८. (सूत्र १७)
वृत्तिकार ने 'वेयावच्चे' के दो संस्कृत रूप दिए हैं 'वैयावृत्त्य' और वयापृत्य'। इनका अर्थ है-सेवा करना, कार्य में व्याप्त होना। प्रस्तुत सूत्र में व्यक्ति-भेद व समूह-भेद से उसके दस प्रकार बतलाए गए हैं। केवल संध-वैयावृत्त्य या सार्मिक-वैयावृत्त्य से काम चल सकता था किन्तु विशेष व स्पष्ट अवबोध के लिए इन सभी भेद-प्रभेदों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में ये सभी एक ही धर्म-संघ के अंग-प्रत्यंग हैं।
तत्त्वार्थ १।२४ में निर्दिष्ट वैयावृत्त्य के दस प्रकारों तथा प्रस्तुत सूत्र के दस प्रकारों में नाम-भेद तथा क्रम-भेद है। तत्त्वार्थ राजवातिक के अनुसार वैयावृत्त्य का अर्थ तथा भेद और व्याख्या इस प्रकार है
वैयावृत्त्य का अर्थ है--आचार्य, उपाध्याय आदि जब व्याधि, परिषह या मिथ्यात्व से ग्रस्त हों तब इन दोषों का प्रतीकार करना । रोग आदि की स्थिति में उन्हें प्रासुक औषधि, आहार-पान, वसति, पीठ, फलक, संस्तरण आदि धर्मोंपकरण उपलब्ध करना तथा उन्हें सम्यक्त्त्व में पुनः स्थापित करना वैयावत्त्य है। बाह्य द्रव्यों की प्राप्ति के अभाव में अपने हाथ से कफ, श्लेष्म आदि मलों का अपनयन कर अनुकूलता पैदा करना वैयावृत्त्य है।
वह दस प्रकार का है
१. आचार्य का वैयावृत्त्य-भव्य जीव जिनकी प्रेरणा से व्रतों का आचरण करते हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। उनका वैयावृत्त्य करना।
२. उपाध्याय का वैयावृत्त्य-जो मुनि व्रत शील और भावना के आधार हैं, उनके पास जाकर विनय से श्रुत का अध्ययन करते हैं उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। उनका वैयावृत्त्य करना ।
३. तपस्वी का वैयावृत्त्य–मासोपवास आदि तप करने वाला तपस्वी कहलाता है। उनका बयावृत्त्य करना।
४. शैक्ष का वैयावृत्त्य-जो श्रुतज्ञान के शिक्षण में तत्पर और व्रतों की भावना में निपुण है उसे शैक्ष कहते हैं। उसका वैयावृत्त्य करना। १. षट्नाभृत, द्वादशानुप्रेक्षा, श्लोक ७१-८१ ।
विसयकसायविणिग्गहभाष काऊण झाणसझाए। कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंग अदि हवेदि सक्खादं ।
जो भावइ मप्पाणं तस्स तवं होदि णियमेण ॥ ण कुणदि किंचि वि कोह तस्स खमा होदि धम्मोत्ति ।।
णिब्वेगतियं भावइ मोहं चइऊण सव्वदज्वेसु । कुलस्वजादिबुद्धिसु तवसुदसीलेसु गारवं किंचि ।
जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणरिदेहि ।। जो ण वि कुव्वदि समणो मद्दवधम्म हवे तस्स ।।
होऊण य णिस्संगो णियभावं णिम्गहित्तु सुहृदुहृदं । मोत्तूण कुडिलभावं णिम्मलाहिदयेण चरदि जो समणो।
णिछंदेण दु वट्टदि अणयारो तस्स किंचण्हं ।। अज्जवधम्म तइयो तस्स दु संभवदि णियमेण ।।
सव्वंगं पेच्छंतो इत्थीणं तासु मुयदि दुब्भावं । परसंतावयकारणवयणं मोत्तूण सपरहिदवयणं ।
सो बम्हचेरभावं सुक्कदि खलु दुद्धरं धरदि । जो वददि भिक्ख तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सच्चं ।।
सावयधम्मं चत्ता जदिधम्मे जो हु वट्टए जीवो। कंखाभावणिवित्ति किच्चा वेरग्गभावणाजुत्तो।
सो ण य वज्जदि मोक्खं धम्म इदि चिंतये णिच्च ।। जो बट्टदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्चं ॥ वदसमिदिपालणाए
१. आवश्यकचूणि, उत्तर भाग, पृष्ठ ११७ । दंडच्चाएण इंदियजएण। परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org