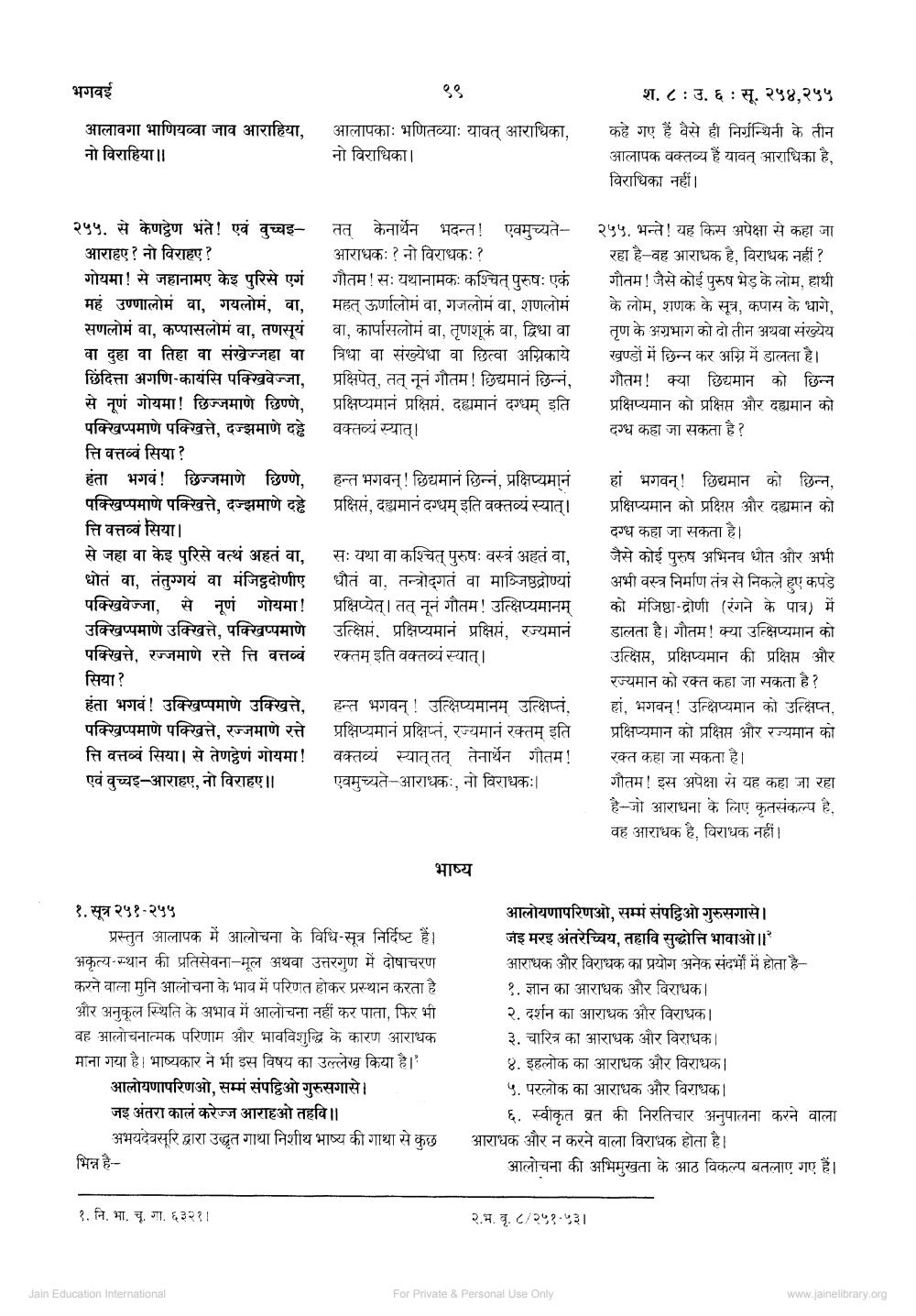________________
भगवई
आलावगा भाणियव्वा जाव आराहिया, आलापकाः भणितव्याः यावत् आराधिका, नो विराहिया॥
नो विराधिका।
श.८ : उ. ६ : सू. २५४,२५५ कहे गए हैं वैसे ही निर्ग्रन्थिनी के तीन आलापक वक्तव्य हैं यावत् आराधिका है, विराधिका नहीं।
Tes.
२५५. से केणद्वेण भंते! एवं वुच्चइ- तत् केनार्थेन भदन्त! एवमुच्यते- २५५. भन्ते! यह किस अपेक्षा से कहा जा आराहए? नो विराहए? आराधकः? नो विराधकः ?
रहा है-वह आराधक है, विराधक नहीं ? गोयमा! से जहानामए केइ पुरिसे एगं गौतम ! सः यथानामकः कश्चित् पुरुषः एकं गौतम ! जैसे कोई पुरुष भेड़ के लोम, हाथी महं उण्णालोमं वा, गयलोम, वा, महत् ऊर्णालोमं वा, गजलोमं वा, शणलोम के लोम, शणक के सूत्र, कपास के धागे, सणलोमं वा, कप्पासलोमं वा, तणसूयं वा, कार्पासलोमं वा, तृणशूकं वा, द्विधा वा तृण के अग्रभाग को दो तीन अथवा संख्येय वा दुहा वा तिहा वा संखेज्जहा वा । त्रिधा वा संख्येधा वा छित्वा अग्निकाये खण्डों में छिन्न कर अग्नि में डालता है। छिंदित्ता अगणि-कायंसि पक्खिवेज्जा, प्रक्षिपेत्, तत् नूनं गौतम ! छिद्यमानं छिन्नं, गौतम! क्या छिद्यमान को छिन्न से नूणं गोयमा! छिज्जमाणे छिपणे, प्रक्षिप्यमानं प्रक्षिप्त, दह्यमानं दग्धम् इति । प्रक्षिप्यमान को प्रक्षिप्त और दह्यमान को पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दज्झमाणे दड्ढे वक्तव्यं स्यात्।
दग्ध कहा जा सकता है? त्ति वत्तव्वं सिया? हंता भगवं! छिज्जमाणे छिण्णे, हन्त भगवन् ! छिद्यमानं छिन्नं, प्रक्षिप्यमानं हां भगवन! छिद्यमान को छिन्न, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दज्झमाणे दड्डे प्रक्षिसं, दह्यमानंदग्धम् इति वक्तव्यं स्यात्। प्रक्षिप्यमान को प्रक्षिप्स और दह्यमान को त्ति वत्तव्वं सिया।
दग्ध कहा जा सकता है। से जहा वा केइ पुरिसे वत्थं अहतं वा, सः यथा वा कश्चित् पुरुषः वस्त्रं अहतं वा, जैसे कोई पुरुष अभिनव धौत और अभी धोतं वा, तंतुग्गयं वा मंजिट्ठदोणीए धौतं वा, तन्त्रोद्गतं वा माञ्जिष्ठद्रोण्या अभी वस्त्र निर्माण तंत्र से निकले हुए कपड़े पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा! प्रक्षिप्येत्। तत् नूनं गौतम ! उत्क्षिप्यमानम् को मंजिष्ठा-द्रोणी (रंगने के पात्र) में उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे उत्क्षिप्त, प्रक्षिप्यमानं प्रक्षिप्त, रज्यमानं डालता है। गौतम! क्या उत्क्षिप्यमान को पक्खित्ते, रज्जमाणे रत्ते त्ति वत्तव्वं रक्तम इति वक्तव्यं स्यात्।
उत्क्षिप्त, प्रक्षिप्यमान की प्रक्षिप्त और सिया?
रज्यमान को रक्त कहा जा सकता है? हंता भगवं! उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, हन्त भगवन् ! उत्क्षिप्यमानम् उत्क्षिप्तं, हां, भगवन् ! उत्क्षिप्यमान को उत्क्षिप्त, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, रज्जमाणे रत्ते प्रक्षिप्यमानं प्रक्षिप्तं, रज्यमानं रक्तम् इति प्रक्षिप्यमान को प्रक्षिप्त और रज्यमान को त्ति वत्तव्वं सिया। से तेणटेणं गोयमा! वक्तव्यं स्यात् तत् तेनार्थेन गौतम ! रक्त कहा जा सकता है। एवं वुच्चइ-आराहए, नो विराहए॥ एवमुच्यते-आराधकः, नो विराधकः। गौतम ! इस अपेक्षा से यह कहा जा रहा
है-जो आराधना के लिए कृतसंकल्प है, वह आराधक है, विराधक नहीं।
भाष्य
१.सूत्र २५१-२५५
प्रस्तुत आलापक में आलोचना के विधि-सूत्र निर्दिष्ट हैं। अकृत्य-स्थान की प्रतिसेवना-मूल अथवा उत्तरगुण में दोषाचरण करने वाला मुनि आलोचना के भाव में परिणत होकर प्रस्थान करता है
और अनुकूल स्थिति के अभाव में आलोचना नहीं कर पाता, फिर भी वह आलोचनात्मक परिणाम और भावविशुद्धि के कारण आराधक माना गया है। भाष्यकार ने भी इस विषय का उल्लेख किया है।'
आलोयणापरिणओ, सम्म संपट्ठिओ गुरुसगासे। जइ अंतरा कालं करेज्ज आराहओ तहवि॥
अभयदेवसूरि द्वारा उद्धृत गाथा निशीथ भाष्य की गाथा से कुछ भिन्न है
आलोयणापरिणओ, सम्मं संपट्ठिओ गुरुसगासे। जइ मरइ अंतरेच्चिय, तहावि सुद्धोत्ति भावाओ॥ आराधक और विराधक का प्रयोग अनेक संदर्भो में होता है१. ज्ञान का आराधक और विराधक। २. दर्शन का आराधक और विराधक। ३. चारित्र का आराधक और विराधक। ४. इहलोक का आराधक और विराधक। ५. परलोक का आराधक और विराधक।
६. स्वीकृत व्रत की निरतिचार अनुपालना करने वाला आराधक और न करने वाला विराधक होता है।
आलोचना की अभिमुखता के आठ विकल्प बतलाए गए हैं।
१.नि. भा. चू. गा. ६३२१॥
२.भ. वृ.८/२५१-५३।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org