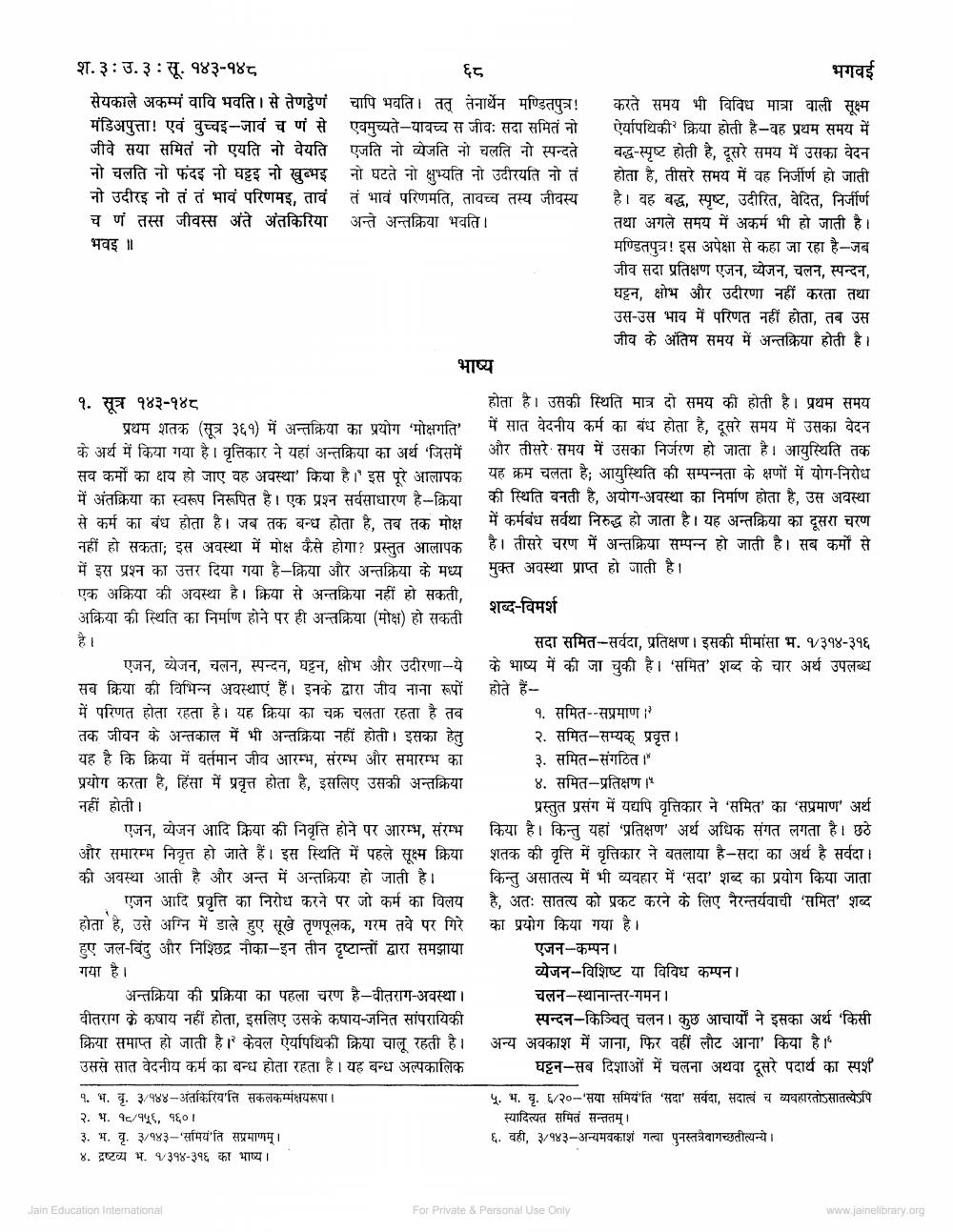________________
६८
श.३: उ.३ : सू. १४३-१४८ सेयकाले अकम्म वावि भवति। से तेणद्वेणं चापि भवति। तत् तेनार्थेन मण्डितपुत्र! मंडिअपुत्ता! एवं वुच्चइ-जावं च णं से एवमुच्यते-यावच्च स जीवः सदा समितं नो । जीवे सया समितं नो एयति नो वेयति एजति नो व्येजति नो चलति नो स्पन्दते नो चलति नो फंदई नो घट्टइ नो खुन्भइ नो घटते नो क्षुभ्यति नो उदीरयति नो तं नो उदीरइ नो तं तं भावं परिणमइ, तावं तं भावं परिणमति, तावच्च तस्य जीवस्य च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया अन्ते अन्तक्रिया भवति। भवइ॥
भगवई करते समय भी विविध मात्रा वाली सूक्ष्म ऐपिथिकी क्रिया होती है-वह प्रथम समय में बद्ध-स्पृष्ट होती है, दूसरे समय में उसका वेदन होता है, तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाती है। वह बद्ध, स्पृष्ट, उदीरित, वेदित, निर्जीर्ण तथा अगले समय में अकर्म भी हो जाती है। मण्डितपुत्र! इस अपेक्षा से कहा जा रहा है-जब जीव सदा प्रतिक्षण एजन, व्येजन, चलन, स्पन्दन, घट्टन, क्षोभ और उदीरणा नहीं करता तथा उस-उस भाव में परिणत नहीं होता, तब उस जीव के अंतिम समय में अन्तक्रिया होती है।
भाष्य
१. सूत्र १४३-१४८
होता है। उसकी स्थिति मात्र दो समय की होती है। प्रथम समय प्रथम शतक (सूत्र ३६१) में अन्तक्रिया का प्रयोग 'मोक्षगति' में सात वेदनीय कर्म का बंध होता है, दूसरे समय में उसका वेदन के अर्थ में किया गया है। वृत्तिकार ने यहां अन्तक्रिया का अर्थ 'जिसमें और तीसरे समय में उसका निर्जरण हो जाता है। आयस्थिति तक सब कर्मों का क्षय हो जाए वह अवस्था' किया है। इस पूरे आलापक यह क्रम चलता है; आयुस्थिति की सम्पन्नता के क्षणों में योग-निरोध में अंतक्रिया का स्वरूप निरूपित है। एक प्रश्न सर्वसाधारण है-क्रिया की स्थिति बनती है, अयोग-अवस्था का निर्माण होता है, उस अवस्था से कर्म का बंध होता है। जब तक बन्ध होता है. तब तक मोक्ष में कर्मबंध सर्वथा निरुद्ध हो जाता है। यह अन्तक्रिया का दसरा चरण नहीं हो सकता: इस अवस्था में मोक्ष कैसे होगा? प्रस्तत आलापक है। तीसरे चरण में अन्तक्रिया सम्पन्न हो जाती है। सब कर्मों से में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है-क्रिया और अन्तक्रिया के मध्य मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। एक अक्रिया की अवस्था है। क्रिया से अन्तक्रिया नहीं हो सकती,
शब्द-विमर्श अक्रिया की स्थिति का निर्माण होने पर ही अन्तक्रिया (मोक्ष) हो सकती
सदा समित-सर्वदा, प्रतिक्षण। इसकी मीमांसा भ. १/३१४-३१६ एजन, व्येजन, चलन, स्पन्दन, घट्टन, क्षोभ और उदीरणा-ये के भाष्य में की जा चुकी है। 'समित' शब्द के चार अर्थ उपलब्ध सब क्रिया की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इनके द्वारा जीव नाना रूपों होते हैंमें परिणत होता रहता है। यह क्रिया का चक्र चलता रहता है तब १. समित--सप्रमाण। तक जीवन के अन्तकाल में भी अन्तक्रिया नहीं होती। इसका हेतु २. समित-सम्यक् प्रवृत्त। यह है कि क्रिया में वर्तमान जीव आरम्भ, संरम्भ और समारम्भ का ३. समित-संगठित। प्रयोग करता है, हिंसा में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसकी अन्तक्रिया ४. समित-प्रतिक्षण। नहीं होती।
प्रस्तुत प्रसंग में यद्यपि वृत्तिकार ने 'समित' का 'सप्रमाण' अर्थ एजन, व्येजन आदि क्रिया की निवृत्ति होने पर आरम्भ, संरम्भ किया है। किन्तु यहां 'प्रतिक्षण' अर्थ अधिक संगत लगता है। छठे और समारम्भ निवृत्त हो जाते हैं। इस स्थिति में पहले सूक्ष्म क्रिया शतक की वृत्ति में वृत्तिकार ने बतलाया है-सदा का अर्थ है सर्वदा। की अवस्था आती है और अन्त में अन्तक्रिया हो जाती है। किन्तु असातत्य में भी व्यवहार में 'सदा' शब्द का प्रयोग किया जाता
एजन आदि प्रवृत्ति का निरोध करने पर जो कर्म का विलय है, अतः सातत्य को प्रकट करने के लिए नैरन्तर्यवाची ‘समित' शब्द होता है, उसे अग्नि में डाले हुए सखे तणपुलक, गरम तवे पर गिरे का प्रयोग किया गया है। हुए जल-बिंदु और निश्छिद्र नौका-इन तीन दृष्टान्तों द्वारा समझाया एजन-कम्पन। गया है।
व्येजन-विशिष्ट या विविध कम्पन। अन्तक्रिया की प्रक्रिया का पहला चरण है-वीतराग-अवस्था। चलन-स्थानान्तर-गमन। वीतराग के कषाय नहीं होता, इसलिए उसके कषाय-जनित सांपरायिकी स्पन्दन-किञ्चित् चलन। कुछ आचार्यों ने इसका अर्थ 'किसी क्रिया समाप्त हो जाती है। केवल ऐपिथिकी क्रिया चालू रहती है। अन्य अवकाश में जाना, फिर वहीं लौट आना' किया है। उससे सात वेदनीय कर्म का बन्ध होता रहता है। यह बन्ध अल्पकालिक घट्टन-सब दिशाओं में चलना अथवा दूसरे पदार्थ का स्पर्श १. भ. वृ. ३/१४४-अंतकिरियत्ति सकलकर्मक्षयरूपा।
५. भ. वृ. ६/२०-'सया समिय'ति 'सदा' सर्वदा, सदात्वं च व्यवहारतोऽसातत्येऽपि २. भ. १८/१५६, १६०।
स्यादित्यत समितं सन्ततम्।। ३. भ. वृ. ३/१४३-'समियंति सप्रमाणम्।
६. वही, ३/१४३-अन्यमवकाशं गत्वा पुनस्तत्रैवागच्छतीत्यन्ये। ४. द्रष्टव्य भ. १/३१४-३१६ का भाष्य।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org