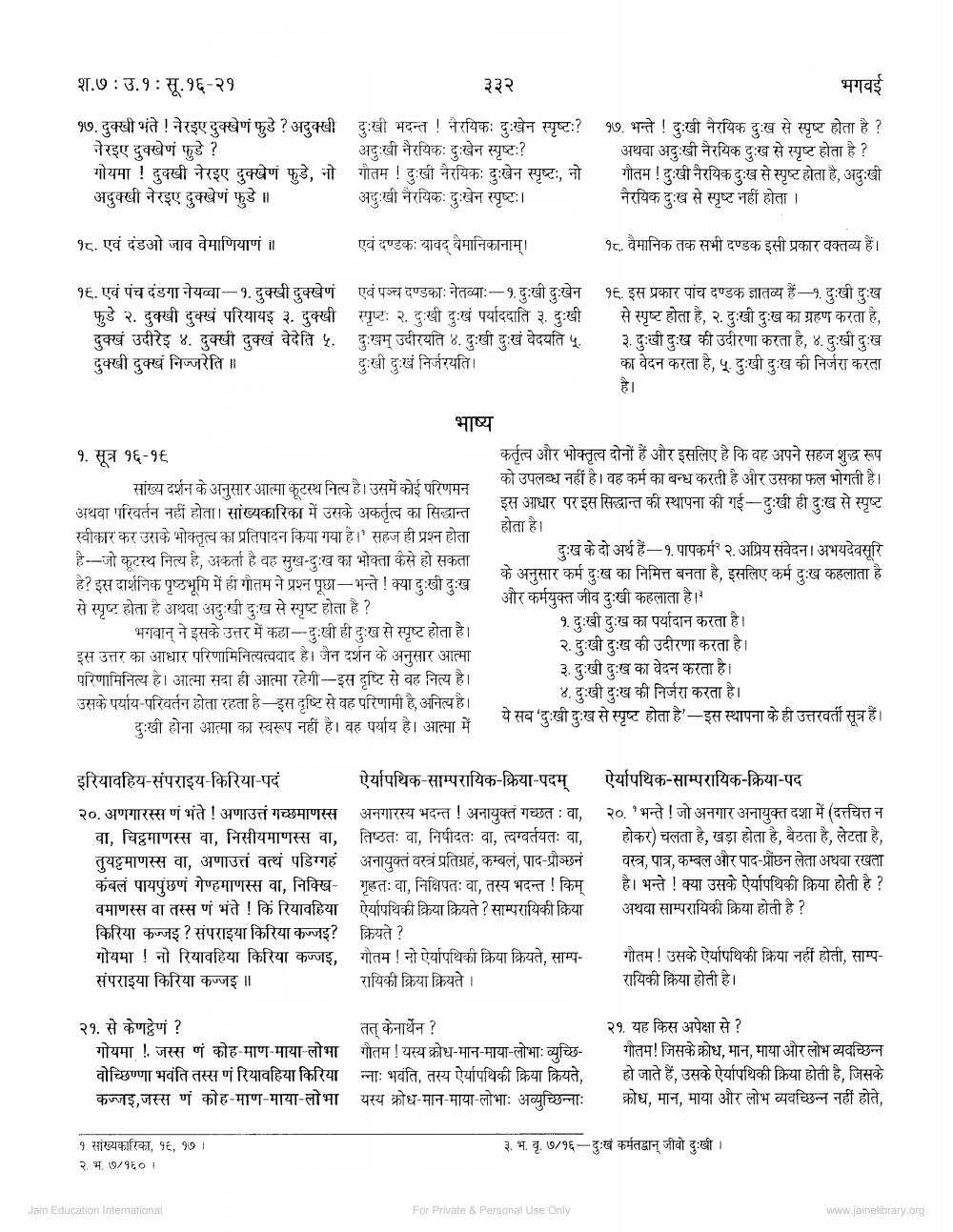________________
श.७ : उ.१ : सू.१६-२१
३३२
भगवई
१७. दुक्खी भंते ! नेरइए दुक्खेणं फुडे ? अदुक्खी दुःखी भदन्त ! नैरयिकः दुःखेन स्पृष्टः? १७. भन्ते ! दुःखी नैरयिक दुःख से स्पृष्ट होता है ? नेरइए दुक्खेणं फुडे ? अदुःखी नैरयिकः दुःखेन स्पृष्टः?
अथवा अदुःखी नैरयिक दुःख से स्पृष्ट होता है ? गोयमा ! दुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे, नो। गौतम ! दुःखी नैरयिकः दुःखेन स्पृष्टः, नो गौतम ! दुःखी नैरयिक दुःख से स्पृष्ट होता है, अदुःखी अदुक्खी नेरइए दुक्खेणं फुडे ॥ अदुःखी नैरयिकः दुःखेन स्पृष्टः।
नैरयिक दुःख से स्पृष्ट नहीं होता ।
१८. एवं दंडओ जाव वेमाणियाणं ॥
एवं दण्डकः यावद् वैमानिकानाम्।
१८. वैमानिक तक सभी दण्डक इसी प्रकार वक्तव्य हैं।
१६. एवं पंच दंडगा नेयव्वा-१. दुक्खी दुक्खेणं एवं पञ्च दण्डकाः नेतव्याः-१. दुःखी दुःखेन १E. इस प्रकार पांच दण्डक ज्ञातव्य हैं-१. दुःखी दुःख फुडे २. दुक्खी दुक्खं परियायइ ३. दुक्खी स्पृष्टः २. दुःखी दुःखं पर्याददाति ३. दुःखीसे स्पृष्ट होता है, २. दुःखी दुःख का ग्रहण करता है, दुक्खं उदीरेइ ४. दुक्खी दुक्खं वेदेति ५. दुःखम् उदीरयति ४. दुःखी दुःखं वेदयति ५. ३. दुःखी दुःख की उदीरणा करता है, ४. दुःखी दुःख दुक्खी दुक्खं निज्जरेति ॥ दुःखी दुःखं निर्जरयति।
का वेदन करता है, ५. दुःखी दुःख की निर्जरा करता
भाष्य १. सूत्र १६-१६
कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों हैं और इसलिए है कि वह अपने सहज शुद्ध रूप सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा कूटस्थ नित्य है। उसमें कोई परिणमन
को उपलब्ध नहीं है। वह कर्म का बन्ध करती है और उसका फल भोगती है। अथवा परिवर्तन नहीं होता। सांख्यकारिका में उसके अकर्तृत्व का सिद्धान्त
इस आधार पर इस सिद्धान्त की स्थापना की गई-दुःखी ही दुःख से स्पृष्ट स्वीकार कर उसके भोक्तृत्व का प्रतिपादन किया गया है।' सहज ही प्रश्न होता
होता है। है ---जो कूटस्थ नित्य है, अकर्ता है वह सुख-दुःख का भोक्ता कैसे हो सकता
दुःख के दो अर्थ हैं-१. पापकर्म २. अप्रिय संवेदन। अभयदेवसरि है? इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में ही गौतम ने प्रश्न पूछा- भन्ते ! क्या दुःखी दुःख
के अनुसार कर्म दुःख का निमित्त बनता है, इसलिए कर्म दुःख कहलाता है से स्पृष्ट होता है अथवा अदुःखी दुःख से स्पृष्ट होता है ?
और कर्मयुक्त जीव दुःखी कहलाता है। भगवान ने इसके उत्तर में कहा--दुःखी ही दुःख से स्पृष्ट होता है।
१. दुःखी दुःख का पर्यादान करता है। इस उत्तर का आधार परिणामिनित्यत्ववाद है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा
२. दुःखी दुःख की उदीरणा करता है। परिणामिनित्य है। आत्मा सदा ही आत्मा रहेगी-इस दृष्टि से वह नित्य है।
३. दुःखी दुःख का वेदन करता है। उसके पर्याय परिवर्तन होता रहता है-इस दृष्टि से वह परिणामी है, अनित्य है।
४. दुःखी दुःख की निर्जरा करता है। दुःखी होना आत्मा का स्वरूप नहीं है। वह पर्याय है। आत्मा में यसब 'दुःखा दुःख से स्पृष्ट होता है'-इस स्थापना के ही उत्तरवर्ती सत्र हैं।
इरियावहिय-संपराइय-किरिया-पदं ऐर्यापथिक-साम्परायिक-क्रिया-पदम् २०. अणगारस्स णं भंते ! अणाउत्तं गच्छमाणस्स अनगारस्य भदन्त ! अनायुक्तं गच्छत : वा, वा, चिट्ठमाणस्स वा, निसीयमाणस्स वा, तिष्ठतः वा, निषीदतः वा, त्वग्वर्तयतः वा, तुयट्टमाणस्स वा, अणाउत्तं वत्थं पडिग्गहं अनायुक्तं वस्त्रं प्रतिग्रह, कम्बलं, पाद-प्रौञ्छनं कंबलं पायपुछणं गेण्हमाणस्स वा, निक्खि- गृहतः वा, निक्षिपतः वा, तस्य भदन्त ! किम् वमाणस्स वा तस्स णं भंते ! किं रियावहिया ऐर्यापथिकी क्रिया क्रियते? साम्परायिकी क्रिया किरिया कज्जइ? संपराइया किरिया कज्जइ? क्रियते ? गोयमा ! नो रियावहिया किरिया कज्जइ, गौतम ! नो ऐपिथिकी क्रिया क्रियते, साम्पसंपराइया किरिया कज्जइ ।।
रायिकी क्रिया क्रियते।
ऐर्यापथिक-साम्परायिक-क्रिया-पद २०. ' भन्ते ! जो अनगार अनायुक्त दशा में (दत्चित्त न होकर) चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, लेटता है, वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद-प्रौंछन लेता अथवा रखता है। भन्ते ! क्या उसके ऐर्यापथिकी क्रिया होती है ? अथवा साम्परायिकी क्रिया होती है ?
गौतम ! उसके ऐर्यापथिकी क्रिया नहीं होती, साम्परायिकी क्रिया होती है।
२१. से केणद्वेणं?
तत् केनार्थेन ? गोयमा !, जस्स णं कोह-माण-माया लोभा गौतम ! यस्य क्रोध-मान-माया-लोभाः व्युच्छि- वोच्छिण्णा भवंति तस्सणं रियावहिया किरिया न्नाः भवंति, तस्य ऐपिथिकी क्रिया क्रियते, कज्जइ,जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा यस्य क्रोध-मान-माया लोभाः अव्युच्छिन्नाः
२१. यह किस अपेक्षा से? गौतम! जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्यवच्छिन्न हो जाते हैं, उसके ऐर्यापथिकी क्रिया होती है, जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्यवच्छिन्न नहीं होते,
३. भ. वृ.७/१६-दुःखं कर्मतद्वान् जीवो दुःखी।
१ सांख्यकारिका, १६, १७ । २. भ.७/१६०।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org