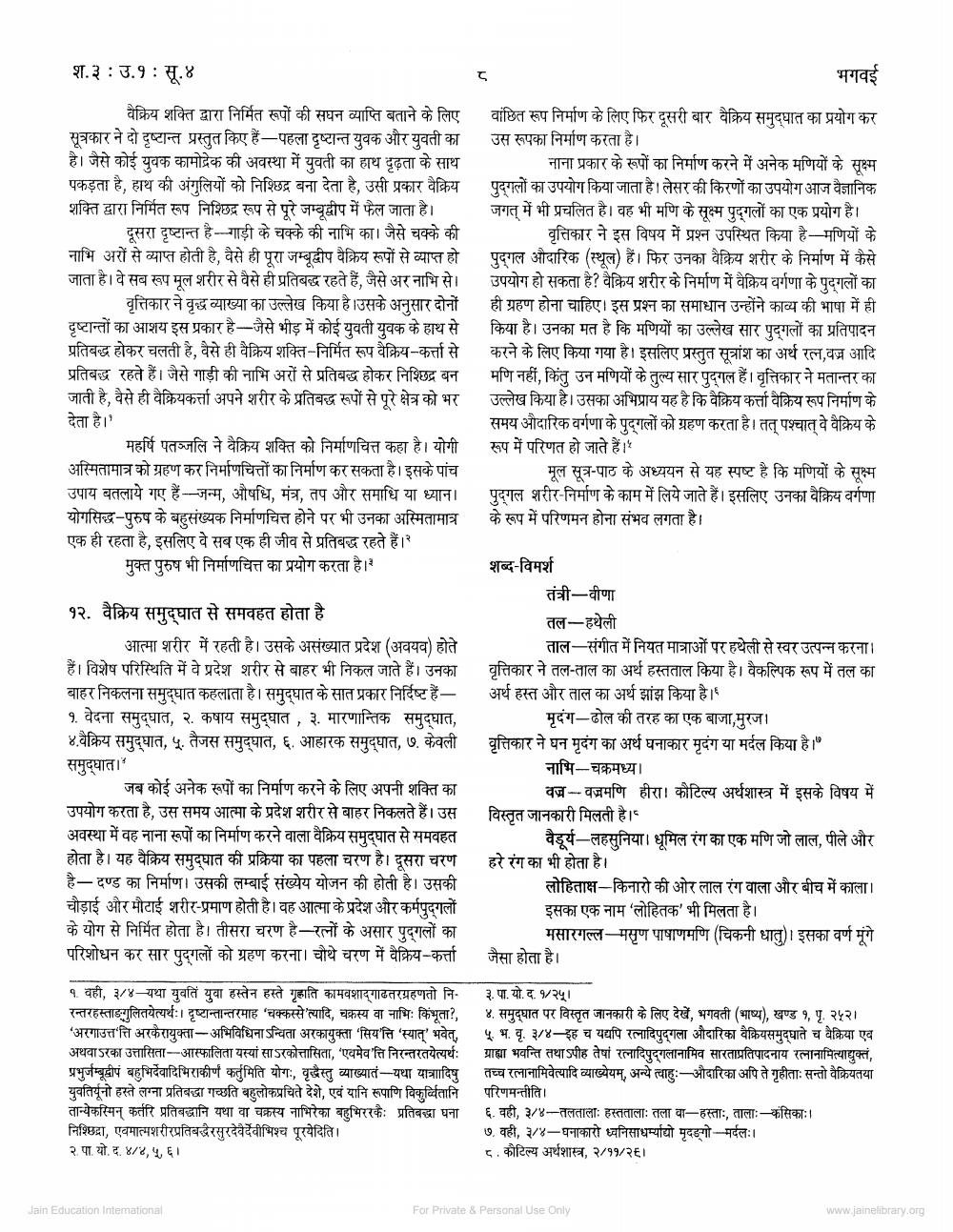________________
श. ३ : उ.१ : सू. ४
वैक्रिय शक्ति द्वारा निर्मित रूपों की सघन व्याप्ति बताने के लिए सूत्रकार ने दो दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं- पहला दृष्टान्त युवक और युवती का है । जैसे कोई युवक कामोद्रेक की अवस्था में युवती का हाथ दृढ़ता के साथ पकड़ता है, हाथ की अंगुलियों को निश्छिद्र बना देता है, उसी प्रकार वैकिय शक्ति द्वारा निर्मित रूप निश्चित रूप से पूरे जम्बूद्वीप में फैल जाता है। दूसरा दृष्टान्त है गाड़ी के चक्के की नाभि का जैसे चक्के की नाभि अरों से व्याप्त होती है, वैसे ही पूरा जम्बूद्वीप किय रूपों से व्याप्त हो जाता है। वे सब रूप मूल शरीर से वैसे ही प्रतिबद्ध रहते हैं, जैसे अर नाभि से ।
वृत्तिकार ने वृद्ध व्याख्या का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दोनों दृष्टान्तों का आशय इस प्रकार है - जैसे भीड़ में कोई युवती युवक के हाथ से प्रतिबद्ध होकर चलती है, वैसे ही क्रियशक्ति निर्मित रूप वैक्रियकर्ता से प्रतिबद्ध रहते हैं जैसे गड़ी की नाभि अरों से प्रतिबद्ध होकर निश्छिद्ध बन जाती है, वैसे ही वैक्रियकर्ता अपने शरीर के प्रतिबद्ध रूपों से पूरे क्षेत्र को भर देता है। '
1
महर्षि पतञ्जलि ने वैक्रिय शक्ति को निर्माणचित्त कहा है। योगी अस्मितामात्र को ग्रहण कर निर्माणवितों का निर्माण कर सकता है। इसके पांच उपाय बतलाये गए हैं जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि या ध्यान योगसिद्ध पुरुष के बहुसंख्यक निर्माणचित्त होने पर भी उनका अस्मितामात्र एक ही रहता है, इसलिए वे सब एक ही जीव से प्रतिबद्ध रहते हैं । २ मुक्त पुरुष भी निर्माणचित्त का प्रयोग करता है। *
१२. वैक्रिय समुद्घात से समवहत होता है
-
आत्मा शरीर में रहती है उसके असंख्यात प्रदेश (अवयव) होते हैं। विशेष परिस्थिति में वे प्रदेश शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। उनका बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। समुद्घात के सात प्रकार निर्दिष्ट हैं१. वेदना समुद्घात, २ कषाय समुद्घात २. मारणान्तिक समुद्घात, ४. वैक्रिय समुद्घात, ५. तेजस समुद्घात, ६. आहारक समुद्घात, ७ केवली समुद्धात।"
9.
7
जब कोई अनेक रूपों का निर्माण करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उस समय आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। उस अवस्था में वह नाना रूपों का निर्माण करने वाला वैक्रिय समुद्घात से समवहत होता है यह वैकिय समुद्यात की प्रक्रिया का पहला चरण है। दूसरा चरण है दण्ड का निर्माण उसकी लम्बाई संख्येय योजन की होती है उसकी चौड़ाई और मोटाई शरीर- प्रमाण होती है। वह आत्मा के प्रदेश और कर्मपुद्गलों के योग से निर्मित होता है। तीसरा चरण है – रत्नों के असार पुद्गलों का परिशोधन कर सार पुद्गलों को ग्रहण करना। चौथे चरण में वैक्रिय-कर्ता
-
१. वही, ३/४ - यथा युवतिं युवा हस्तेन हस्ते गृह्णाति कामवशाद्गाढतरग्रहणतो निरन्तरहस्ताङ्गुलितयेत्यर्थः । दृष्टान्तान्तरमाह 'चक्कस्से 'त्यादि, चक्रस्य वा नाभिः किंभूता?, 'अरगाउत्त'त्ति अरकैरायुक्ता - अभिविधिनाऽन्विता अरकायुक्ता 'सिय'त्ति 'स्यात्' भवेत्, अथवा ऽरका उत्तासिता - आस्फालिता यस्यां साऽरकोत्तासिता, 'एवमेव 'त्ति निरन्तरतयेत्यर्थः प्रभुर्जम्बूद्वीपं बहुभिर्देवादिभिराकीर्ण कर्तुमिति योगः, वृद्धैस्तु व्याख्यातं यथा यात्राादिषु युवतिर्यूनो हस्ते लग्ना प्रतिबद्धा गच्छति बहुलोकप्रचिते देशे, एवं यानि रूपाणि विकुर्व्वितानि तान्येकस्मिन् कर्तरि प्रतिबद्धानि यथा वा चक्रस्य नाभिरेका बहुभिररकैः प्रतिबद्धा घना निशिदा एवमात्मशरीरप्रतिदेवेश्वपूवैदिति । २. पा. यो. द. ४/४, ५, ६ ।
Jain Education International
ご
भगवई
छित रूप निर्माण के लिए फिर दूसरी बार क्रिय समुद्घात का प्रयोग कर उस रूपका निर्माण करता है।
नाना प्रकार के रूपों का निर्माण करने में अनेक मणियों के सूक्ष्म पुद्गलो का उपयोग किया जाता है। लेसर की किरणों का उपयोग आज वैज्ञानिक जगत् में भी प्रचलित है। वह भी मणि के सूक्ष्म पुद्गलों का एक प्रयोग है।
वृत्तिकार ने इस विषय में प्रश्न उपस्थित किया है— मणियों के पुद्गल औदारिक (स्थूल) हैं फिर उनका वैकिय शरीर के निर्माण में कैसे उपयोग हो सकता है? वैक्रिय शरीर के निर्माण में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों का ही ग्रहण होना चाहिए। इस प्रश्न का समाधान उन्होंने काव्य की भाषा में ही किया है। उनका मत है कि मणियों का उल्लेख सार पुद्गलों का प्रतिपादन करने के लिए किया गया है। इसलिए प्रस्तुत सूत्रांश का अर्थ रत्न, वज्र आदि मणि नहीं, किंतु उन मणियों के तुल्य सार पुद्गल हैं। वृत्तिकार ने मतान्तर का उल्लेख किया है। उसका अभिप्राय यह है कि वैक्रिय कर्ता वैक्रिय रूप निर्माण के समय औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तत्पश्चात् ये वैक्रिय के रूप में परिणत हो जाते हैं।
मूल सूत्र- पाठ के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मणियों के सूक्ष्म पुद्गल शरीर निर्माण के काम में लिये जाते हैं। इसलिए उनका वैक्रिय वर्गणा के रूप में परिणमन होना संभव लगता है।
शब्द-विमर्श
तंत्री - वीणा तल- हथेली
ताल - संगीत में नियत मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना। वृत्तिकार ने तल-ताल का अर्थ हस्तताल किया है। वैकल्पिक रूप में तल का अर्थ हस्त और ताल का अर्थ झांझ किया है।
मृदंग-ढोल की तरह का एक बाजा, मुरज ।
वृत्तिकार ने पन मृदंग का अर्थ घनाकार मृदंग या मर्दल किया है।"
नाभि - चक्रमध्य |
वज्र -- वज्रमणि हीरा । कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसके विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है।
वैडूर्य - लहसुनिया | धूमिल रंग का एक मणि जो लाल, पीले और हरे रंग का भी होता है।
लोहिताक्ष - किनारो की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला। इसका एक नाम 'लोहितक' भी मिलता है।
मसारगल्ल—मसृण पाषाणमणि ( चिकनी धातु)। इसका वर्ण मूंगे
जैसा होता है।
३. पा. यो. द. १/२५ ।
४. समुद्घात पर विस्तृत जानकारी के लिए देखें, भगवती (भाष्य), खण्ड १, पृ. २५२ । ५. भ. वृ. ३/४—इह च यद्यपि रत्नादिपुद्गला औदारिका वैक्रियसमुद्घाते च वैक्रिया एव ग्राह्या भवन्ति तथाऽपीह तेषां रत्नादिपुद्गलानामिव सारताप्रतिपादनाय रत्नानामित्याद्युक्तं, तच्च रत्नानामिवेत्यादि व्याख्येयम्, अन्ये त्वाहुः - औदारिका अपि ते गृहीताः सन्तो वैक्रियतया परिणमन्तीति ।
६. वही, ३/४ -तलतालाः हस्ततालाः तला वा - हस्ताः, तालाः – कसिकाः । ७. वही, ३/४ - घनाकारो ध्वनिसाधर्म्याद्यो मृदङ्गो मर्दलः । कौटिल्य अर्थशास्त्र, २/११/२६|
८.
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org