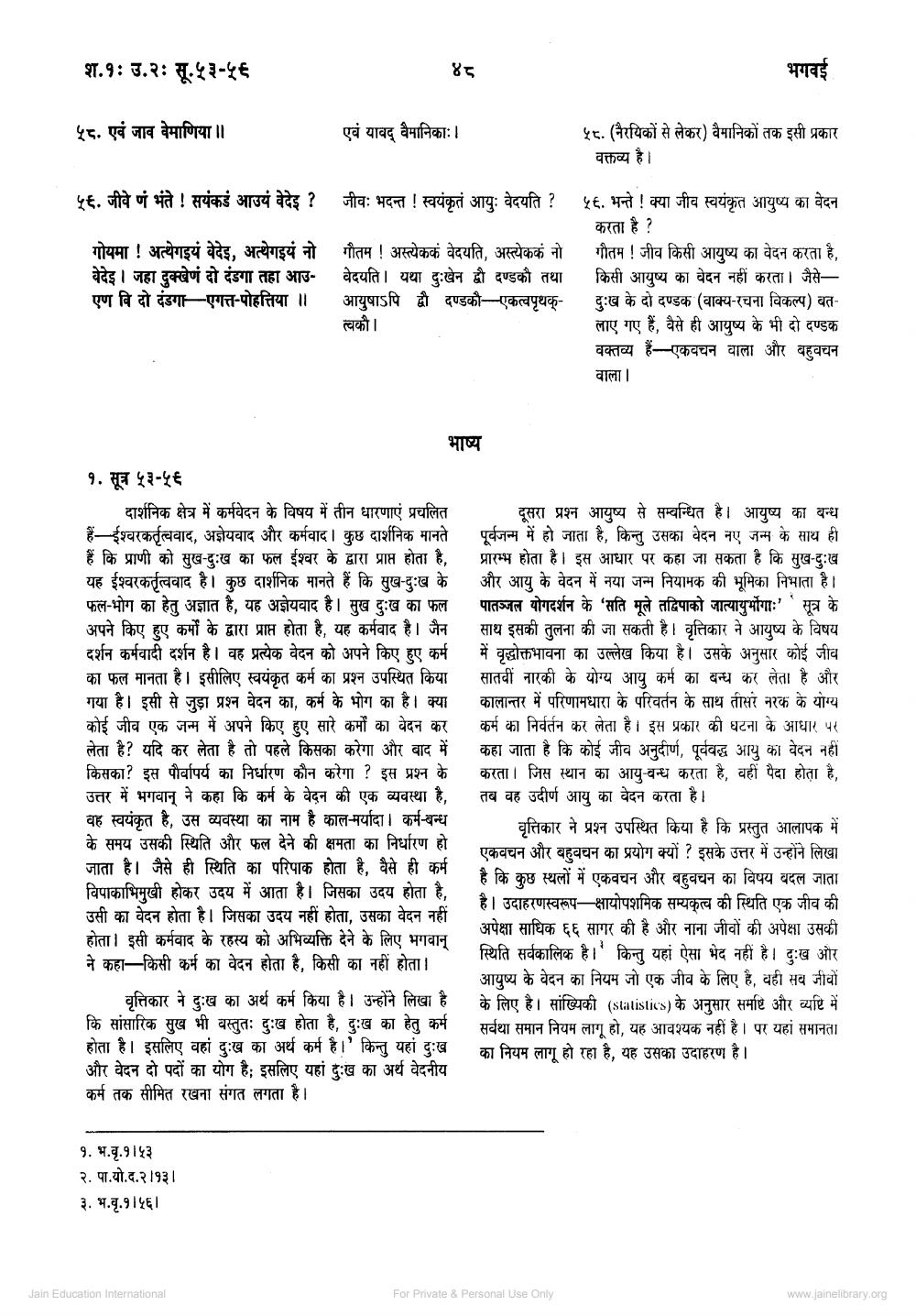________________
श.१: उ.२ः सू.५३-५६
४८
भगवई
५८. एवं जाव वेमाणिया॥
एवं यावद् वैमानिकाः।
५५. (नैरयिकों से लेकर) वैमानिकों तक इसी प्रकार वक्तव्य है।
५६.जीवे णं भंते ! सयंकडं आउयं वेदेइ ?
जीवः भदन्त ! स्वयंकृतं आयुः वेदयति ?
गोयमा ! अत्थेगइयं वेदेड, अत्थेगइयं नो वेदेइ । जहा दुक्खेणं दो दंडगा तहा आउ- एण वि दो दंडगा एगत्त-पोहत्तिया ॥
गौतम ! अस्त्येककं वेदयति, अस्त्येककं नो वेदयति । यथा दुःखेन द्वौ दण्डको तथा आयुषाऽपि द्वौ दण्डकी-एकत्वपृथक्त्वको।
५६. भन्ते ! क्या जीव स्वयंकृत आयुष्य का वेदन
करता है ? गौतम ! जीव किसी आयुष्य का वेदन करता है, किसी आयुष्य का वेदन नहीं करता। जैसेदुःख के दो दण्डक (वाक्य-रचना विकल्प) बतलाए गए हैं, वैसे ही आयुष्य के भी दो दण्डक वक्तव्य हैं-एकवचन वाला और बहुवचन वाला।
भाष्य १. सूत्र ५३-५६
दार्शनिक क्षेत्र में कर्मवेदन के विषय में तीन धारणाएं प्रचलित दूसरा प्रश्न आयुष्य से सम्बन्धित है। आयुष्य का बन्ध हैं-ईश्वरकर्तृत्ववाद, अज्ञेयवाद और कर्मवाद । कुछ दार्शनिक मानते पूर्वजन्म में हो जाता है, किन्तु उसका वेदन नए जन्म के साथ ही हैं कि प्राणी को सुख-दुःख का फल ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, प्रारम्भ होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सुख-दुःख यह ईश्वरकर्तृत्ववाद है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि सुख-दुःख के और आयु के वेदन में नया जन्म नियामक की भूमिका निभाता है। फल-भोग का हेतु अज्ञात है, यह अज्ञेयवाद है। सुख दुःख का फल पातञ्जल योगदर्शन के 'सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्मोगाः' सूत्र के अपने किए हुए कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, यह कर्मवाद है। जैन साथ इसकी तुलना की जा सकती है। वृत्तिकार ने आयुष्य के विषय दर्शन कर्मवादी दर्शन है। वह प्रत्येक वेदन को अपने किए हुए कर्म में वृद्धोक्तभावना का उल्लेख किया है। उसके अनुसार कोई जीव का फल मानता है। इसीलिए स्वयंकृत कर्म का प्रश्न उपस्थित किया सातवीं नारकी के योग्य आयु कर्म का बन्ध कर लेता है और गया है। इसी से जुड़ा प्रश्न चेदन का, कर्म के भोग का है। क्या कालान्तर में परिणामधारा के परिवर्तन के साथ तीसरे नरक के योग्य कोई जीव एक जन्म में अपने किए हुए सारे कर्मों का वेदन कर कर्म का निर्वर्तन कर लेता है। इस प्रकार की घटना के आधार पर लेता है? यदि कर लेता है तो पहले किसका करेगा और बाद में कहा जाता है कि कोई जीव अनुदीर्ण, पूर्वबद्ध आयु का वेदन नहीं किसका? इस पौर्वापर्य का निर्धारण कौन करेगा ? इस प्रश्न के करता। जिस स्थान का आयु-बन्ध करता है, वहीं पैदा होता है, उत्तर में भगवान् ने कहा कि कर्म के वेदन की एक व्यवस्था है, तब वह उदीर्ण आयु का वेदन करता है। वह स्वयंकृत है, उस व्यवस्था का नाम है काल-मर्यादा। कर्म-बन्ध
वृत्तिकार ने प्रश्न उपस्थित किया है कि प्रस्तुत आलापक में के समय उसकी स्थिति और फल देने की क्षमता का निर्धारण हो
एकवचन और बहुवचन का प्रयोग क्यों ? इसके उत्तर में उन्होंने लिखा जाता है। जैसे ही स्थिति का परिपाक होता है, वैसे ही कर्म
है कि कुछ स्थलों में एकवचन और बहुवचन का विषय बदल जाता विपाकाभिमुखी होकर उदय में आता है। जिसका उदय होता है,
है। उदाहरणस्वरूप–क्षायोपशमिक सम्यकत्व की स्थिति एक जीव की उसी का वेदन होता है। जिसका उदय नहीं होता, उसका वेदन नहीं
अपेक्षा साधिक ६६ सागर की है और नाना जीवों की अपेक्षा उसकी होता। इसी कर्मवाद के रहस्य को अभिव्यक्ति देने के लिए भगवान् ने कहा-किसी कर्म का वेदन होता है, किसी का नहीं होता।
स्थिति सर्वकालिक है।' किन्तु यहां ऐसा भेद नहीं है। दुःख और
आयुष्य के वेदन का नियम जो एक जीव के लिए है, वही सब जीवों वृत्तिकार ने दुःख का अर्थ कर्म किया है। उन्होंने लिखा है के लिए है। सांख्यिकी (statistics) के अनुसार समष्टि और व्यष्टि में कि सांसारिक सुख भी वस्तुतः दुःख होता है, दुःख का हेतु कर्म सर्वथा समान नियम लागू हो, यह आवश्यक नहीं है। पर यहां समानता होता है। इसलिए वहां दुःख का अर्थ कर्म है।' किन्तु यहां दुःख का नियम लाग हो रहा है. यह उसका उदाहरण है।
और वेदन दो पदों का योग है; इसलिए यहां दुःख का अर्थ वेदनीय कर्म तक सीमित रखना संगत लगता है।
१. भ.वृ.११५३ २. पा.यो.द.२।१३। ३. भ.वृ.११५६।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org