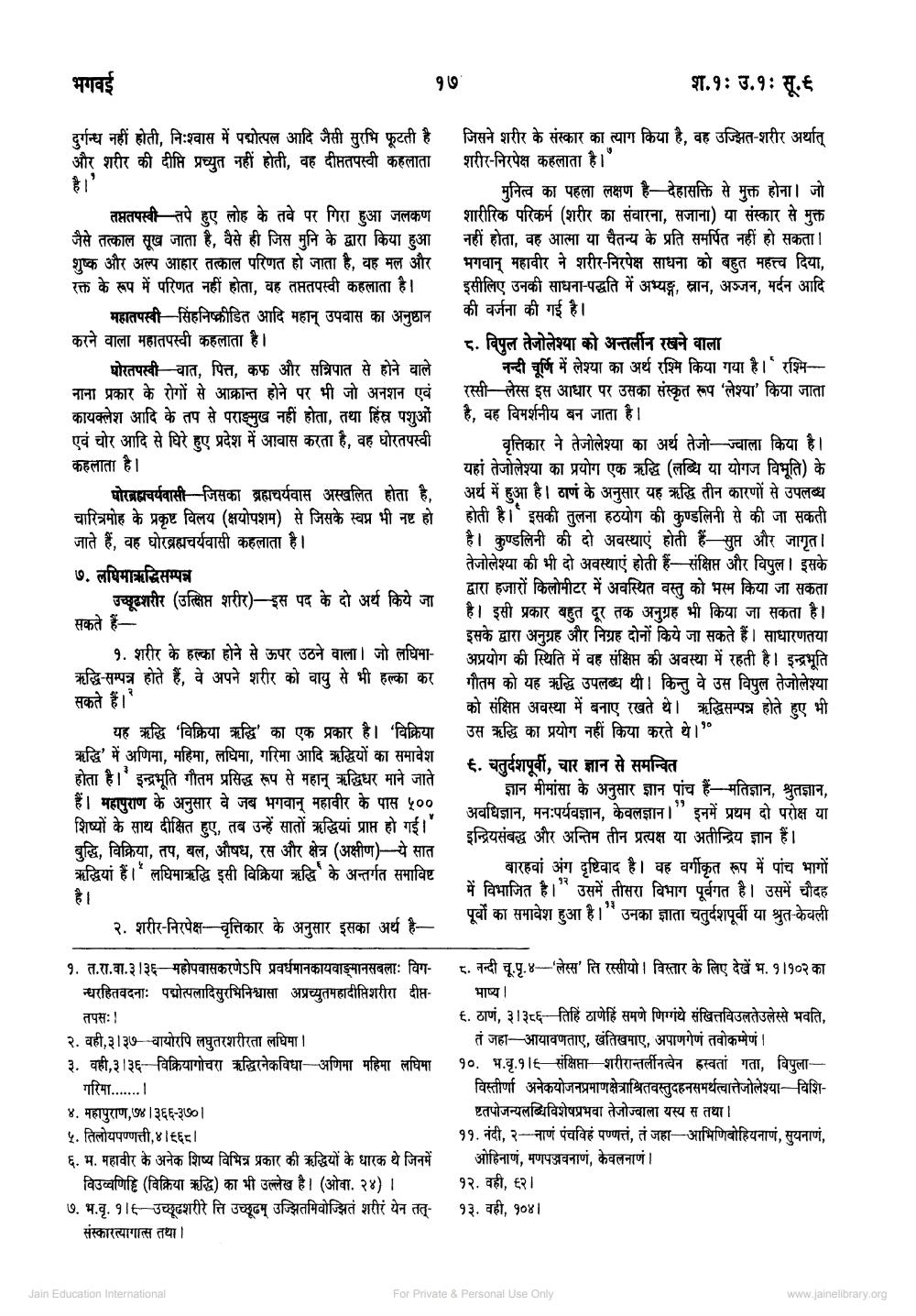________________
भगवई
श. १: उ.१: सू.६
दुर्गन्ध नहीं होती, निःश्वास में पद्मोत्पल आदि जैसी सुरभि फूटती है। जिसने शरीर के संस्कार का त्याग किया है, वह उज्झित-शरीर अर्थात् और शरीर की दीप्ति प्रच्युत नहीं होती, वह दीप्ततपस्वी कहलाता है । '
शरीर-निरपेक्ष कहलाता है।"
तप्ततपस्वी— तपे हुए लोह के तवे पर गिरा हुआ जलकण जैसे तत्काल सूख जाता है, वैसे ही जिस मुनि के द्वारा किया हुआ शुष्क और अल्प आहार तत्काल परिणत हो जाता है, वह मल और रक्त के रूप में परिणत नहीं होता, वह तप्ततपस्वी कहलाता है।
महातपस्वी — सिंहनिष्क्रीडित आदि महान् उपवास का अनुष्ठान करने वाला महातपस्वी कहलाता है।
घोरतपस्वी वात, पित्त, कफ और सन्निपात से होने वाले नाना प्रकार के रोगों से आक्रान्त होने पर भी जो अनशन एवं कायक्लेश आदि के तप से पराङ्मुख नहीं होता, तथा हिंस्र पशुओं एवं चोर आदि से घिरे हुए प्रदेश में आवास करता है, वह घोरतपस्वी कहलाता है।
घोरब्रह्मचर्यवासी जिसका ब्रह्मचर्यवास अस्खलित होता है, चारित्रमोह के प्रकृष्ट विलय ( क्षयोपशम) से जिसके स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं, वह घोरब्रह्मचर्यवासी कहलाता है।
७. लघिमाऋद्धिसम्पन्न
उच्छूढशरीर ( उत्क्षिप्त शरीर ) – इस पद के दो अर्थ किये जा सकते हैं
9. शरीर के हल्का होने से ऊपर उठने वाला। जो लघिमाऋद्धि-सम्पन्न होते हैं, वे अपने शरीर को वायु से भी हल्का कर सकते हैं।
यह ऋद्धि 'विक्रिया ऋद्धि' का एक प्रकार है। 'विक्रिया ऋद्धि' में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि ऋद्धियों का समावेश होता है । इन्द्रभूति गौतम प्रसिद्ध रूप से महान् ऋद्धिधर माने जाते हैं। महापुराण के अनुसार वे जब भगवान् महावीर के पास ५०० शिष्यों के साथ दीक्षित हुए, तब उन्हें सातों ऋद्धियां प्राप्त हो गई । " बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र (अक्षीण ) ये सात ऋद्धियां हैं। ' लघिमाऋद्धि इसी विक्रिया ऋद्धि' के अन्तर्गत समाविष्ट
है ।
१७
२. शरीर - निरपेक्ष-वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है
१. त. रा. वा. ३ | ३६ – महोपवासकरणेऽपि प्रवर्धमानकायवाङ्मानसबलाः विगन्धरहितवदनाः पद्मोत्पलादिसुरभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपसः !
२. वही, ३ | ३७ - वायोरपि लघुतरशरीरता लघिमा ।
३. वही, ३ | ३६ - विक्रियागोचरा ऋद्धिरनेकविधा— अणिमा महिमा लघिमा गरिमा....... ।
४. महापुराण, ७४ । ३६६-३७० ।
५. तिलोयपण्णत्ती, ४ । ६६८
६. भ. महावीर के अनेक शिष्य विभिन्न प्रकार की ऋद्धियों के धारक थे जिनमें विव्वणि विक्रिया ऋद्धि) का भी उल्लेख है। (ओवा. २४) । ७. भ. वृ. ११६ - उच्छूढशरीरे त्ति उच्छूढम् उज्झितमिवोज्झितं शरीरं येन तत्
संस्कारत्यागात्स तथा ।
Jain Education International
मुनित्व का पहला लक्षण है— देहासक्ति से मुक्त होना । जो शारीरिक परिकर्म ( शरीर का संवारना, सजाना) या संस्कार से मुक्त नहीं होता, वह आत्मा या चैतन्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकता । भगवान् महावीर ने शरीर-निरपेक्ष साधना को बहुत महत्त्व दिया, इसीलिए उनकी साधना-पद्धति में अभ्यङ्ग, स्नान, अञ्जन, मर्दन आदि की वर्जना की गई है।
८. विपुल तेजोलेश्या को अन्तर्लीन रखने वाला
नन्दी चूर्णि में लेश्या का अर्थ रश्मि किया गया है।' रश्मिरस्सी —-लेस्स इस आधार पर उसका संस्कृत रूप 'लेश्या' किया जाता है, वह विमर्शनीय बन जाता है।
वृत्तिकार ने तेजोलेश्या का अर्थ तेजो-ज्वाला किया है। यहां तेजोलेश्या का प्रयोग एक ऋद्धि (लब्धि या योगज विभूति) के अर्थ में हुआ है। ठाणं के अनुसार यह ऋद्धि तीन कारणों से उपलब्ध होती है। इसकी तुलना हठयोग की कुण्डलिनी से की जा सकती है । कुण्डलिनी की दो अवस्थाएं होती हैं— सुप्त और जागृत । तेजोलेश्या की भी दो अवस्थाएं होती हैं—संक्षिप्त और विपुल । इसके द्वारा हजारों किलोमीटर में अवस्थित वस्तु को भस्म किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत दूर तक अनुग्रह भी किया जा सकता है। इसके द्वारा अनुग्रह और निग्रह दोनों किये जा सकते हैं। साधारणतया अप्रयोग की स्थिति में वह संक्षिप्त की अवस्था में रहती है । इन्द्रभूति गौतम को यह ऋद्धि उपलब्ध थी। किन्तु वे उस विपुल तेजोलेश्या को संक्षिप्त अवस्था में बनाए रखते थे। ऋद्धिसम्पन्न होते हुए भी उस ऋद्धि का प्रयोग नहीं किया करते थे। "
६. चतुर्दशपूर्वी, चार ज्ञान से समन्वित
ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान पांच हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान, केवलज्ञान ।" इनमें प्रथम दो परोक्ष या इन्द्रियसंबद्ध और अन्तिम तीन प्रत्यक्ष या अतीन्द्रिय ज्ञान हैं।
बारहवां अंग दृष्टिवाद है। वह वर्गीकृत रूप में पांच भागों में विभाजित है ।" उसमें तीसरा विभाग पूर्वगत है । उसमें चौदह पूर्वो का समावेश हुआ है।" उनका ज्ञाता चतुर्दशपूर्वी या श्रुत- केवली
८. नन्दी चू. पू. ४ -- ' लेस्स' ति रस्सीयो । विस्तार के लिए देखें भ. १।१०२ का
भाष्य ।
६. ठाणं, ३।३८६ तिहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे संखित्तविउलतेउलेस्से भवति, तं जहा आयावणताए, खंतिखमाए, अपाणगेणं तवोकम्मेणं ।
१०. भ.वृ. १ १६ संक्षिप्ता-— शरीरान्तर्लीनत्वेन ह्रस्वतां गता, विपुला - विस्तीर्णा अनेकयोजनप्रमाणक्षेत्राश्रितवस्तुदहनसमर्थत्वात्तेजोलेश्या विशि ष्टतपोजन्यलब्धिविशेषप्रभवा तेजोज्वाला यस्य स तथा ।
११. नंदी, २ नाणं पंचविहं पण्णत्तं तं जहा - आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपजवनाणं, केवलनाणं ।
१२. वही, ६२ ।
१३. वही, १०४ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org