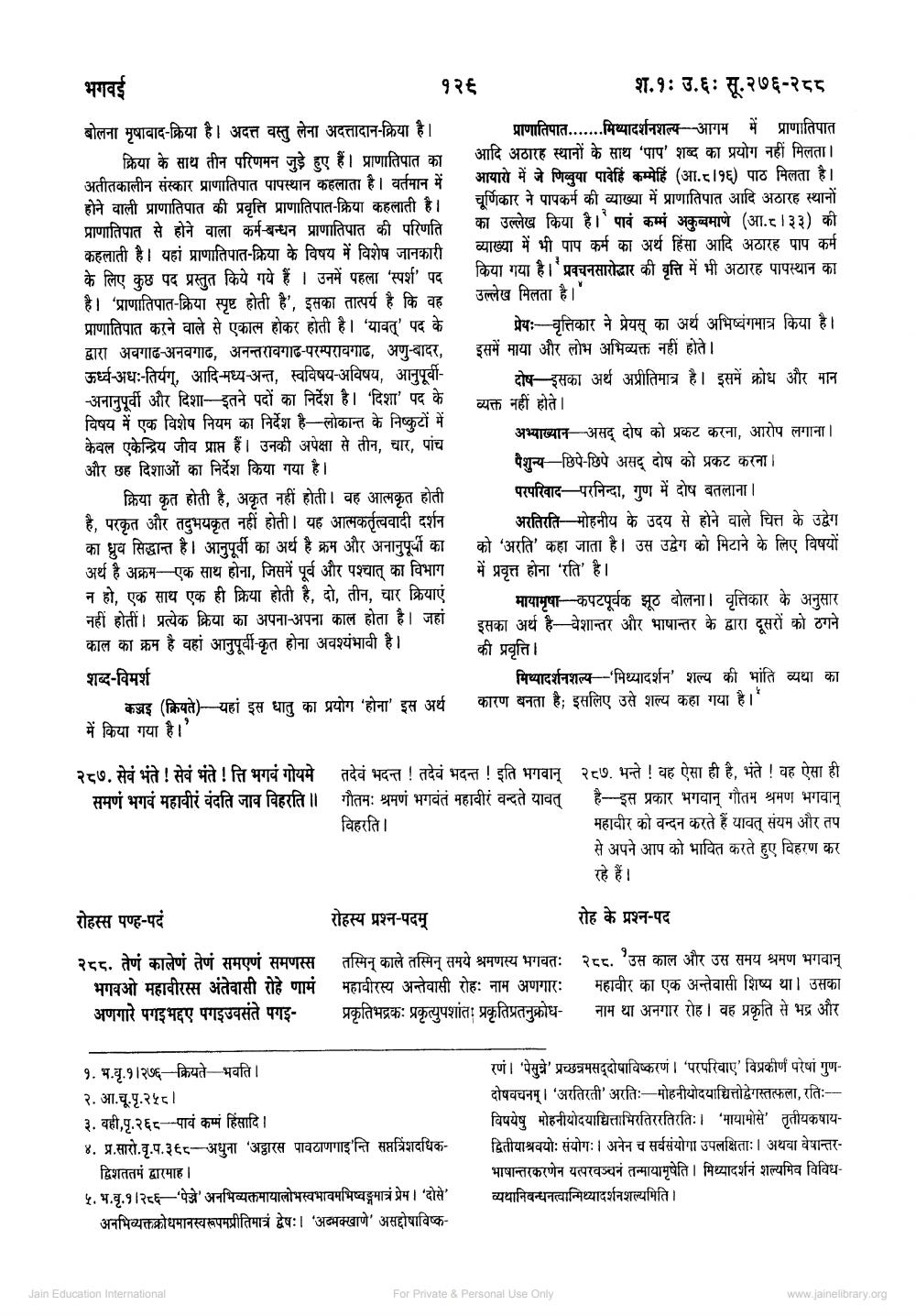________________
भगवई
१२६
श.१: उ.६: सू.२७६-२८८ बोलना मृषावाद-क्रिया है। अदत्त वस्तु लेना अदत्तादान-क्रिया है। प्राणातिपात.......मिथ्यादर्शनशल्य-आगम में प्राणातिपात
क्रिया के साथ तीन परिणमन जुड़े हुए हैं। प्राणातिपात का आदि अठारह स्थानों के साथ 'पाप' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। अतीतकालीन संस्कार प्राणातिपात पापस्थान कहलाता है। वर्तमान में
आयारो में जे णिबुया पावेहि कम्मेहिं (आ.८/१६) पाठ मिलता है। होने वाली प्राणातिपात की प्रवृत्ति प्राणातिपात-क्रिया कहलाती है।
चूर्णिकार ने पापकर्म की व्याख्या में प्राणातिपात आदि अठारह स्थानों प्राणातिपात से होने वाला कर्म-बन्धन प्राणातिपात की परिणति
का उल्लेख किया है।' पावं कम्मं अकुब्बमाणे (आ.८३३) की कहलाती है। यहां प्राणातिपात-क्रिया के विषय में विशेष जानकारी
व्याख्या में भी पाप कर्म का अर्थ हिंसा आदि अठारह पाप कर्म के लिए कुछ पद प्रस्तुत किये गये हैं । उनमें पहला 'स्पर्श' पद
किया गया है। 'प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति में भी अठारह पापस्थान का है। 'प्राणातिपात-क्रिया स्पृष्ट होती है', इसका तात्पर्य है कि वह उल्लेख मिलता है। प्राणातिपात करने वाले से एकात्म होकर होती है। ‘यावत्' पद के प्रेयः-वृत्तिकार ने प्रेयस् का अर्थ अभिष्वंगमात्र किया है। द्वारा अवगाढ-अनवगाढ, अनन्तरावगाढ-परम्परावगाढ, अणु-बादर, इसमें माया और लोभ अभिव्यक्त नहीं होते। ऊर्ध्व-अधः-तिर्यग, आदि-मध्य-अन्त, स्वविषय-अविषय, आनुपूर्वी
दोष—इसका अर्थ अप्रीतिमात्र है। इसमें क्रोध और मान अनानुपूर्वी और दिशा-इतने पदों का निर्देश है। 'दिशा' पद के
व्यक्त नहीं होते। विषय में एक विशेष नियम का निर्देश है—लोकान्त के निष्कुटों में
अभ्याख्यान-असद् दोष को प्रकट करना, आरोप लगाना। केवल एकेन्द्रिय जीव प्राप्त हैं। उनकी अपेक्षा से तीन, चार, पांच और छह दिशाओं का निर्देश किया गया है।
पैशुन्य-छिपे-छिपे असद् दोष को प्रकट करना । क्रिया कृत होती है, अकृत नहीं होती। वह आत्मकृत होती
परपरिवाद परनिन्दा, गुण में दोष बतलाना । है, परकृत और तदुभयकृत नहीं होती। यह आत्मकर्तृत्ववादी दर्शन अरतिरति मोहनीय के उदय से होने वाले चित्त के उद्वेग का ध्रुव सिद्धान्त है। आनुपूर्वी का अर्थ है क्रम और अनानुपूर्वी का को 'अरति' कहा जाता है। उस उद्वेग को मिटाने के लिए विषयों अर्थ है अक्रम—एक साथ होना, जिसमें पूर्व और पश्चात् का विभाग में प्रवृत्त होना ‘रति' है। न हो, एक साथ एक ही क्रिया होती है, दो, तीन, चार क्रियाएं
मायामृषा-कपटपूर्वक झूठ बोलना। वृत्तिकार के अनुसार नहीं होतीं। प्रत्येक क्रिया का अपना-अपना काल होता है। जहां
इसका अर्थ है वेशान्तर और भाषान्तर के द्वारा दूसरों को ठगने काल का क्रम है वहां आनुपूर्वी-कृत होना अवश्यंभावी है।
की प्रवृत्ति। शब्द-विमर्श
मिथ्यादर्शनशल्य-'मिथ्यादर्शन' शल्य की भांति व्यथा का कजइ (क्रियते) यहां इस धातु का प्रयोग होना' इस अर्थ कारण बनता है; इसलिए उसे शल्य कहा गया है।' में किया गया है।'
२६७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति भगवं गोयमे
समणं भगवं महावीरं वंदति जाव विहरति ॥
तदेवं भदन्त ! तदेवं भदन्त ! इति भगवान् २८७. भन्ते ! वह ऐसा ही है, भंते ! वह ऐसा ही गौतमः श्रमणं भगवंतं महावीरं वन्दते यावत् है-इस प्रकार भगवान् गौतम श्रमण भगवान् विहरति।
महावीर को वन्दन करते हैं यावत् संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण कर
रोहस्स पह-पदं
रोहस्य प्रश्न-पदम्
रोह के प्रश्न-पद
२५८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी रोहे णामं अणगारे पगइभद्दए पगइउवसंते पगइ-
तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणस्य भगवतः २८८. 'उस काल और उस समय श्रमण भगवान् महावीरस्य अन्तेवासी रोहः नाम अणगारः महावीर का एक अन्तेवासी शिष्य था। उसका प्रकृतिभद्रकः प्रकृत्युपशांतः प्रकृतिप्रतनुक्रोध- नाम था अनगार रोह । वह प्रकृति से भद्र और
१. भ.वृ.१।२७६ क्रियते भवति । २. आ.चू.पृ.२५८। ३. वही,पृ.२६८---पावं कम्मं हिंसादि । ४. प्र.सारो.वृ.प.३६५-अधुना 'अट्ठारस पावठाणगाइति सप्तत्रिंशदधिक
द्विशततमं द्वारमाह। ५. भ.वृ.१।२८६–'पेजे' अनभिव्यक्तमायालोभस्वभावमभिष्वङ्गमात्रं प्रेम । 'दोसे'
अनभिव्यक्तक्रोधमानस्वरूपमप्रीतिमात्र द्वेषः। 'अमक्खाणे' असद्दोषाविष्क
रणं । 'पेसुन्ने' प्रच्छन्नमसद्दोषाविष्करणं | ‘परपरिवाए' विप्रकीर्णं परेषां गुणदोषवचनम् । 'अरतिरती' अरतिः–मोहनीयोदयाच्चित्तोद्वेगस्तत्फला, रतिःविषयेषु मोहनीयोदयाच्चित्ताभिरतिररतिरतिः। 'मायामोसे' तृतीयकषायद्वितीयाश्रवयोः संयोगः । अनेन च सर्वसंयोगा उपलक्षिताः । अथवा वेषान्तरभाषान्तरकरणेन यत्परवञ्चनं तन्मायामृषेति । मिथ्यादर्शनं शल्यमिव विविधव्यथानिवन्धनत्वान्मिध्यादर्शनशल्यमिति ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org