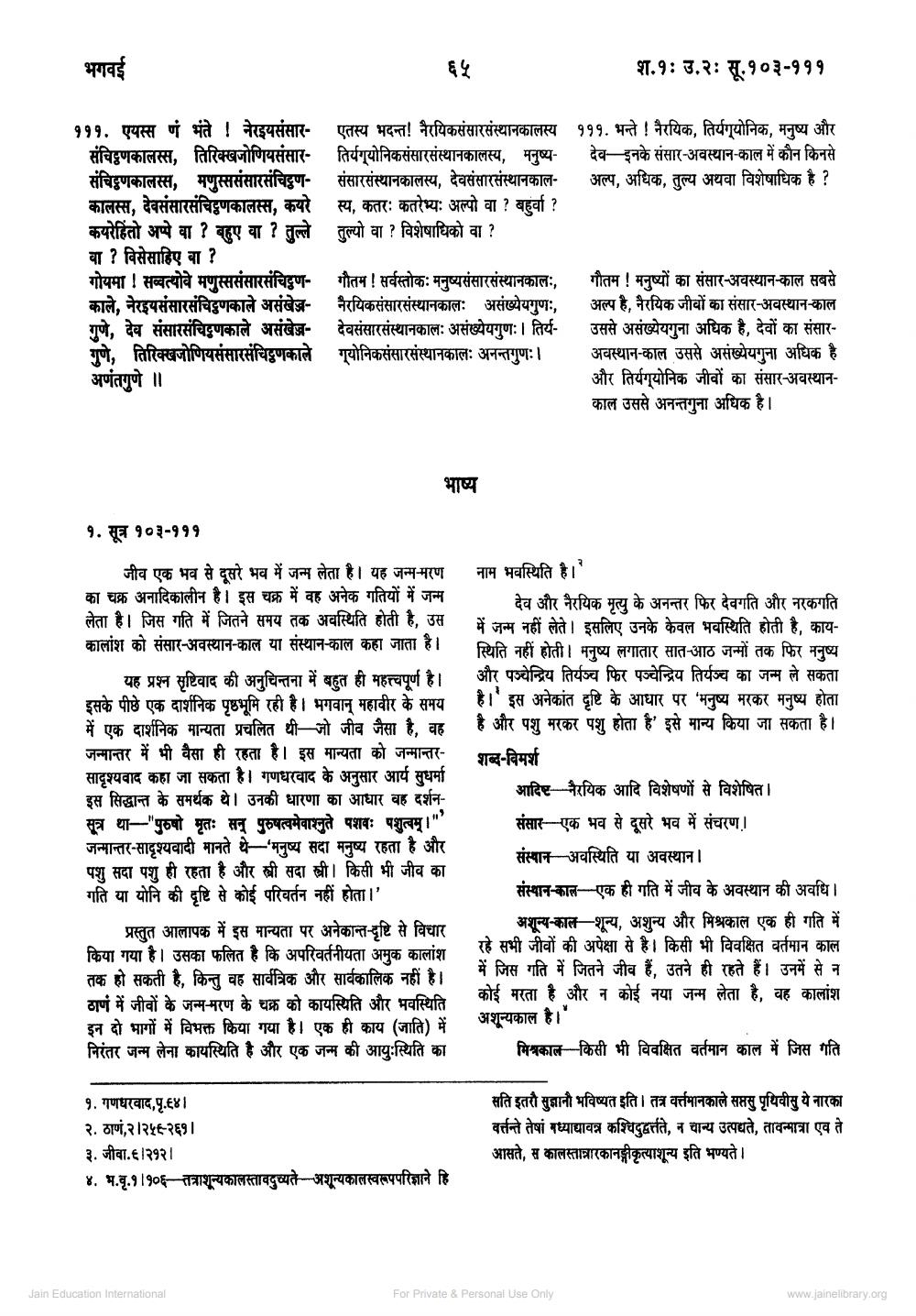________________
भगवई
६५
श.१: उ.२: सू.१०३-१११
१११. एयस्स णं भंते ! नेरइयसंसार- एतस्य भदन्त! नैरयिकसंसारसंस्थानकालस्य १११. भन्ते ! नैरयिक, तिर्यग्योनिक, मनुष्य और संचिट्ठणकालस्स, तिरिक्खजोणियसंसार- तिर्यग्योनिकसंसारसंस्थानकालस्य, मनुष्य- देव-इनके संसार-अवस्थान-काल में कौन किनसे संचिट्ठणकालस्स, मणुस्ससंसारसंचिट्ठण- संसारसंस्थानकालस्य, देवसंसारसंस्थानकाल- अल्प, अधिक, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? कालस्स, देवसंसारसंचिट्ठणकालस्स, कयरे स्य, कतरः कतरेभ्यः अल्पो वा ? बहुर्वा ? कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले तुल्यो वा ? विशेषाधिको वा ? या ? विसेसाहिए वा ? गोयमा । सव्वत्योवे मणुस्ससंसारसंचिगुण- गौतम ! सर्वस्तोकः मनुष्यसंसारसंस्थानकालः, गौतम ! मनुष्यों का संसार-अवस्थान-काल सबसे काले, नेरइयसंसारसंचिगुणकाले असंखेज- नैरयिकसंसारसंस्थानकालः असंख्येयगुणः, अल्प है, नैरयिक जीवों का संसार-अवस्थान-काल गणे, देव संसारसंचिगुणकाले असंखेज- देवसंसारसंस्थानकालः असंख्येयगुणः । तिर्य- उससे असंख्येयगुना अधिक है, देवों का संसारगणे, तिरिक्खजोणियसंसारसंचिटुणकाले गयोनिकसंसारसंस्थानकालः अनन्तगुणः। अवस्थान-काल उससे असंख्येयगुना अधिक है अणंतगुणे ॥
और तिर्यग्योनिक जीवों का संसार-अवस्थानकाल उससे अनन्तगुना अधिक है।
भाष्य
१. सूत्र १०३-१११
जीव एक भव से दूसरे भव में जन्म लेता है। यह जन्म मरण का चक्र अनादिकालीन है। इस चक्र में वह अनेक गतियों में जन्म लेता है। जिस गति में जितने समय तक अवस्थिति होती है, उस कालांश को संसार-अवस्थान-काल या संस्थान-काल कहा जाता है।
यह प्रश्न सष्टिवाद की अनुचिन्तना में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसके पीछे एक दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है। भगवान महावीर के समय में एक दार्शनिक मान्यता प्रचलित थी जो जीव जैसा है, वह जन्मान्तर में भी वैसा ही रहता है। इस मान्यता को जन्मान्तर- सादृश्यवाद कहा जा सकता है। गणधरवाद के अनुसार आर्य सुधर्मा इस सिद्धान्त के समर्थक थे। उनकी धारणा का आधार वह दर्शनसूत्र था-"पुरुषो मृतः सन् पुरुषत्वमेवाश्नुते पशवः पशुत्वम् ।'' जन्मान्तर-सादृश्यवादी मानते थे-'मनुष्य सदा मनुष्य रहता है और पशु सदा पशु ही रहता है और स्त्री सदा स्त्री। किसी भी जीव का गति या योनि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता।'
प्रस्तुत आलापक में इस मान्यता पर अनेकान्त-दृष्टि से विचार किया गया है। उसका फलित है कि अपरिवर्तनीयता अमुक कालांश तक हो सकती है, किन्तु वह सार्वत्रिक और सार्वकालिक नहीं है। ठाणं में जीवों के जन्म-मरण के चक्र को कायस्थिति और भवस्थिति इन दो भागों में विभक्त किया गया है। एक ही काय (जाति) में निरंतर जन्म लेना कायस्थिति है और एक जन्म की आयुःस्थिति का
नाम भवस्थिति है।'
देव और नैरयिक मृत्यु के अनन्तर फिर देवगति और नरकगति में लेने दमलिन केवल अवस्थिति होती है कायस्थिति नहीं होती। मनुष्य लगातार सात-आठ जन्मों तक फिर मनुष्य शिति नहीं होती लगा
और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च फिर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च का जन्म ले सकता है। इस अनेकांत दृष्टि के आधार पर 'मनुष्य मरकर मनुष्य होता है और पशु मरकर पशु होता है' इसे मान्य किया जा सकता है। शल-विमर्श
आदिए-नैरयिक आदि विशेषणों से विशेषित। संसार-एक भव से दूसरे भव में संचरण । संस्थान-अवस्थिति या अवस्थान । संस्थान-काल-एक ही गति में जीव के अवस्थान की अवधि ।
अशून्य-काल-शून्य, अशुन्य और मिश्रकाल एक ही गति में रहे सभी जीवों की अपेक्षा से है। किसी भी विवक्षित वर्तमान काल में जिस गति में जितने जीव हैं, उतने ही रहते हैं। उनमें से न कोई मरता है और न कोई नया जन्म लेता है, वह कालांश अशून्यकाल है।'
मित्रकाल-किसी भी विवक्षित वर्तमान काल में जिस गति
१. गणधरवाद,पृ.६४॥ २. ठाणं,२।२५६-२६१। ३. जीवा.६/२१२। ४. भ.बृ.१।१०६-तत्राशून्यकालस्तावदुच्यते-अशून्यकालस्वरूपपरिज्ञाने हि
सति इतरौ सुज्ञानौ भविष्यत इति। तत्र वर्तमानकाले सप्तसु पृथिवीसु ये नारका वर्तन्ते तेषां मध्याद्यावन्न कश्चिदुद्वर्तते, न चान्य उत्पद्यते, तावन्मात्रा एव ते आसते, स कालस्ताचारकानङ्गीकृत्याशून्य इति भण्यते ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org