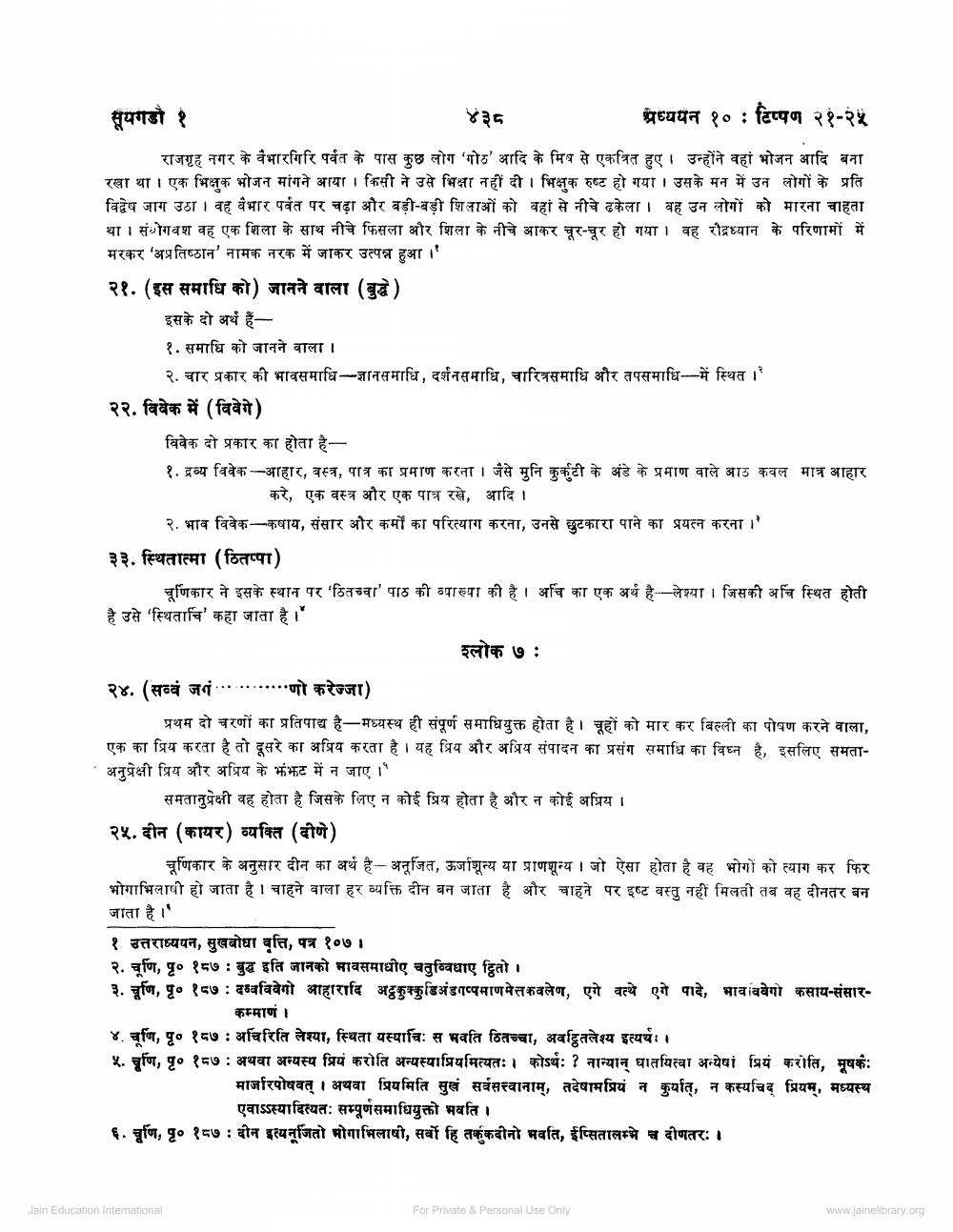________________
४३८
सूयगडौ १
अध्ययन १० : टिप्पण २१-२५ राजगृह नगर के वैभारगिरि पर्वत के पास कुछ लोग 'गोठ' आदि के मिष से एकत्रित हुए। उन्होंने वहां भोजन आदि बना रखा था। एक भिक्षुक भोजन मांगने आया । किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। भिक्षुक रुष्ट हो गया। उसके मन में उन लोगों के प्रति विद्वेष जाग उठा । वह वैभार पर्वत पर चढ़ा और बड़ी-बड़ी शिलाओं को वहां से नीचे ढकेला। वह उन लोगों को मारना चाहता था। संयोगवश वह एक शिला के साथ नीचे फिसला और शिला के नीचे आकर चूर-चूर हो गया। वह रौद्रध्यान के परिणामों में मरकर 'अप्रतिष्ठान' नामक नरक में जाकर उत्पन्न हुआ ।' २१. (इस समाधि को) जानने वाला (बुद्ध)
इसके दो अर्थ हैं१. समाधि को जानने वाला ।
२. चार प्रकार की भावसमाधि-ज्ञानसमाधि, दर्शनसमाधि, चारित्रसमाधि और तपसमाधि-में स्थित ।' २२. विवेक में (विवेगे)
विवेक दो प्रकार का होता है१. द्रव्य विवेक-आहार, वस्त्र, पात्र का प्रमाण करना । जैसे मुनि कुकूटी के अंडे के प्रमाण वाले आठ कवल मात्र आहार
करे, एक वस्त्र और एक पात्र रखे, आदि । २. भाव विवेक-कषाय, संसार और कर्मों का परित्याग करना, उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करना।' ३३. स्थितात्मा (ठितप्पा)
चूर्णिकार ने इसके स्थान पर 'ठितच्चा' पाठ की व्याख्या की है। अचि का एक अर्थ है-लेश्या । जिसकी अचि स्थित होती है उसे 'स्थिताचि' कहा जाता है।'
श्लोक ७: २४. (सव्वं जगं............णो करेज्जा )
प्रथम दो चरणों का प्रतिपाद्य है-मध्यस्थ ही संपूर्ण समाधियुक्त होता है। चूहों को मार कर बिल्ली का पोषण करने वाला, एक का प्रिय करता है तो दूसरे का अप्रिय करता है। यह प्रिय और अप्रिय संपादन का प्रसंग समाधि का विघ्न है, इसलिए समताअनुप्रेक्षी प्रिय और अप्रिय के झंझट में न जाए।'
समतानुप्रेक्षी वह होता है जिसके लिए न कोई प्रिय होता है और न कोई अप्रिय । २५. दीन (कायर) व्यक्ति (दोणे)
चूर्णिकार के अनुसार दीन का अर्थ है- अनूजित, ऊर्जाशून्य या प्राणशून्य । जो ऐसा होता है वह भोगों को त्याग कर फिर भोगाभिलाषी हो जाता है । चाहने वाला हर व्यक्ति दीन बन जाता है और चाहने पर इष्ट वस्तु नहीं मिलती तब वह दीनतर बन जाता है। १ उत्तराध्ययन, सुखबोधा वृत्ति, पत्र १०७ । २. चूणि, पृ० १८७ : बुद्ध इति जानको भावसमाधीए चतुविधाए द्वितो। ३. चूणि, पृ० १८७ : दम्वविवेगो आहारादि अट्ठकुक्कुडिअंडगप्पमाणमेतकवलेण, एगे वत्थे एगे पादे, भावविवेगो कसाय-संसार
कम्माणं। ४. चूणि, पृ० १८७ : अचिरिति लेश्या, स्थिता यस्याचिः स भवति ठितच्चा, अद्वितलेश्य इत्यर्थः । ५. चूणि, पृ० १८७ : अथवा अन्यस्य प्रियं करोति अन्यस्याप्रियमित्यतः। कोऽर्थः ? नान्यान् घातयित्वा अन्येषां प्रियं करोति, मूषकः
मार्जारपोषवत् । अथवा प्रियमिति सुखं सर्वसत्वानाम्, तदेषामप्रियं न कुर्यात्, न कस्यचिद् प्रियम्, मध्यस्थ
एवाऽस्यादित्यत: सम्पूर्णसमाधियुक्तो भवति । ६. चूणि, पृ० १८७ : दीन इत्यनूजितो भोगाभिलाषी, सर्वो हि तर्कुकदीनो भवति, ईप्सितालम्भे च दीणतरः ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org