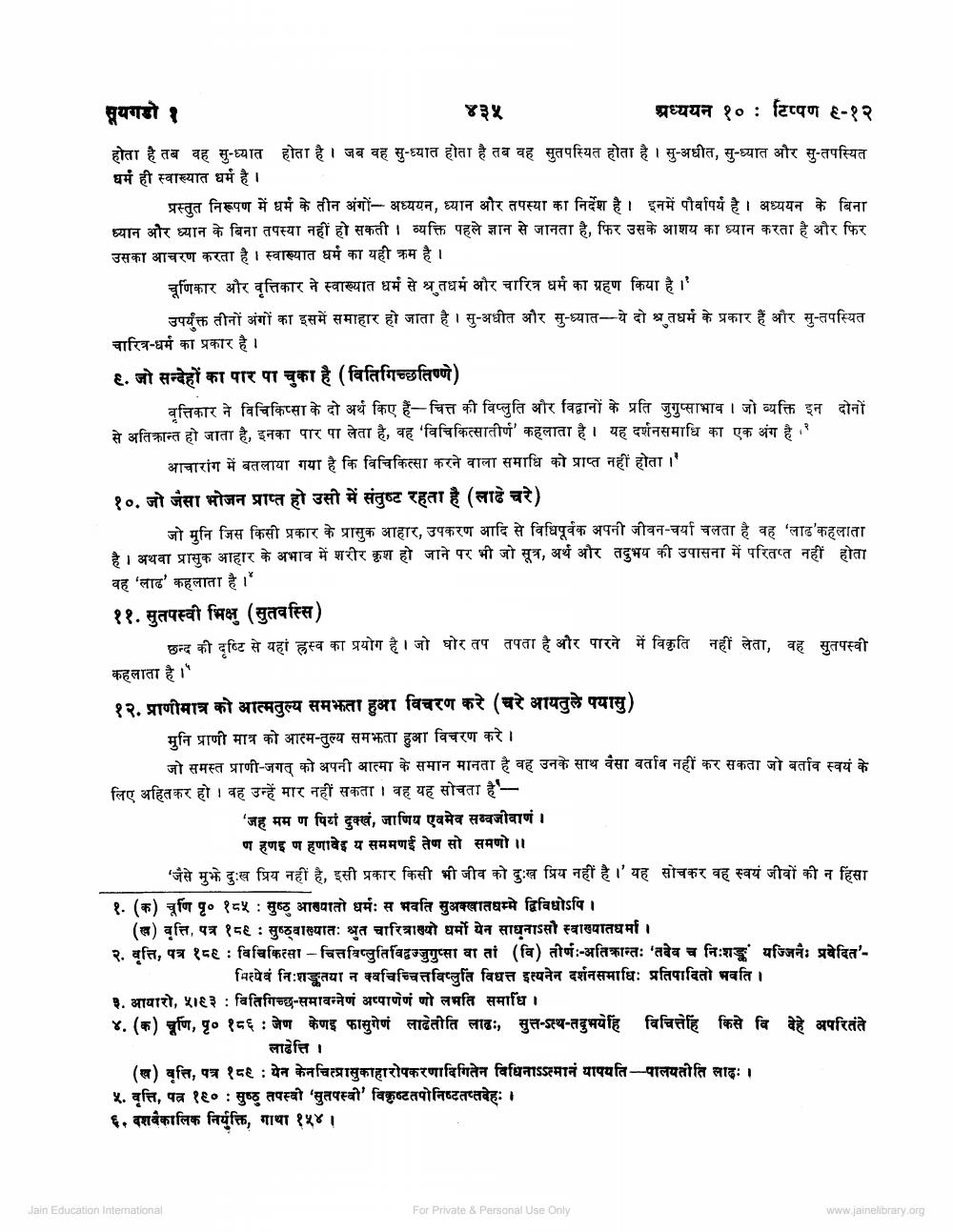________________
सूयगडो ।
४३५
अध्ययन १० : टिप्पण ६-१२ होता है तब वह सु-ध्यात होता है। जब वह सु-ध्यात होता है तब वह सुतपस्थित होता है । सु-अधीत, सु-ध्यात और सु-तपस्थित धर्म ही स्वाख्यात धर्म है।
प्रस्तुत निरूपण में धर्म के तीन अंगों- अध्ययन, ध्यान और तपस्या का निर्देश है। इनमें पौर्वापर्य है। अध्ययन के बिना ध्यान और ध्यान के बिना तपस्या नहीं हो सकती । व्यक्ति पहले ज्ञान से जानता है, फिर उसके आशय का ध्यान करता है और फिर उसका आचरण करता है । स्वाख्यात धर्म का यही क्रम है।
चूर्णिकार और वृत्तिकार ने स्वाख्यात धर्म से श्रु तधर्म और चारित्र धर्म का ग्रहण किया है।'
उपर्युक्त तीनों अंगों का इसमें समाहार हो जाता है । सु-अधीत और सु-ध्यात-ये दो श्रु तधर्म के प्रकार हैं और सु-तपस्थित चारित्र-धर्म का प्रकार है। ६. जो सन्देहों का पार पा चुका है (वितिगिच्छतिणे)
वृत्तिकार ने विचिकिप्सा के दो अर्थ किए हैं-चित्त की विप्लुति और विद्वानों के प्रति जुगुप्साभाव । जो व्यक्ति इन दोनों से अतिक्रान्त हो जाता है, इनका पार पा लेता है, वह 'विचिकित्सातीर्ण' कहलाता है। यह दर्शनसमाधि का एक अंग है २
आचारांग में बतलाया गया है कि विचिकित्सा करने वाला समाधि को प्राप्त नहीं होता।' १०. जो जैसा भोजन प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है (लाढे चरे)
जो मनि जिस किसी प्रकार के प्रासुक आहार, उपकरण आदि से विधिपूर्वक अपनी जीवन-चर्या चलता है वह 'लाढ'कहलाता है। अथवा प्रासुक आहार के अभाव में शरीर कृश हो जाने पर भी जो सूत्र, अर्थ और तदुभय की उपासना में परितप्त नहीं होता वह 'लाढ' कहलाता है।" ११. सुतपस्वी भिक्षु (सुतवस्सि)
छन्द की दृष्टि से यहां ह्रस्व का प्रयोग है । जो घोर तप तपता है और पारने में विकृति नहीं लेता, वह सूतपस्वी कहलाता है। १२. प्राणीमात्र को आत्मतुल्य समझता हुआ विचरण करे (चरे आयतुले पयास)
मुनि प्राणी मात्र को आत्म-तुल्य समझता हुआ विचरण करे ।
जो समस्त प्राणी-जगत् को अपनी आत्मा के समान मानता है वह उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकता जो बर्ताव स्वयं के लिए अहितकर हो । वह उन्हें मार नहीं सकता। वह यह सोचता है
'जह मम ण पियं दुक्खं, जाणिय एवमेव सम्वजीवाणं ।
ण हणइ ण हणावेद य सममणई तेण सो समणो॥ _ 'जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है, इसी प्रकार किसी भी जीव को दुःख प्रिय नहीं है।' यह सोचकर वह स्वयं जीवों की न हिंसा १. (क) चूणि पृ० १८५ : सुष्ठ आख्यातो धर्मः स भवति सुअक्खातधम्मे द्विविधोऽपि ।
(ख) वृत्ति, पत्र १८६ : सुष्ठ्वाख्यातः श्रुत चारित्राख्यो धर्मो येन साधनाऽसौ स्वाख्यातधर्मा । २. वृत्ति, पत्र १८६ : विचिकित्सा -चित्तविप्लुतिविद्वज्जुगुप्सा वा तां (वि) तीर्ण:-अतिक्रान्तः 'तवेव च निःशङ्क यज्जिनः प्रवेदित'
___मित्येवं नि:शङ्कतया न क्वचिच्चित्तविप्लुति विधत्त इत्यनेन दर्शनसमाधिः प्रतिपावितो भवति। ३. आयारो, ५२९३ : वितिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं णो लमति समाधि । ४. (क) चूणि, पृ० १८६ : जेण केणइ फासुगेणं लाढेतीति लाढः, सुत्त-ऽस्थ-तदुभयहिं विचित्तेहिं किसे वि देहे अपरितंते
लाढेत्ति। (ख) वृत्ति, पत्र १८६ : येन केनचित्प्रासुकाहारोपकरणादिगितेन विधिनाऽऽस्मानं यापयति-पालयतीति लादः । ५. वृत्ति, पत्र १९० : सुष्ठु तपस्वी 'सुतपस्वी' विकृष्टतपोनिष्टतप्तदेहः । ६. दशवकालिक नियुक्ति, गाथा १५४ ।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org