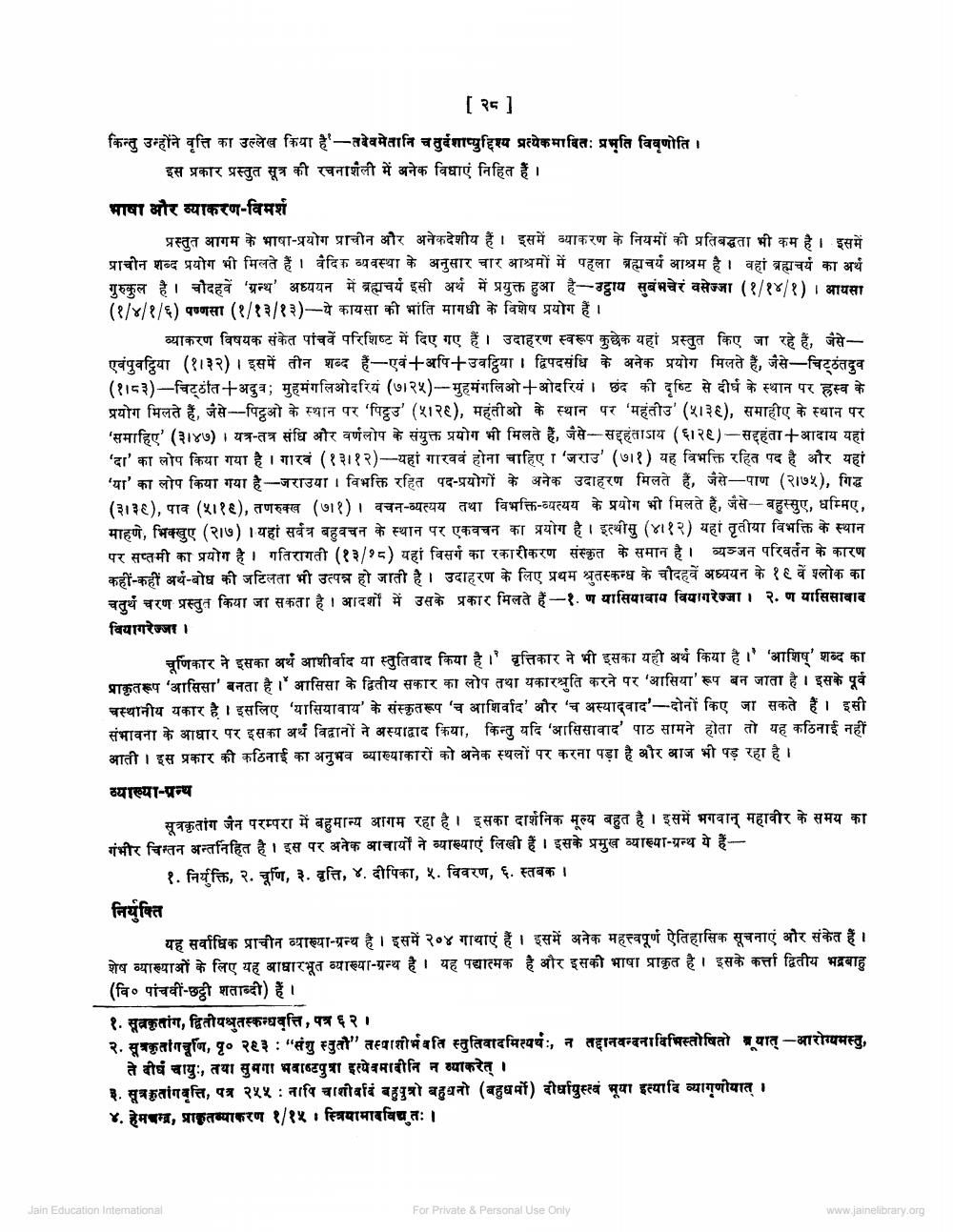________________
[ २८ ]
किन्तु उन्होंने वृत्ति का उल्लेख किया है' - तदेवमेतानि चतुर्दशादिस्य प्रत्येकमावितः प्रभृति विवृणोति । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र की रचनाशैली में अनेक विधाएं निहित हैं ।
भाषा और व्याकरण-विमर्श
प्रस्तुत आगम के भाषा प्रयोग प्राचीन और अनेकदेशीय हैं। इसमें व्याकरण के नियमों की प्रतिबद्धता भी कम है । इसमें प्राचीन शब्द प्रयोग भी मिलते हैं । वैदिक व्यवस्था के अनुसार चार आश्रमों में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है। वहां ब्रह्मचर्य का अर्थ गुरुकुल हैं। चौदहवें 'ग्रन्थ' अध्ययन में ब्रह्मचर्य इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है- उट्ठाय सुबंभचेरं वसेज्जा (१/१४ / १) | आयसा (१/४/१/६) वसा (१/१२/१३ ) - कायता की भांति मागधी के विशेष प्रयोग है।
व्याकरण विषयक संकेत पांचवें परिशिष्ट में दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछेक यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसेएवंद्विया (१।३२) इसमें तीन शब्द हैं- एवं+अपि+ उयडिया द्विपदसंधि के अनेक प्रयोग मिलते हैं, जैसे- चितव (११८३) – चिट्ठांत +अदुव; मुहमंगलिओदरियं ( ७।२५ ) - मुहमंगलिओ + ओदरियं । छंद की दृष्टि से दीर्घं के स्थान पर ह्रस्व के प्रयोग मिलते हैं, जैसे--पिट्ठओ के स्थान पर 'पिट्ठउ' (५।२६), महंतीओ के स्थान पर 'महंतीउ' (५।३६), समाहीए के स्थान पर 'समाहिए' (३।४७) । यत्र-तत्र संधि और वर्णलोप के संयुक्त प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे- सद्दहंताडाय ( ६।२९ ) - सद्दहंता + आदाय यहां 'दा' का लोप किया गया है । गारवं ( १३ | १२ ) - यहां गारववं होना चाहिए । 'जराउ' (७।१) यह विभक्ति रहित पद है और यहां 'या' का लोप किया गया है—जराउया । विभक्ति रहित पद-प्रयोगों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे—पाण (२०७५), गिद्ध (३०३९), पाव (५।१६), तणरुक्ख ( ७११) । वचन व्यत्यय तथा विभक्ति-व्यत्यय के प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे- बहुस्सुए, धम्मिए, माहणे, भिक्खुए (२७) । यहां सर्वत्र बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है । इत्थीसु (४।१२) यहां तृतीया विभक्ति के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग है । गतिरागती ( १३ / १८ ) यहां विसर्ग का रकारीकरण संस्कृत के समान है । व्यञ्जन परिवर्तन के कारण कहीं-कहीं अर्थ- बोध की जटिलता भी उत्पन्न हो जाती है । उदाहरण के लिए प्रथम श्रुतस्कन्ध के चौदहवें अध्ययन के १६ वें श्लोक का चतुर्थ चरण प्रस्तुत किया जा सकता है। आदर्शों में उसके प्रकार मिलते हैं - १. ण यासियावाय वियागरेज्जा । २. ण यासिसाबाद वियागरेज्जा ।
चूर्णिकार ने इसका अर्थ आशीर्वाद या स्तुतिवाद किया है।" वृत्तिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है।' 'आशिष' शब्द का प्राकृतरूप 'आसिसा' बनता है। आसिसा के द्वितीय सकार का लोप तथा यकारश्रुति करने पर 'आसिया' रूप बन जाता है। इसके पूर्व स्थानीय वकार है। इसलिए 'पासियावाय' के संस्कृतरूप व आशिर्वाद' और 'च अस्यादवाद' दोनों किए जा सकते हैं। इसी संभावना के आधार पर इसका अर्थ विद्वानों ने अस्याद्वाद किया, किन्तु यदि 'आसिसावाद' पाठ सामने होता तो यह कठिनाई नहीं आती। इस प्रकार की कठिनाई का अनुभव व्याख्याकारों को अनेक स्थलों पर करना पड़ा है और आज भी पड़ रहा है।
व्याख्या-ग्रन्थ
सूत्रकृतांग जैन परम्परा में बहुमान्य आगम रहा है। इसका दार्शनिक मूल्य बहुत है। इसमें भगवान् महावीर के समय का गंभीर चिन्तन अन्तर्निहित है। इस पर अनेक आचार्यों ने व्याख्याएं लिखी हैं। इसके प्रमुख व्याख्या-ग्रन्थ ये हैं
१. नियुक्ति २. चूर्ण ३. वृत्ति, ४. दीपिका, ५. विवरण ६. स्तबक
नियुक्ति
यह सर्वाधिक प्राचीन व्याख्या-ग्रन्थ है । इसमें २०४ गाथाएं हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं और संकेत हैं । शेष व्याख्याओं के लिए यह आधारभूत व्याख्या ग्रन्थ है । यह पद्यात्मक है और इसकी भाषा प्राकृत है। इसके कर्त्ता द्वितीय भद्रबाहु (वि० पांचवीं छुट्टी शताब्दी) हैं ।
१. सूत्रकृतांग, द्वितीयभूतस्कन्धवृत्ति पत्र ६२ ।
3
२.
--
०२१३ "संतुस्ती" स्वातीति स्तुतियादनित्यर्थः ननन्दनादिभिस्तोषितो वात् आरोग्यमस्तु ते दीर्घायु तथा सुमना चाष्टा इत्येवमादीनि न व्याकरेत् ।
३. सूत्रकृतांगवृत्ति, पत्र २५५ : नापि चाशीर्वादं बहुपुत्रो बहुधनो (बहुधर्मो ) दीर्घायुस्त्वं सूया इत्यादि व्यागुणीयात् । ४. हेमचन्द्र प्राकृतव्याकरण १/१५ स्वियामादविद्यतः ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org