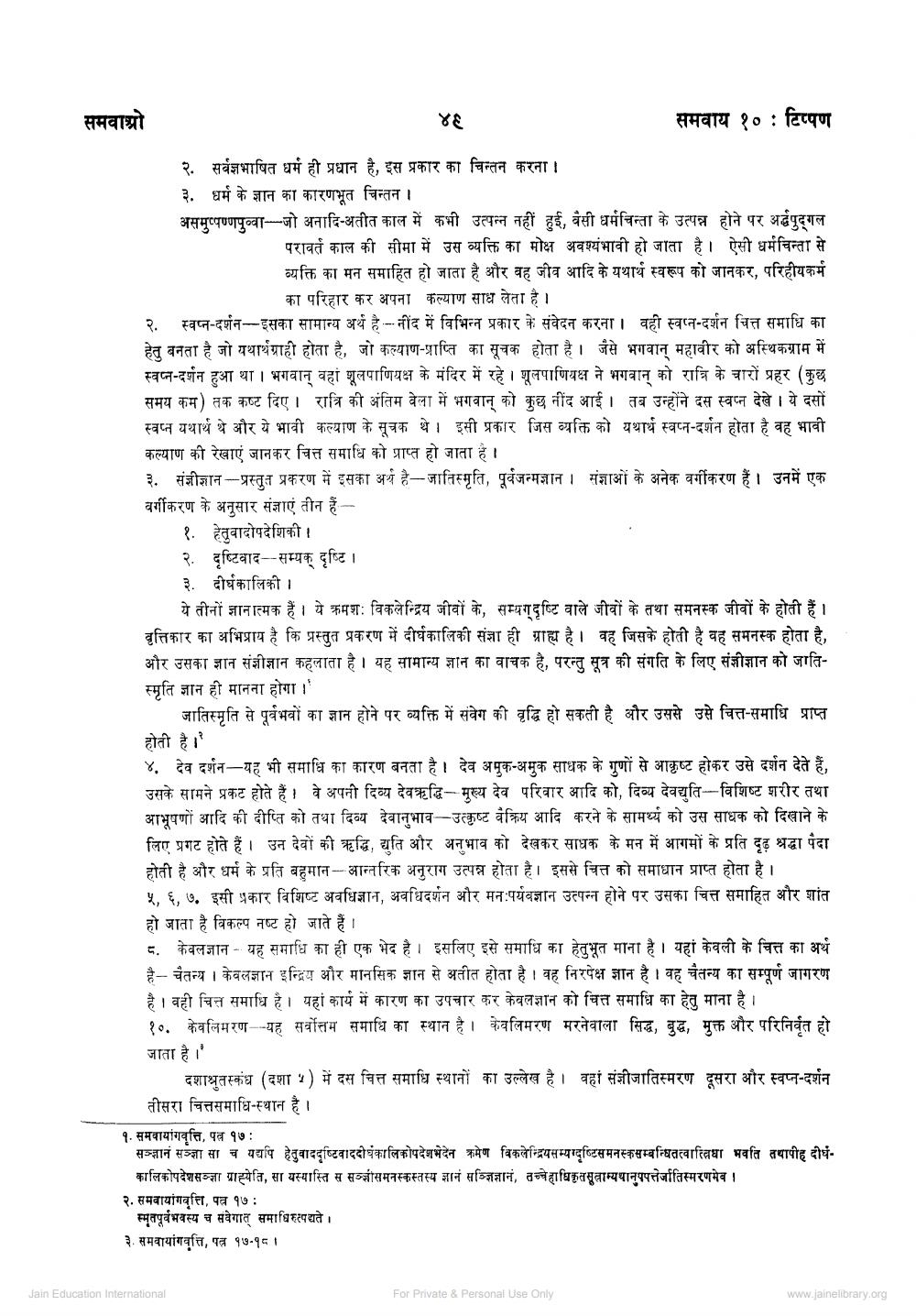________________
समवाश्रो
४६
२. सर्वज्ञभाषित धर्म ही प्रधान है, इस प्रकार का चिन्तन करना ।
३. धर्म के ज्ञान का कारणभूत चिन्तन ।
असमुप्पण्णपुव्वा - जो अनादि अतीत काल में कभी उत्पन्न नहीं हुई, वैसी धर्मचिन्ता के उत्पन्न होने पर अर्द्धपुद्गल
परावर्त काल की सीमा में उस व्यक्ति का मोक्ष अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसी धर्मचिन्ता से व्यक्ति का मन समाहित हो जाता है और वह जीव आदि के यथार्थ स्वरूप को जानकर, परिहीय कर्म का परिहार कर अपना कल्याण साध लेता है ।
२.
स्वप्न-दर्शन -- इसका सामान्य अर्थ है - नींद में विभिन्न प्रकार के संवेदन करना। वही स्वप्न-दर्शन चित्त समाधि का हेतु बनता है जो यथार्थग्राही होता है, जो कल्याण प्राप्ति का सूचक होता है। जैसे भगवान् महावीर को अस्थिकग्राम में स्वप्न-दर्शन हुआ था । भगवान् वहां शूलपाणियक्ष के मंदिर में रहे। शूलपाणियक्ष ने भगवान् को रात्रि के चारों प्रहर ( कुछ समय कम ) तक कष्ट दिए । रात्रि की अंतिम वेला में भगवान् को कुछ नींद आई। तब उन्होंने दस स्वप्न देखे । ये दसों स्वप्न यथार्थ थे और ये भावी कल्याण के सूचक थे। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को यथार्थ स्वप्न-दर्शन होता है वह भावी कल्याण की रेखाएं जानकर चित्त समाधि को प्राप्त हो जाता है ।
३. संज्ञीज्ञान - प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है-जातिस्मृति, पूर्वजन्मज्ञान । संज्ञाओं के अनेक वर्गीकरण हैं। उनमें एक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञाएं तीन हैं
१. हेतुवादोपदेशिकी ।
२.
३. दीर्घकालिकी ।
दृष्टिवाद - सम्यक् दृष्टि ।
ये तीनों ज्ञानात्मक हैं । ये क्रमशः विकलेन्द्रिय जीवों के, सम्यग्दृष्टि वाले जीवों के तथा समनस्क जीवों के होती हैं । वृत्तिकार का अभिप्राय है कि प्रस्तुत प्रकरण में दीर्घकालिकी संज्ञा ही ग्राह्य है । वह जिसके होती है वह समनस्क होता है, और उसका ज्ञान संज्ञीज्ञान कहलाता है । यह सामान्य ज्ञान का वाचक है, परन्तु सूत्र की संगति के लिए संज्ञीज्ञान को जातिस्मृति ज्ञान ही मानना होगा ।'
जातिस्मृति से पूर्वभवों का ज्ञान होने पर व्यक्ति में संवेग की वृद्धि हो सकती है और उससे उसे चित्त-समाधि प्राप्त होती है । '
४. देव दर्शन - यह भी समाधि का कारण बनता है। देव अमुक-अमुक साधक के गुणों से आकृष्ट होकर उसे दर्शन देते हैं, उसके सामने प्रकट होते हैं। वे अपनी दिव्य देवऋद्धि - मुख्य देव परिवार आदि को दिव्य देवद्युति - विशिष्ट शरीर तथा आभूषणों आदि की दीप्ति को तथा दिव्य देवानुभाव - उत्कृष्ट वैक्रिय आदि करने के सामर्थ्य को उस साधक को दिखाने के लिए प्रगट होते हैं । उन देवों की ऋद्धि द्युति और अनुभाव को देखकर साधक के मन में आगमों के प्रति दृढ़ श्रद्धा पैदा होती है और धर्म के प्रति बहुमान - आन्तरिक अनुराग उत्पन्न होता है। इससे चित्त को समाधान प्राप्त होता है ।
५, ६, ७. इसी प्रकार विशिष्ट अवधिज्ञान, अवधिदर्शन और मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न होने पर उसका चित्त समाहित और शांत हो जाता है विकल्प नष्ट हो जाते हैं।
८. केवलज्ञान यह समाधि का ही एक भेद है।
इसलिए इसे समाधि का हेतुभूत माना है। यहां केवली के चित्त का अर्थ
है - चैतन्य । केवलज्ञान इन्द्रिय और मानसिक ज्ञान से अतीत होता है। वह निरपेक्ष ज्ञान है। वह चैतन्य का सम्पूर्ण जागरण
T
समवाय १० : टिप्पण
है । वही चित्त समाधि है । यहां कार्य में कारण का उपचार कर केवलज्ञान को चित्त समाधि का हेतु माना है ।
१०. केवलिमरण - यह सर्वोत्तम समाधि का स्थान है । केवलिमरण मरनेवाला सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वृत हो जाता है।'
दशाश्रुतस्कंध ( दशा 1 ) में दस चित्त समाधि स्थानों का उल्लेख है। वहां संज्ञीजातिस्मरण दूसरा और स्वप्न-दर्शन तीसरा चित्तसमाधि स्थान है ।
Jain Education International
१. समवायांगवृत्ति, पत्र १७:
सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा सा च यद्यपि हेतुवाददृष्टिवाददीर्घकालिकोपदेशभेदेन क्रमेण विकलेन्द्रियसम्यग्दृष्टिसमनस्क सम्बन्धितत्वात्तिधा भवति तथापीह दीर्घकालिकोपदेशसञ्ज्ञा ग्राह्येति, सा यस्यास्ति स सञ्ज्ञीसमनस्कस्तस्य ज्ञानं सञ्ज्ञिज्ञानं तच्चे हा धिकृत सूत्राम्यथानुपपत्तेर्जातिस्मरणमेव ।
२. समवायांगवृत्ति पत्र १७ : स्मृतपूर्वभवस्य च संवेगात् समाधिरुत्पद्यते ।
३. समवायांगवृत्ति पत्र १७-१८ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org