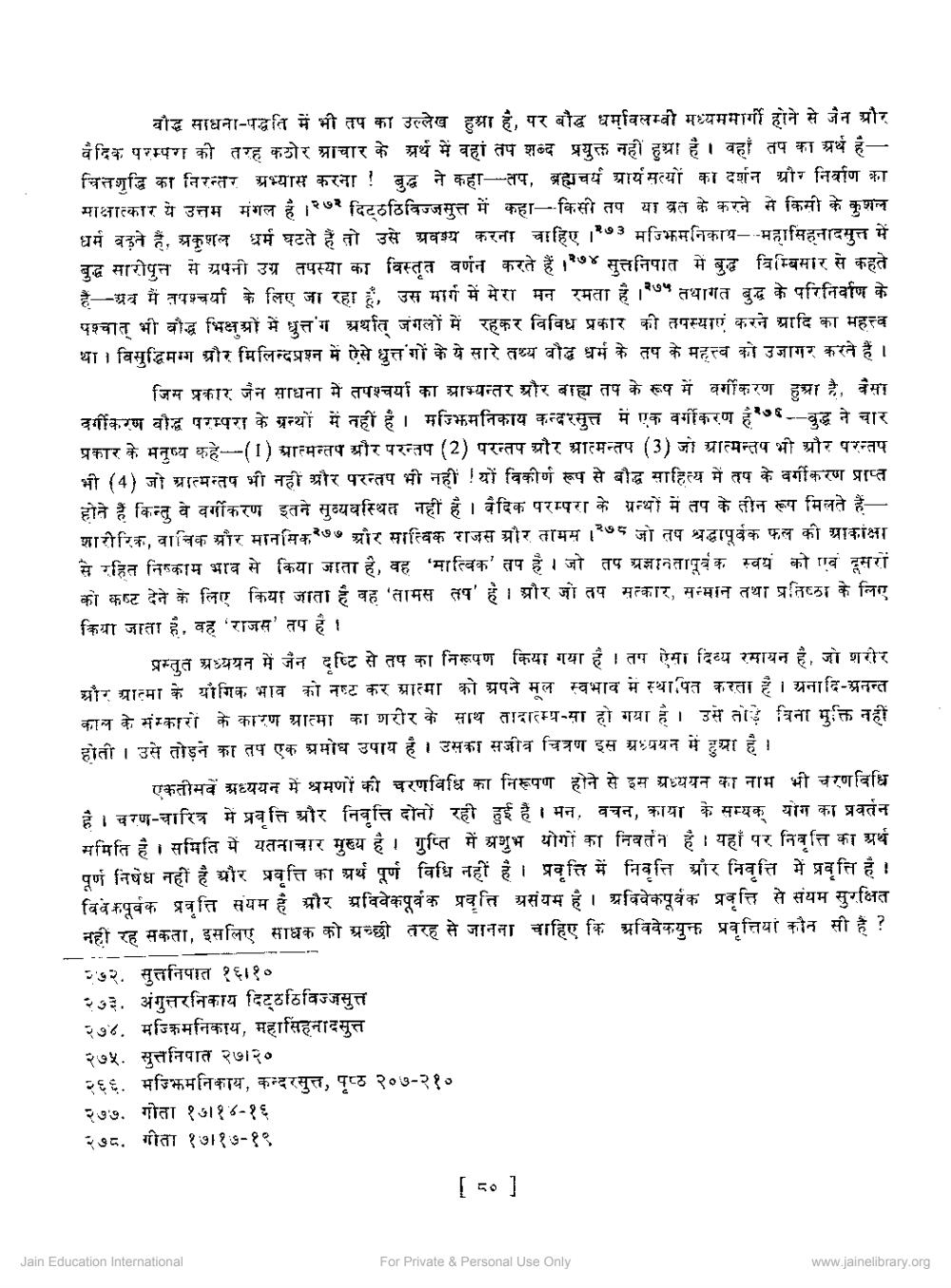________________ बौद्ध साधना-पद्धति में भी तप का उल्लेख हुन्मा है, पर बौद्ध धर्मावलम्बी मध्यममार्गी होने से जैन और वैदिक परम्परा की तरह कठोर आचार के अर्थ में वहां तप शब्द प्रयुक्त नहीं हया है। वहाँ तप का अर्थ हैचित्तशुद्धि का निरन्तर अभ्यास करना ! बुद्ध ने कहा--तप, ब्रह्मचर्य पार्यसत्यों का दर्शन और निर्वाण का माक्षात्कार ये उत्तम मंगल है / 272 दिठिविज्जसुत्त में कहा--किसी तप या व्रत के करने से किसी के कुशल धर्म बढ़ते हैं, अकुशल धर्म घटते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए / 273 मज्झिमनिकाय-महासिंहनादत्त में बुद्ध सारोपुत से अपनी उग्र तपस्या का विस्तृत वर्णन करते हैं / 274 सुत्तनिपात में बुद्ध विम्बिसार से कहते हैं--प्रव मैं तपश्चर्या के लिए जा रहा है, उस मार्ग में मेरा मन रमता है / 275 तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् भी बौद्ध भिक्षुओं में धुत्तग अर्थात जंगलों में रहकर विविध प्रकार की तपस्याएं करने आदि का महत्त्व था। विसुद्धिमम्ग और मिलिन्दप्रश्न में ऐसे धुत्तगों के ये सारे तथ्य बौद्ध धर्म के तप के महत्त्व को उजागर करते हैं। जिस प्रकार जैन साधना में तपश्चर्या का आभ्यन्तर और बाह्य तप के रूप में वर्गीकरण हुअा है, वैसा वर्गीकरण बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों में नहीं है। मज्झिमनिकाय कन्दरसुत्त में एक वर्गीकरण है ७६.-बुद्ध ने चार प्रकार के मनुष्य कहे--(1) आत्मन्तप और परन्तप (2) परन्तप और आत्मन्तप (3) जो प्रात्मन्तप भी और परन्तप भी (4) जो ग्रात्मन्तप भी नहीं और परन्तप भी नहीं ! यों विकीर्ण रूप से बौद्ध साहित्य में तप के वर्गीकरण प्राप्त होते हैं किन्तु वे वर्गीकरण इतने सुव्यवस्थित नहीं है। वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में तप के तीन रूप मिलते हैंशारीरिक, वानिक और मानसिक 77 और सात्विक राजस और तामम / 278 जो तप श्रद्धापूर्वक फल की प्राकांक्षा से रहित निष्काम भाव से किया जाता है, वह 'मात्विक' तप है। जो तप अज्ञानतापूर्वक स्वयं को व दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह 'तामस तप' है। और जो तप मत्कार, सन्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, वह 'राजस' तप है। प्रस्तुत अध्ययन में जैन दृष्टि से तप का निरूपण किया गया है / तप ऐमा दिव्य रमायन है, जो शरीर और प्रात्मा के यौगिक भाव को नष्ट कर आत्मा को अपने मूल स्वभाव में स्थापित करता है / अनादि-अनन्त काल के संस्कारों के कारण प्रात्मा का शरीर के साथ तादात्म्प-सा हो गया है। उसे तोड़े विना मुक्ति नहीं होती। उसे तोडने का तप एक अमोघ उपाय है। उसका सजीव चित्रण इस अध्ययन में सुना है। एकतीमवें अध्ययन में श्रमणों की चरणविधि का निरूपण होने से इस अध्ययन का नाम भी चरणविधि है। चरण-चारित्र में प्रवत्ति और निवृत्ति दोनों रही हुई हैं / मन, वचन, काया के सम्यक योग का प्रवर्तन ममिति है। समिति में यतनाचार मुख्य है। गुप्ति में अशुभ योगों का निवर्तन है। यहाँ पर निवत्ति का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है और प्रवृत्ति का अर्थ पूर्ण विधि नहीं है / प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति है। विवपूर्वक प्रवृत्ति संयम है और अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति असंयम है / अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति से संयम सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए साधक को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि अविवेकयुक्त प्रवृत्तियां कौन सी हैं ? 272. सुत्तनिपात 16 / 10 273. अंगुत्तरनिकाय दिठिविज्जसुत्त 274. मजिक्रमनिकाय, महासिंहनादसुत्त 275. सुत्तनिपात 27 / 20 266. मज्झिमनिकाय, कन्दरसुत, पृष्ठ 207-210 277. गोता 17 // 14-16 278. गीता 17.17-19 [80 ] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org