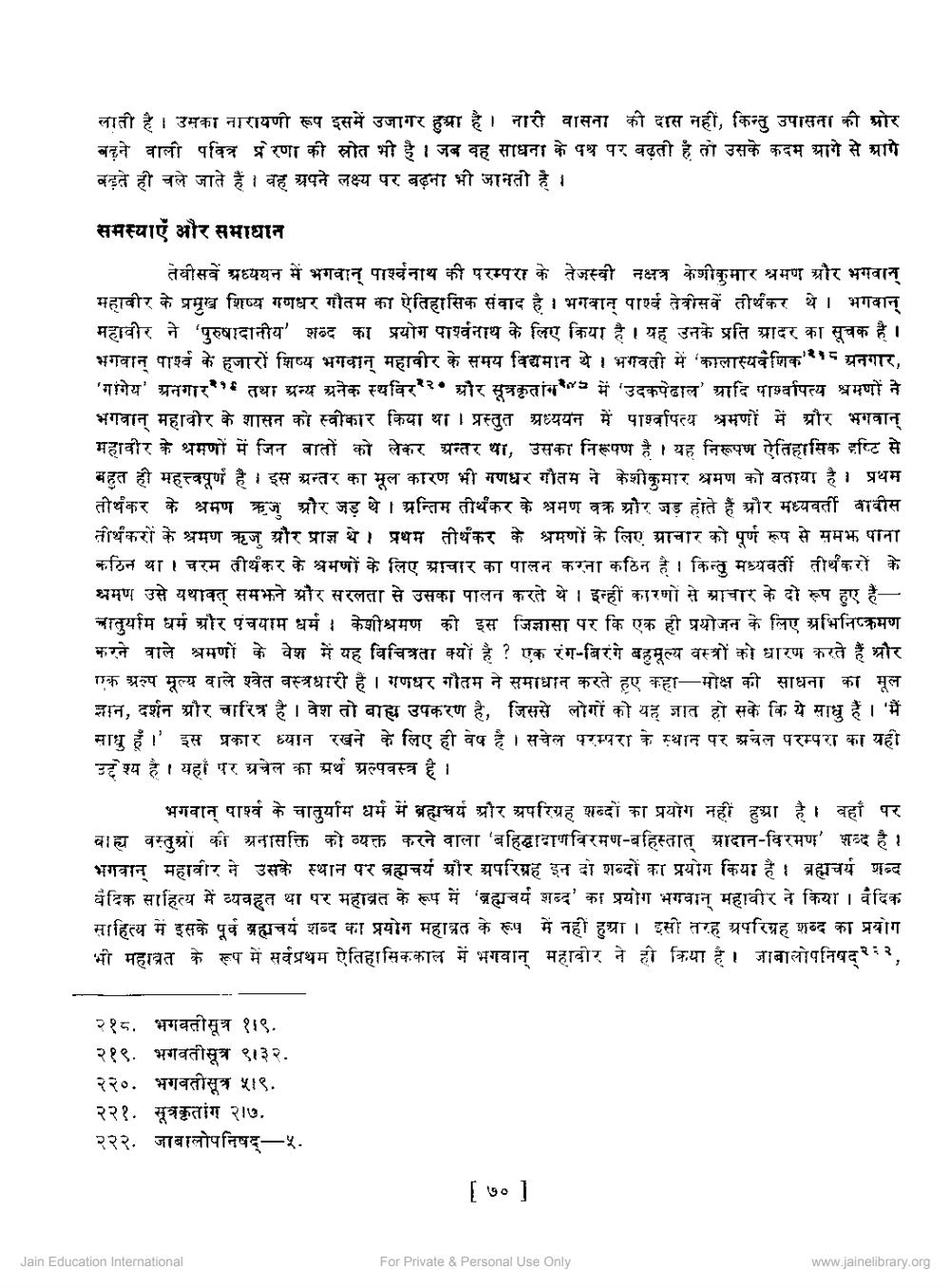________________ लाती है। उसका नारायणी रूप इसमें उजागर हुआ है। नारी वासना की दास नहीं, किन्तु उपासना की ओर बढ़ने वाली पवित्र प्रेरणा की स्रोत भी है। जब वह साधना के पथ पर बढ़ती है तो उसके कदम आगे से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। वह अपने लक्ष्य पर बढ़ना भी जानती है। समस्याएँ और समाधान तेवीसवें अध्ययन में भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा के तेजस्वी नक्षत्र केशीकूमार श्रमण और भगवान हावीर के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम का ऐतिहासिक संवाद है। भगवान पाच तेवीसवें तीर्थंकर थे / भगवान् महावीर ने 'पुरुषादानीय' शब्द का प्रयोग पार्श्वनाथ के लिए किया है। यह उनके प्रति अादर का सूचक है। भगवान पार्श्व के हजारों शिष्य भगवान महावीर के समय विद्यमान थे। भगवती में 'कालास्यवैशिक 18 अनगार, 'गांगेय' अनगार तथा अन्य अनेक स्थविर'२. और सूत्रकृतांग में 'उदकपेढाल' ग्रादि पाश्र्वापत्य श्रमणों ने भगवान् महावीर के शासन को स्वीकार किया था। प्रस्तुत अध्ययन में पापित्य श्रमणों में और भगवान् महावीर के श्रमणों में जिन बातों को लेकर अन्तर था, उसका निरूपण है / यह निरूपण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस अन्तर का मूल कारण भी गणधर गौतम ने केशीकुमार श्रमण को बताया है। प्रथम तीर्थकर के श्रमण ऋज और जड़ थे / अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण वक्र और जड़ होते हैं और मध्यवर्ती बावीस तीर्थंकरों के श्रमण ऋजु और प्राज्ञ थे। प्रथम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए प्राचार को पूर्ण रूप से समझ पाना कठिन था। चरम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए प्राचार का पालन करना कठिन है। किन्तु मध्यवती तीर्थंकरों के श्रमण उसे यथावत् समझने और सरलता से उसका पालन करते थे। इन्हीं कारणों से प्राचार के दो रूप हुए हैंचातुर्याम धर्म और पंचयाम धर्म / केशीश्रमण को इस जिज्ञासा पर कि एक ही प्रयोजन के लिए अभिनिष्क्रमण करने वाले श्रमणों के वेश में यह विचित्रता क्यों है ? एक रंग-बिरंगे बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करते हैं और एक अल्प मूल्य वाले श्वेत वस्त्रधारी हैं / गणधर गौतम ने समाधान करते हए कहा-मोक्ष की साधना का मूल ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। वेश तो बाह्य उपकरण है, जिससे लोगों को यह ज्ञात हो सके कि ये साधु हैं / 'मैं माधु हूँ।' इस प्रकार ध्यान रखने के लिए ही वेष है / सचेल परम्परा के स्थान पर अचल परम्परा का यही उद्देश्य है। यहाँ पर अचेल का अर्थ अल्पवस्त्र है। भगवान पार्श्व के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ पर बाह्य वस्तुओं की अनासक्ति को व्यक्त करने वाला 'बहिदादाणविरमण-बहिस्तात् आदान-विरमण' शब्द है। भगवान महावीर ने उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य शब्द वैदिक साहित्य में व्यवहृत था पर महाव्रत के रूप में 'ब्रह्मचर्य शब्द' का प्रयोग भगवान् महावीर ने किया / वैदिक साहित्य में इसके पूर्व ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग महावत के रूप में नहीं हुअा। इसी तरह अपरिग्रह शब्द का प्रयोग भी महावत के रूप में सर्वप्रथम ऐतिहासिक काल में भगवान महावीर ने ही क्रिया है। जाबालोपनिषदर 22. 218. भगवतीसूत्र 129. 219. भगवतीसूत्र 9 / 32. 220. भगवतीसूत्र 519. 221. सूत्रकृतांग 217. 222. जाबालोपनिषद-५. [70 ] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org