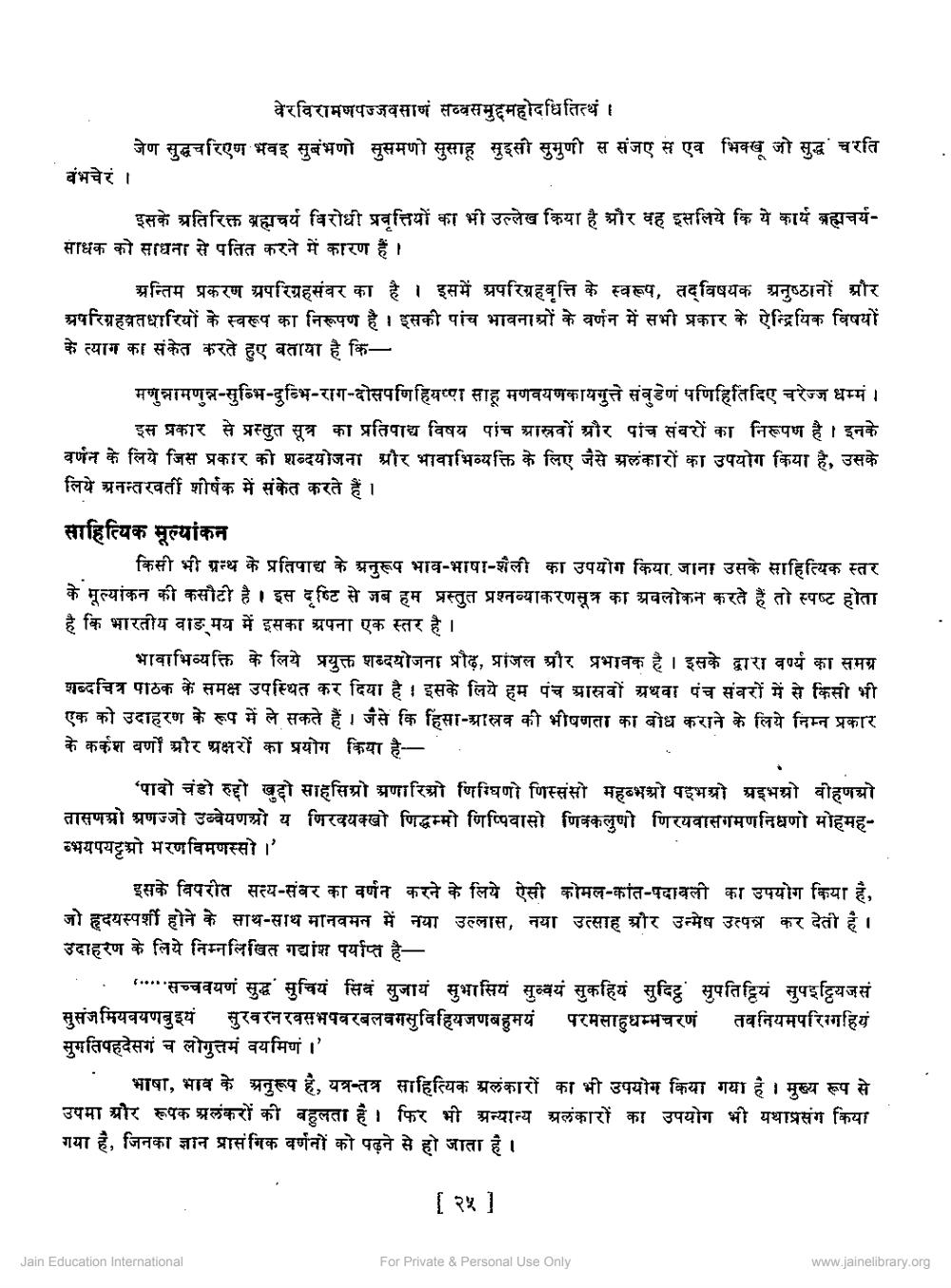________________ वेरविरामणपज्जवसाणं सव्वसमुद्दमहोदधितित्थं / जेण सुद्धचरिएण भवइ सुबंभणो सुसमणो सुसाहू सुइसी सुमुणी स संजए स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति बंभचेरं / इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य विरोधी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया है और वह इसलिये कि ये कार्य ब्रह्मचर्यसाधक को साधना से पतित करने में कारण हैं। अन्तिम प्रकरण अपरिग्रहसंबर का है / इसमें अपरिग्रहवृत्ति के स्वरूप, तद्विषयक अनुष्ठानों और अपरिग्रहवतधारियों के स्वरूप का निरूपण है। इसकी पांच भावनाओं के वर्णन में सभी प्रकार के ऐन्द्रियिक विषयों के त्याग का संकेत करते हुए बताया है कि मणुनामणुन्न-सुब्भि-दुन्भि-राग-दोसपणिहियप्पा साहू मणवयणकायगुत्ते संवुडेणं पणिहितिदिए चरेज्ज धम्म / इस प्रकार से प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य विषय पांच आस्रवों और पांच संवरों का निरूपण है। इनके वर्णन के लिये जिस प्रकार को शब्दयोजना और भावाभिव्यक्ति के लिए जैसे अलंकारों का उपयोग किया है, उसके लिये अनन्तरवर्ती शीर्षक में संकेत करते हैं। साहित्यिक मूल्यांकन किसी भी ग्रन्थ के प्रतिपाद्य के अनुरूप भाव-भाषा-शैली का उपयोग किया जाना उसके साहित्यिक स्तर के मूल्यांकन की कसौटी है। इस दृष्टि से जब हम प्रस्तुत प्रश्नव्याकरणसूत्र का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि भारतीय वाङमय में इसका अपना एक स्तर है / भावाभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त शब्दयोजना प्रौढ़, प्रांजल और प्रभावक है / इसके द्वारा वर्ण्य का समग्र शब्दचित्र पाठक के समक्ष उपस्थित कर दिया है। इसके लिये हम पंच प्रास्रवों अथवा पंच संवरों में से किसी भी एक को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि हिंसा-आस्रव की भीषणता का बोध कराने के लिये निम्न प्रकार के कर्कश बों और अक्षरों का प्रयोग किया है- . 'पावो चंडो रुद्दो खुद्दो साहसियो प्रणारियो णिग्घिणो णिस्संसो महब्भो पइभो अइभनो बोहणतो तासणो अणज्जो उब्वेयणो य गिरक्यक्खो णिद्धम्मो णिप्पिवासो णिक्कलुणो णिरयवासगमणनिधणो मोहमहउभयपयट्टो मरणविमणस्सो।' इसके विपरीत सत्य-संबर का वर्णन करने के लिये ऐसी कोमल-कांत-पदावली का उपयोग किया है, जो हृदयस्पर्शी होने के साथ-साथ मानवमन में नया उल्लास, नया उत्साह और उन्मेष उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित गद्यांश पर्याप्त है ..... 'सच्चवयणं सुद्ध सुचियं सिर्व सुजायं सुभासियं सुव्वयं सुकहियं सुदिटु सुपतिट्टियं सुपइट्टियजसं सुसंजमियवयणबुइयं सुरवरनरवसभपवरबलवगसुविहियजणबहुमयं परमसाहुधम्मचरणं तवनियमपरिग्गहियं सुमतिपहदेसगं च लोगुत्तमं वयमिणं / ' भाषा, भाव के अनुरूप है, यत्र-तत्र साहित्यिक अलंकारों का भी उपयोग किया गया है। मुख्य रूप से उपमा और रूपक अलंकरों की बहुलता है। फिर भी अन्यान्य अलंकारों का उपयोग भी यथाप्रसंग किया गया है, जिनका ज्ञान प्रासंगिक वर्णनों को पढ़ने से हो जाता है। [25] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org