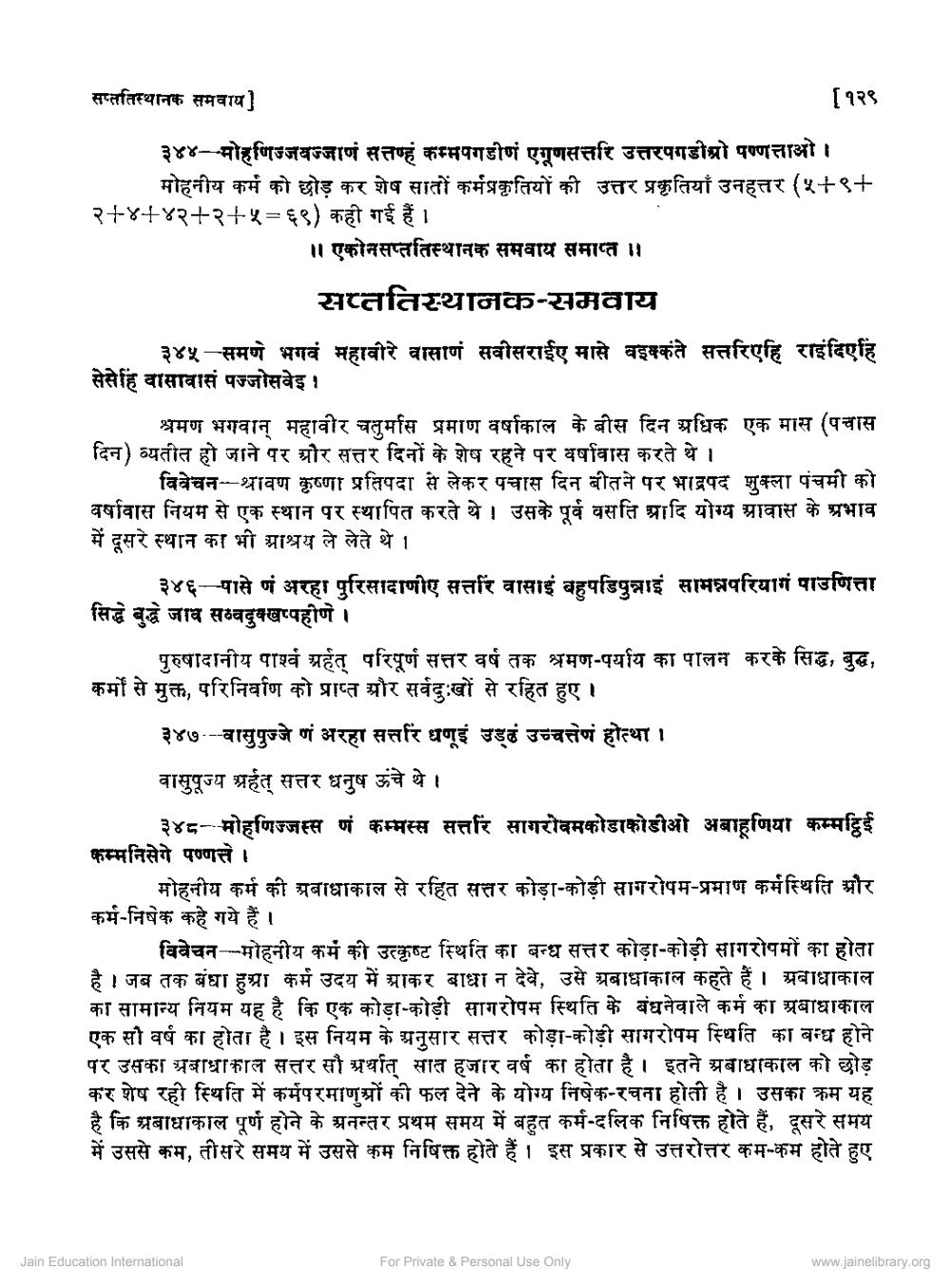________________ सप्ततिस्थानक समवाय] [129 ३४४-मोहणिज्जवज्जाणं सत्तण्हं कम्मपगडीणं एगूणसत्तरि उत्तरपगडीनो पण्णत्ताओ। मोहनीय कर्म को छोड़ कर शेष सातों कर्मप्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ उनहत्तर (5+9+ 2+4+42+2+5= 69) कही गई हैं। // एकोनसप्ततिस्थानक समवाय समाप्त / / सप्ततिस्थानक-समवाय ___३४५-समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसराईए मासे वइक्कते सत्तरिएहि राइंदिरहि सेसेहि वासावासं पज्जोसवेइ। श्रमण भगवान् महावीर चतुर्मास प्रमाण वर्षाकाल के बीस दिन अधिक एक मास (पचास दिन) व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिनों के शेष रहने पर वर्षावास करते थे। विवेचन-श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से लेकर पचास दिन बीतने पर भाद्रपद शुक्ला पंचमी को वर्षावास नियम से एक स्थान पर स्थापित करते थे। उसके पूर्व वसति प्रादि योग्य प्रावास के प्रभाव में दूसरे स्थान का भी आश्रय ले लेते थे। ___३४६-पासे णं अरहा पुरिसादाणीए सत्तर वासाई बहुपडिपुन्नाइं सामनपरियागं पाउणित्ता सिद्धे बुद्धे जाव सम्वदुक्खप्पहीणे / पुरुषादानीय पार्श्व अर्हत् परिपूर्ण सत्तर वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन करके सिद्ध, बुद्ध, कर्मों से मुक्त, परिनिर्वाण को प्राप्त और सर्वदुःखों से रहित हुए। 347 -वासुपुज्जे णं अरहा सरि धणूइं उड्ढं उच्चत्तेणं होत्था / वासुपूज्य अर्हत् सत्तर धनुष ऊंचे थे। ३४८--मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स सरि सागरोवमकोडाकोडीओ अबाहूणिया कम्मदिई कम्मनिसेगे पण्णत्ते। मोहनीय कर्म की अबाधाकाल से रहित सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम-प्रमाण कर्मस्थिति और कर्म-निषेक कहे गये हैं। विवेचन-मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपमों का होता है। जब तक बंधा हुआ कर्म उदय में आकर बाधा न देवे, उसे अबाधाकाल कहते हैं। अबाधाकाल का सामान्य नियम यह है कि एक कोड़ा-कोड़ी सागरोपम स्थिति के बंधनेवाले कर्म का अबाधाकाल एक सौ वर्ष का होता है / इस नियम के अनुसार सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपम स्थिति का बन्ध होने पर उसका अबाधाकाल सत्तर सौ अर्थात् सात हजार वर्ष का होता है। इतने अबाधाकाल को छोड़ कर शेष रही स्थिति में कर्मपरमाणुओं की फल देने के योग्य निषेक-रचना होती है। उसका क्रम यह है कि अबाधाकाल पूर्ण होने के अनन्तर प्रथम समय में बहुत कर्म-दलिक निषिक्त होते हैं, दूसरे समय में उससे कम, तीसरे समय में उससे कम निषिक्त होते हैं। इस प्रकार से उत्तरोत्तर कम-कम होते हुए Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org