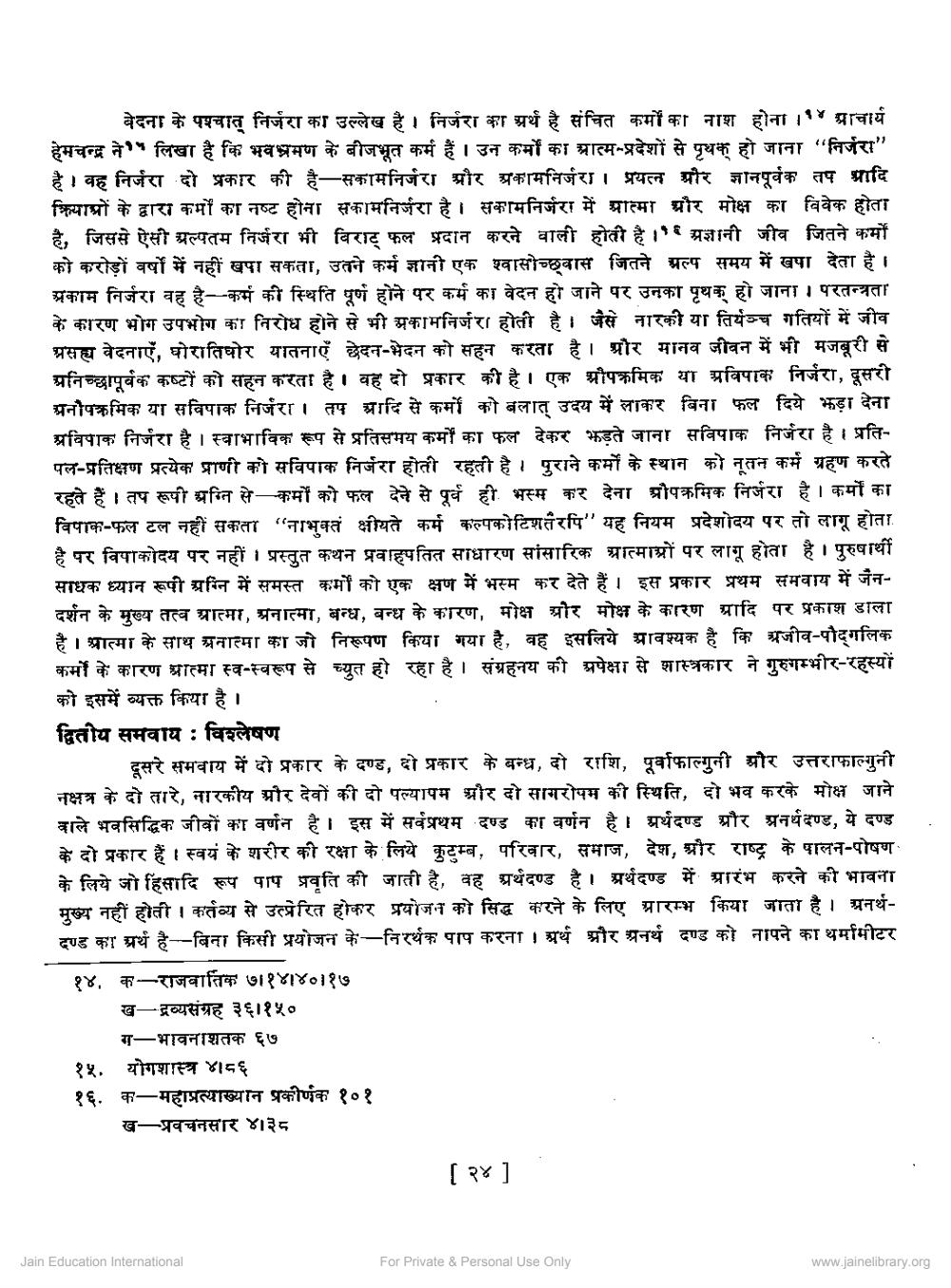________________ बेदना के पश्चात निर्जरा का उल्लेख है। निर्जरा का अर्थ है संचित कमों का नाश होना / / 4 प्राचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि भवभ्रमण के बीजभूत कर्म हैं। उन कर्मों का पात्म-प्रदेशों से पृथक हो जाना "निर्जरा" है। वह निर्जरा दो प्रकार की है-सकामनिर्जरा और अकामनिर्जरा। प्रयत्न और ज्ञानपूर्वक तप आदि क्रियाओं के द्वारा कर्मों का नष्ट होना सकामनिर्जरा है। सकामनिर्जरा में प्रात्मा और मोक्ष का विवेक होता है, जिससे ऐसी अल्पतम निर्जरा भी विराट् फल प्रदान करने वाली होती है। अज्ञानी जीव जितने कर्मों को करोड़ों वर्षों में नहीं खपा सकता, उतने कर्म ज्ञानी एक श्वासोच्छ्वास जितने अल्प समय में खपा देता है / अकाम निर्जरा वह है--कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर कर्म का वेदन हो जाने पर उनका पृथक हो जाना / परतन्त्रता के कारण भोग उपभोग का निरोध होने से भी प्रकामनिर्जरा होती है। जैसे नारकी या तिर्यञ्च गतियों में जीव असह्य वेदनाएँ, घोरातिघोर यातनाएँ छेदन-भेदन को सहन करता है। और मानव जीवन में भी मजबूरी से अनिच्छापूर्वक कष्टों को सहन करता है। वह दो प्रकार की है। एक औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा, दूसरी अनौपक्रमिक या सविपाक निर्जरा। तप आदि से कर्मों को बलात् उदय में लाकर बिना फल दिये झड़ा देना अविपाक निर्जरा है। स्वाभाविक रूप से प्रतिसमय कर्मों का फल देकर झड़ते जाना सविपाक निर्जरा है। प्रतिपल-प्रतिक्षण प्रत्येक प्राणी को सविपाक निर्जरा होती रहती है। पुराने कर्मों के स्थान को नूतन कर्म ग्रहण करते रहते हैं। तप रूपी अग्नि से—कर्मों को फल देने से पूर्व ही भस्म कर देना प्रौपक्रमिक निर्जरा है। कर्मों का विपाक-फल टल नहीं सकता "नाभक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरपि" यह नियम प्रदेशोदय पर तो लागू होता है पर विपाकोदय पर नहीं। प्रस्तुत कथन प्रवाहपतित साधारण सांसारिक अात्माओं पर लागू होता है। पुरुषार्थी साधक ध्यान रूपी अग्नि में समस्त कर्मों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। इस प्रकार प्रथम समवाय में जैनदर्शन के मुख्य तत्व प्रात्मा, अनात्मा, बन्ध, बन्ध के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण प्रादि पर प्रकाश डाला है / प्रात्मा के साथ अनात्मा का जो निरूपण किया गया है, वह इसलिये आवश्यक है कि अजीव-पौद्गलिक कर्मों के कारण प्रात्मा स्व-स्वरूप से च्युत हो रहा है। संग्रहनय की अपेक्षा से शास्त्रकार ने गुरुगम्भीर-रहस्यों को इसमें व्यक्त किया है। द्वितीय समवाय : विश्लेषण दूसरे समवाय में दो प्रकार के दण्ड, दो प्रकार के बन्ध, दो राशि, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के दो तारे, नारकीय और देवों की दो पल्यापम और दो सागरोपम की स्थिति, दो भव करके मोक्ष जाने वाले भवसिद्धिक जीवों का वर्णन है। इस में सर्वप्रथम दण्ड का वर्णन है। अर्थदण्ड और अनर्थदण्ड, ये दण्ड के दो प्रकार हैं / स्वयं के शरीर की रक्षा के लिये कुटुम्ब, परिवार, समाज, देश, और राष्ट्र के पालन-पोषण के लिये जो हिंसादि रूप पाप प्रवृति की जाती है, वह अर्थदण्ड है। अर्थदण्ड में प्रारंभ करने की भावना मुख्य नहीं होती / कर्तव्य से उत्प्रेरित होकर प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रारम्भ किया जाता है। अनर्थदण्ड का अर्थ है--बिना किसी प्रयोजन के-निरर्थक पाप करना / अर्थ और अनर्थ दण्ड को नापने का थर्मामीटर . 14. क-राजवार्तिक 7 / 14 / 40 / 17 ख-द्रव्यसंग्रह 36 / 150 ग-भावनाशतक 67 15. योगशास्त्र 486 16. क-महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक 101 ख-प्रवचनसार 4 / 38 [24] Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org