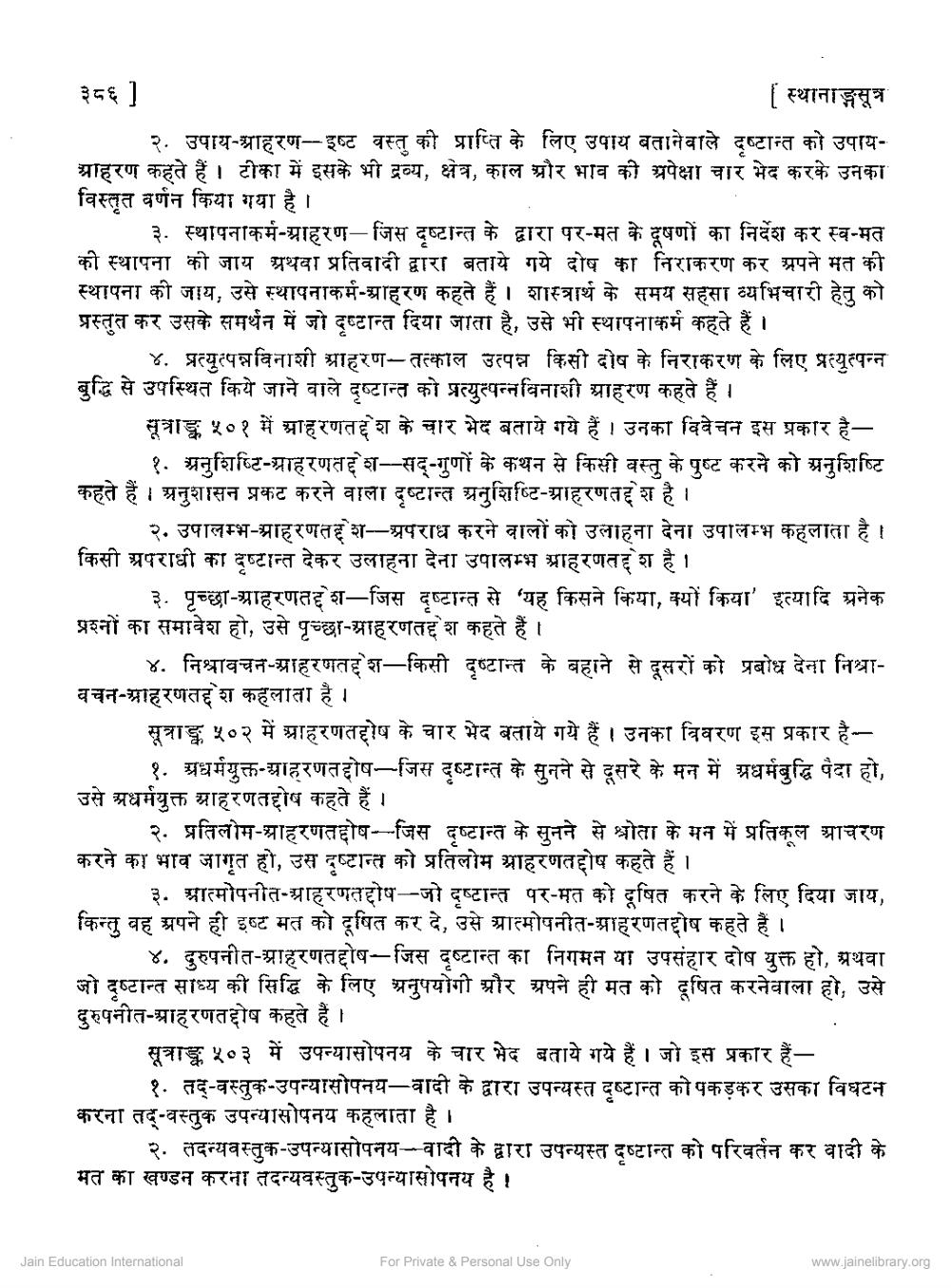________________ 386 ] [ स्थानाङ्गसूत्र 2. उपाय-बाहरण-इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए उपाय बतानेवाले दृष्टान्त को उपायआहरण कहते हैं। टीका में इसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चार भेद करके उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। 3. स्थापनाकर्म-ग्राहरण—जिस दृष्टान्त के द्वारा पर-मत के दूषणों का निर्देश कर स्व-मत की स्थापना की जाय अथवा प्रतिवादी द्वारा बताये गये दोष का निराकरण कर अपने मत की स्थापना की जाय, उसे स्थापनाकर्म-आहरण कहते हैं। शास्त्रार्थ के समय सहसा व्यभिचारी हेतु को प्रस्तुत कर उसके समर्थन में जो दृष्टान्त दिया जाता है, उसे भी स्थापनाकर्म कहते हैं। 4. प्रत्युत्पन्नविनाशी आहरण-तत्काल उत्पन्न किसी दोष के निराकरण के लिए प्रत्युत्पन्न बुद्धि से उपस्थित किये जाने वाले दृष्टान्त को प्रत्युत्पन्नविनाशी पाहरण कहते हैं / सूत्राङ्क 501 में आहरणतद्देश के चार भेद बताये गये हैं। उनका विवेचन इस प्रकार है 1. अनुशिष्टि-पाहरणतद्देश-सद्-गुणों के कथन से किसी वस्तु के पुष्ट करने को अनुशिष्टि कहते हैं / अनुशासन प्रकट करने वाला दृष्टान्त अनुशिष्टि-पाहरणतद्दे श है / 2. उपालम्भ-आहरणतद्देश-अपराध करने वालों को उलाहना देना उपालम्भ कहलाता है। किसी अपराधी का दृष्टान्त देकर उलाहना देना उपालम्भ आहरणतद्देश है। 3. पृच्छा-आहरणतद्देश-जिस दृष्टान्त से 'यह किसने किया, क्यों किया' इत्यादि अनेक प्रश्नों का समावेश हो, उसे पृच्छा-अाहरणतद्देश कहते हैं / 4. निश्रावचन-अाहरणतद्देश-किसी दृष्टान्त के बहाने से दूसरों को प्रबोध देना निश्रावचन-पाहरणतद्देश कहलाता है / सूत्राङ्क 502 में प्राहरणतद्दोष के चार भेद बताये गये हैं। उनका विवरण इस प्रकार है 1. अधर्मयुक्त-बाहरणतद्दोष-जिस दृष्टान्त के सुनने से दूसरे के मन में अधर्मबुद्धि पैदा हो, उसे अधर्मयुक्त आहरणतद्दोष कहते हैं / 2. प्रतिलोम-बाहरणतद्दोष-जिस दृष्टान्त के सुनने से श्रोता के मन में प्रतिकूल आचरण करने का भाव जागृत हो, उस दृष्टान्त को प्रतिलोम आहरणतद्दोष कहते हैं / 3. आत्मोपनीत-पाहरणतद्दोष--जो दृष्टान्त पर-मत को दूषित करने के लिए दिया जाय, किन्तु वह अपने ही इष्ट मत को दूषित कर दे, उसे आत्मोपनीत-आहरणतदोष कहते हैं / 4. दुरुपनीत-आहरणतद्दोष-जिस दृष्टान्त का निगमन या उपसंहार दोष युक्त हो, अथवा जो दृष्टान्त साध्य की सिद्धि के लिए अनुपयोगी और अपने ही मत को दूषित करनेवाला हो, उसे दुरुपनीत-अाहरणतद्दोष कहते हैं / सूत्राङ्क 503 में उपन्यासोपनय के चार भेद बताये गये हैं / जो इस प्रकार हैं 1. तद्-वस्तुक-उपन्यासोपनय-वादी के द्वारा उपन्यस्त दृष्टान्त को पकड़कर उसका विघटन करना तद्-वस्तुक उपन्यासोपनय कहलाता है। 2. तदन्यवस्तुक-उपन्यासोपनय-वादी के द्वारा उपन्यस्त दृष्टान्त को परिवर्तन कर वादी के मत का खण्डन करना तदन्यवस्तुक-उपन्यासोपनय है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org