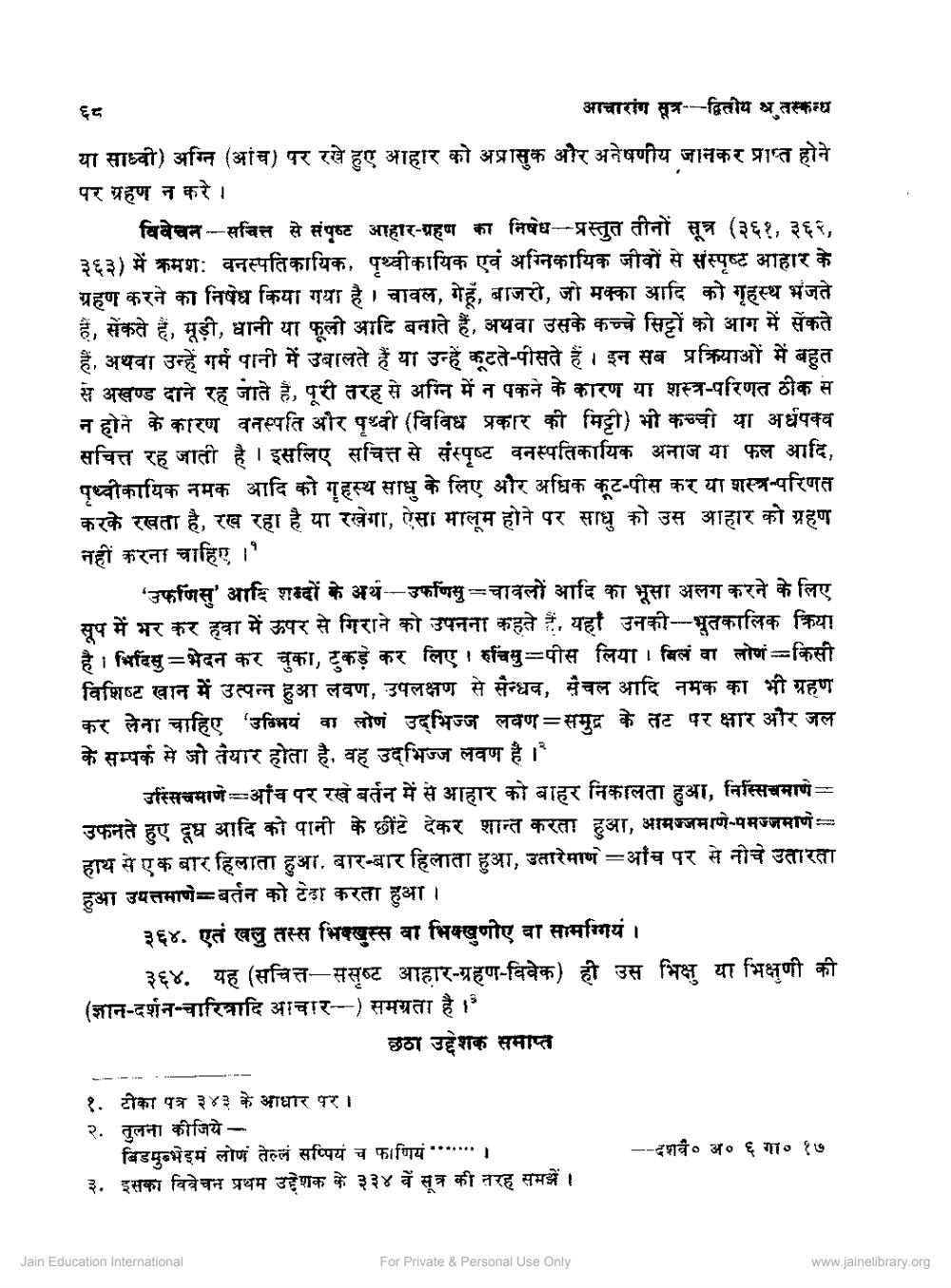________________ आचारांग सूत्र--द्वितीय श्रु तस्कन्ध या साध्वी) अग्नि (आंच) पर रखे हुए आहार को अप्रासुक और अनेषणीय जानकर प्राप्त होने पर ग्रहण न करे। विवेचन--सचित्त से संपृष्ट आहार-ग्रहण का निषेध--प्रस्तुत तीनों सूत्र (361, 362, 363) में क्रमश: वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिक एवं अग्निकायिक जीवों से संस्पृष्ट आहार के ग्रहण करने का निषेध किया गया है। चावल, गेहूँ, बाजरी, जो मक्का आदि को गृहस्थ भजते हैं, सेंकते हैं, मूड़ी, धानी या फूलो आदि बनाते हैं, अथवा उसके कच्चे सिट्टों को आग में सेंकते हैं, अथवा उन्हें गर्म पानी में उबालते हैं या उन्हें कटते-पीसते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में बहुत से अखण्ड दाने रह जाते हैं, पूरी तरह से अग्नि में न पकने के कारण या शस्त्र-परिणत ठीक स न होने के कारण वनस्पति और पृथ्वी (विविध प्रकार की मिट्टी) भी कच्ची या अर्धपक्व सचित्त रह जाती है / इसलिए सचित्त से संस्पृष्ट वनस्पतिकायिक अनाज या फल आदि, पृथ्वीकायिक नमक आदि को गृहस्थ साधु के लिए और अधिक कूट-पीस कर या शस्त्र-परिणत करके रखता है, रख रहा है या रखेगा, ऐसा मालूम होने पर साधु को उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए।' 'उणिसु' आदि शब्दों के अर्थ-उणिसु =चावलों आदि का भूसा अलग करने के लिए सूप में भर कर हवा में ऊपर से गिराने को उपनना कहते हैं. यहाँ उनकी-भुतकालिक क्रिया है। भिदिसु =भेदन कर चुका, टुकड़े कर लिए / चिसुपीस लिया। बिलं वा लोणं-किसी विशिष्ट खान में उत्पन्न हुआ लवण, उपलक्षण से सैन्धव, सैचल आदि नमक का भी ग्रहण कर लेना चाहिए 'उभियं वा लोणं उद्भिज्ज लवण =समुद्र के तट पर क्षार और जल के सम्पर्क से जो तैयार होता है, वह उद्भिज्ज लवण है / ' उस्सिवमाणे-आंच पर रखे बर्तन में से आहार को बाहर निकालता हुआ, निस्सिचमाणे = उफनते हुए दूध आदि को पानी के छींटे देकर शान्त करता हुआ, आमज्जमाणे-पमज्जमाणेहाथ से एक बार हिलाता हुआ, बार-बार हिलाता हुआ, उतारेमाण =आंच पर से नीचे उतारता हुआ उयत्तमाणे-बर्तन को टेढा करता हुआ। 364. एतं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणोए वा सामग्गियं / / ___ 364. यह (सचित्त-ससृष्ट आहार-ग्रहण-विवेक) ही उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञान-दर्शन-चारित्रादि आचार---) समग्रता है।' छठा उद्देशक समाप्त 1. टीका पत्र 343 के आधार पर। 2. तुलना कीजिये बिडमुन्भेइमं लोणं तेल्लं सप्पियं च फाणियं.......। 3. इसका विवेचन प्रथम उद्देशक के 334 वें सूत्र की तरह समझें / --दशवै० अ० 6 गा० 17 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org