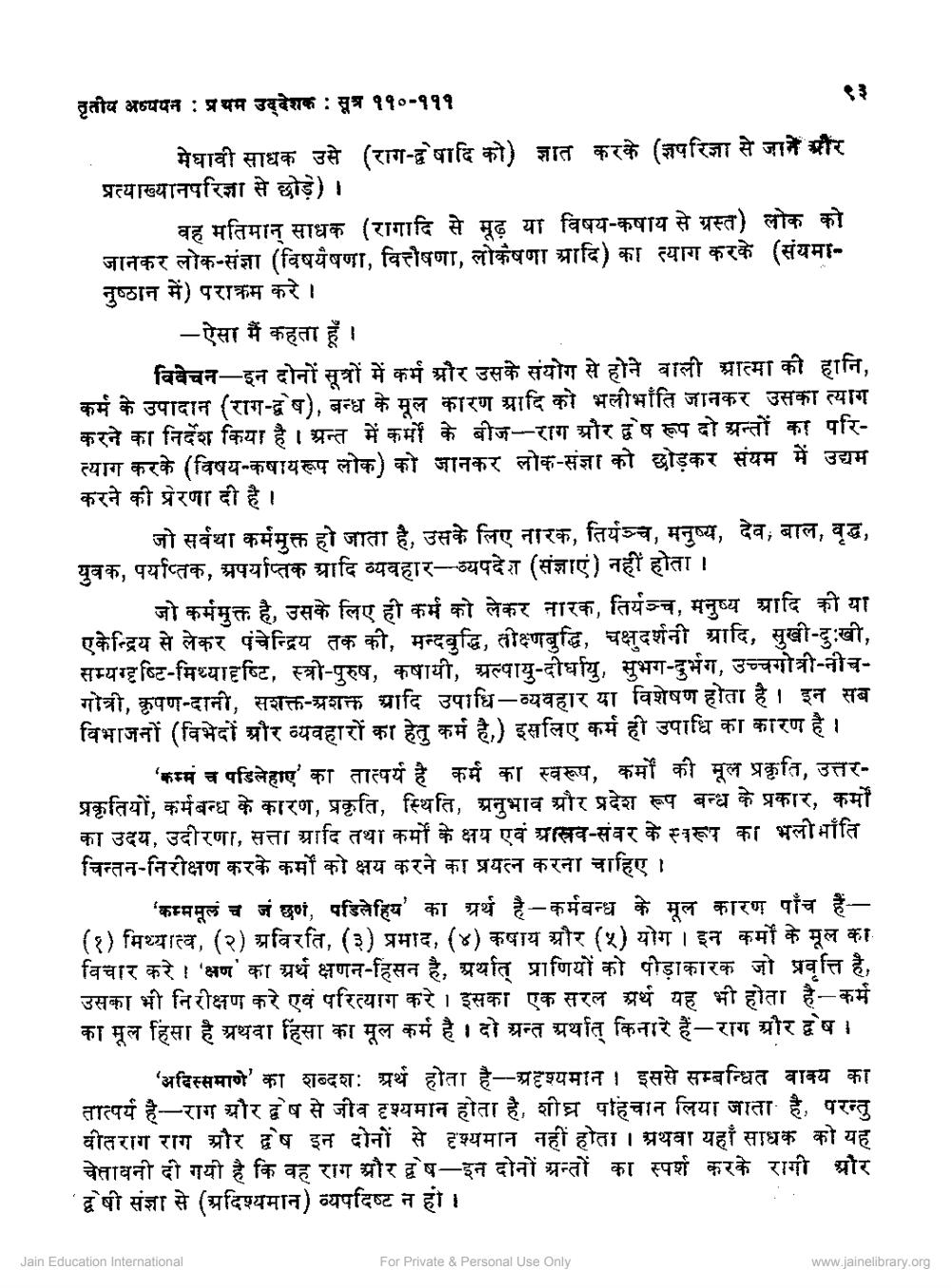________________ तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सूत्र 110-111 मेघावी साधक उसे (राग-द्वषादि को) ज्ञात करके (ज्ञपरिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोड़े)। वह मतिमान् साधक (रागादि से मूढ़ या विषय-कषाय से ग्रस्त) लोक को जानकर लोक-संज्ञा (विषयैषणा, वित्तौषणा, लोकषणा आदि) का त्याग करके (संयमानुष्ठान में) पराक्रम करे। -ऐसा मैं कहता हूँ। विवेचन-इन दोनों सूत्रों में कर्म और उसके संयोग से होने वाली प्रात्मा की हानि, कर्म के उपादान (राग-द्वष), बन्ध के मूल कारण आदि को भलीभाँति जानकर उसका त्याग करने का निर्देश किया है / अन्त में कर्मों के बीज-राग और द्वष रूप दो अन्तों का परित्याग करके (विषय-कषायरूप लोक) को जानकर लोक-संज्ञा को छोड़कर संयम में उद्यम करने की प्रेरणा दी है। जो सर्वथा कर्ममुक्त हो जाता है, उसके लिए नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, बाल, वृद्ध, युवक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक प्रादि व्यवहार-व्यपदेश (संज्ञाएं) नहीं होता / ___ जो कर्ममुक्त है, उसके लिए ही कर्म को लेकर नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि की या एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की, मन्दबुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि, चक्षुदर्शनी आदि, सुखी-दुःखी, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि, स्त्री-पुरुष, कषायी, अल्पायु-दीर्घायु, सुभग-दुर्भग, उच्चगोत्री-नीचगोत्री, कृपण-दानी, सशक्त-अशक्त आदि उपाधि-व्यवहार या विशेषण होता है। इन सब विभाजनों (विभेदों और व्यवहारों का हेतु कर्म है,) इसलिए कर्म ही उपाधि का कारण है / __ 'कम्मं च पडिलेहाए' का तात्पर्य है कर्म का स्वरूप, कर्मों की मूल प्रकृति, उत्तरप्रकृतियों, कर्मबन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप बन्ध के प्रकार, कर्मों का उदय, उदीरणा, सत्ता प्रादि तथा कर्मों के क्षय एवं प्रास्रव-संवर के स्वरूप का भलीभाँति चिन्तन-निरीक्षण करके कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। _ 'कम्ममूलं च जं छणं, पडिलेहिय' का अर्थ है- कर्मबन्ध के मूल कारण पाँच हैं(१) मिथ्यात्व, (2) अविरति, (3) प्रमाद, (4) कषाय और (5) योग / इन कर्मों के मूल का विचार करे / 'क्षण' का अर्थ क्षणन-हिंसन है, अर्थात् प्राणियों को पीड़ाकारक जो प्रवृत्ति है, उसका भी निरीक्षण करे एवं परित्याग करे / इसका एक सरल अर्थ यह भी होता है-कर्म का मूल हिंसा है अथवा हिंसा का मूल कर्म है / दो अन्त अर्थात् किनारे हैं-राग और द्वेष / / ____ 'अदिस्समाणे' का शब्दशः अर्थ होता है-अदृश्यमान। इससे सम्बन्धित वाक्य का तात्पर्य है-राग और द्वेष से जीव दृश्यमान होता है, शीघ्र पहिचान लिया जाता है, परन्तु वीतराग राग और द्वष इन दोनों से दृश्यमान नहीं होता / अथवा यहाँ साधक को यह चेतावनी दी गयी है कि वह राग और द्वष—इन दोनों अन्तों का स्पर्श करके रागी और 'द्वषी संज्ञा से (अदिश्यमान) व्यपदिष्ट न हो। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org