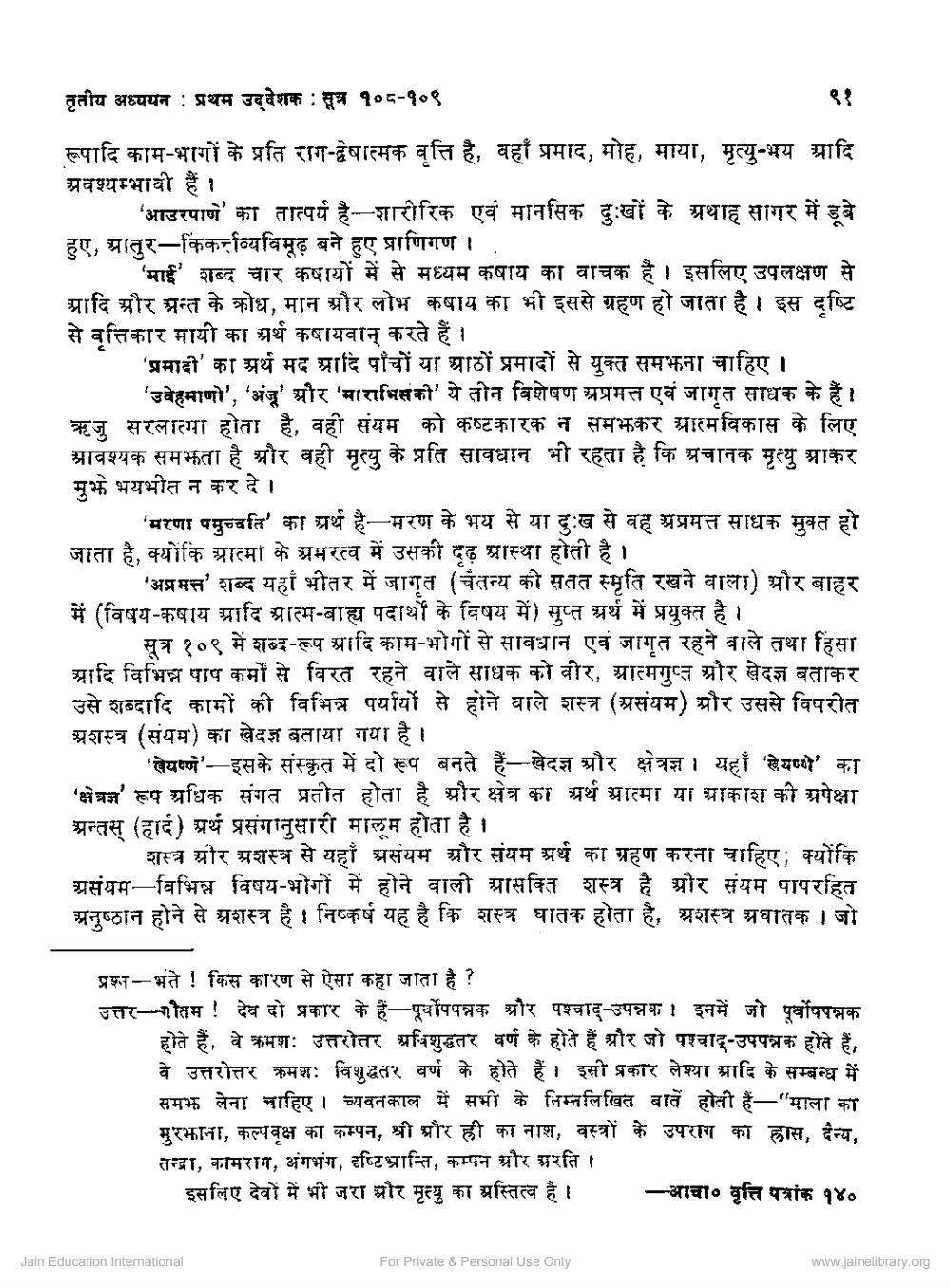________________ तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सूत्र 108-109 रूपादि काम-भागों के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वहाँ प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि अवश्यम्भावी हैं। 'आउरपाणे का तात्पर्य है-शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के अथाह सागर में डूबे हुए, पातुर-किंकर्तव्यविमूढ़ बने हुए प्राणिगण / 'माई' शब्द चार कषायों में से मध्यम कषाय का वाचक है। इसलिए उपलक्षण से आदि और अन्त के क्रोध, मान और लोभ कषाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि से वृत्तिकार मायी का अर्थ कषायवान् करते हैं। 'प्रमादी' का अर्थ मद आदि पाँचों या आठों प्रमादों से युक्त समझना चाहिए। 'उवेहमाणो', 'अंजू' और 'माराभिसको' ये तीन विशेषण अप्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। ऋजु सरलात्मा होता है, वही संयम को कष्टकारक न समझकर प्रारमविकास के लिए आवश्यक समझता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अचानक मृत्यु पाकर मुझे भयभीत न कर दे। 'मरणा पमुच्चति' का अर्थ है-मरण के भय से या दुःख से वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रात्मा के अमरत्व में उसकी दृढ़ प्रास्था होती है। 'अप्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर में (विषय-कषाय आदि आत्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) सुप्त अर्थ में प्रयुक्त है। सूत्र 109 में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिंसा आदि विभिन्न पाप कर्मों से विरत रहने वाले साधक को वीर, आत्मगुप्त और खेदज्ञ बताकर उसे शब्दादि कामों की विभिन्न पर्यों से होने वाले शस्त्र (असंयम) और उससे विपरीत प्रशस्त्र (संयम) का खेदज्ञ बताया गया है। ___ 'खेयपणे'—इसके संस्कृत में दो रूप बनते हैं-खेदज्ञ और क्षेत्रज्ञ। यहाँ 'खेयण्णे' का 'क्षेत्रज रूप अधिक संगत प्रतीत होता है और क्षेत्र का अर्थ आत्मा या आकाश की अपेक्षा अन्तस् (हार्द) अर्थ प्रसंगानुसारी मालम होता है। शस्त्र और प्रशस्त्र से यहाँ असंयम और संयम अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि असंयम-विभिन्न विषय-भोगों में होने वाली प्रासक्ति शस्त्र है और संयम पापरहित अनुष्ठान होने से प्रशस्त्र है / निष्कर्ष यह है कि शस्त्र घातक होता है, अशस्त्र अघातक / जो प्रश्न-भते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? उत्तर-गौतम ! देव दो प्रकार के हैं—पूर्वोपपन्नक और पश्चाद्-उपन्नक। इनमें जो पूर्वोपपन्नक होते हैं, वे क्रमशः उत्तरोत्तर अविशुद्धतर वर्ण के होते हैं और जो पश्चाद्-उपपन्नक होते हैं, वे उत्तरोत्तर क्रमशः विशुद्धतर वर्ग के होते हैं। इसी प्रकार लेश्या आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। च्यवनकाल में सभी के निम्नलिखित बातें होती हैं-"माला का मुरझाना, कल्पवृक्ष का कम्पन, श्री और ह्री का नाश, वस्त्रों के उपराग का ह्रास, दैन्य, तन्द्रा, कामराग, अंगभंग, दृष्टिभ्रान्ति, कम्पन और अरति / इसलिए देवों में भी जरा और मृत्यु का अस्तित्व है। -आचा० वृत्ति पत्रांक 140 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org