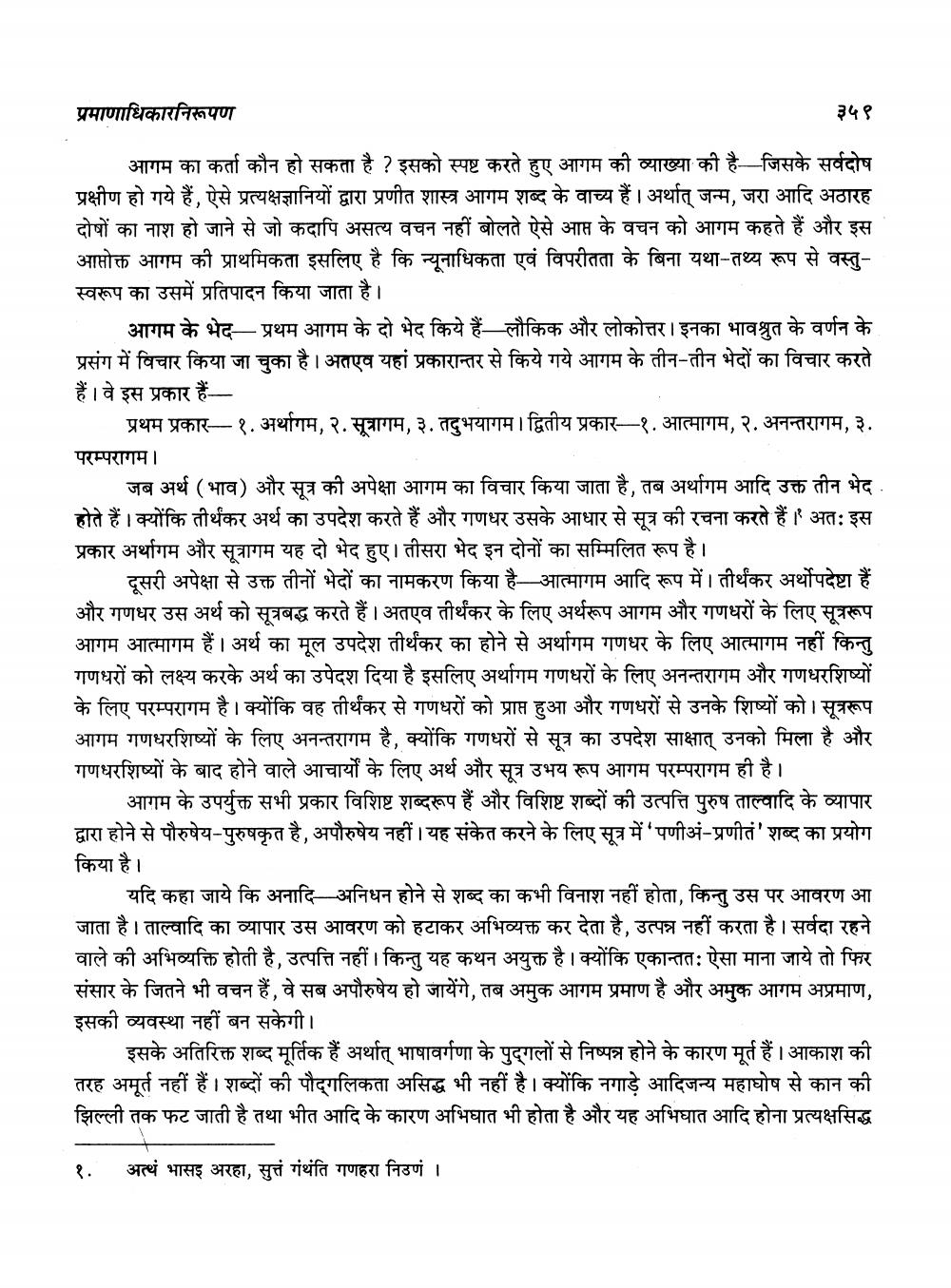________________
प्रमाणाधिकारनिरूपण
३५९
आगम का कर्ता कौन हो सकता है ? इसको स्पष्ट करते हुए आगम की व्याख्या की है जिसके सर्वदोष प्रक्षीण हो गये हैं, ऐसे प्रत्यक्षज्ञानियों द्वारा प्रणीत शास्त्र आगम शब्द के वाच्य हैं । अर्थात् जन्म, जरा आदि अठारह दोषों का नाश हो जाने से जो कदापि असत्य वचन नहीं बोलते ऐसे आप्त के वचन को आगम कहते हैं और इस आप्तोक्त आगम की प्राथमिकता इसलिए है कि न्यूनाधिकता एवं विपरीतता के बिना यथा-तथ्य रूप से वस्तुस्वरूप का उसमें प्रतिपादन किया जाता है।
आगम के भेद— प्रथम आगम के दो भेद किये हैं—लौकिक और लोकोत्तर । इनका भावश्रुत के वर्णन के प्रसंग में विचार किया जा चुका है। अतएव यहां प्रकारान्तर से किये गये आगम के तीन-तीन भेदों का विचार करते हैं । वे इस प्रकार हैं
प्रथम प्रकार- १. अर्थागम, २. सूत्रागम, ३. तदुभयागम। द्वितीय प्रकार—१. आत्मागम, २. अनन्तरागम, ३. परम्परागम।
जब अर्थ (भाव) और सूत्र की अपेक्षा आगम का विचार किया जाता है, तब अर्थागम आदि उक्त तीन भेद होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर अर्थ का उपदेश करते हैं और गणधर उसके आधार से सूत्र की रचना करते हैं। अतः इस प्रकार अर्थागम और सूत्रागम यह दो भेद हुए। तीसरा भेद इन दोनों का सम्मिलित रूप है।
दूसरी अपेक्षा से उक्त तीनों भेदों का नामकरण किया है—आत्मागम आदि रूप में। तीर्थंकर अर्थोपदेष्टा हैं और गणधर उस अर्थ को सूत्रबद्ध करते हैं । अतएव तीर्थंकर के लिए अर्थरूप आगम और गणधरों के लिए सूत्ररूप आगम आत्मागम हैं। अर्थ का मूल उपदेश तीर्थंकर का होने से अर्थागम गणधर के लिए आत्मागम नहीं किन्तु गणधरों को लक्ष्य करके अर्थ का उपेदश दिया है इसलिए अर्थागम गणधरों के लिए अनन्तरागम और गणधरशिष्यों के लिए परम्परागम है। क्योंकि वह तीर्थंकर से गणधरों को प्राप्त हुआ और गणधरों से उनके शिष्यों को। सूत्ररूप आगम गणधरशिष्यों के लिए अनन्तरागम है, क्योंकि गणधरों से सूत्र का उपदेश साक्षात् उनको मिला है और गणधरशिष्यों के बाद होने वाले आचार्यों के लिए अर्थ और सूत्र उभय रूप आगम परम्परागम ही है।
आगम के उपर्युक्त सभी प्रकार विशिष्ट शब्दरूप हैं और विशिष्ट शब्दों की उत्पत्ति पुरुष ताल्वादि के व्यापार द्वारा होने से पौरुषेय-पुरुषकृत है, अपौरुषेय नहीं। यह संकेत करने के लिए सूत्र में 'पणीअं-प्रणीतं' शब्द का प्रयोग किया है।
यदि कहा जाये कि अनादि अनिधन होने से शब्द का कभी विनाश नहीं होता, किन्तु उस पर आवरण आ जाता है। ताल्वादि का व्यापार उस आवरण को हटाकर अभिव्यक्त कर देता है, उत्पन्न नहीं करता है। सर्वदा रहने वाले की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं। किन्तु यह कथन अयुक्त है। क्योंकि एकान्ततः ऐसा माना जाये तो फिर संसार के जितने भी वचन हैं, वे सब अपौरुषेय हो जायेंगे, तब अमुक आगम प्रमाण है और अमुक आगम अप्रमाण, इसकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी।
इसके अतिरिक्त शब्द मूर्तिक हैं अर्थात् भाषावर्गणा के पुद्गलों से निष्पन्न होने के कारण मूर्त हैं। आकाश की तरह अमूर्त नहीं हैं। शब्दों की पौद्गलिकता असिद्ध भी नहीं है। क्योंकि नगाड़े आदिजन्य महाघोष से कान की झिल्ली तक फट जाती है तथा भीत आदि के कारण अभिघात भी होता है और यह अभिघात आदि होना प्रत्यक्षसिद्ध
१.
अत्थं भासइ अरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउणं ।