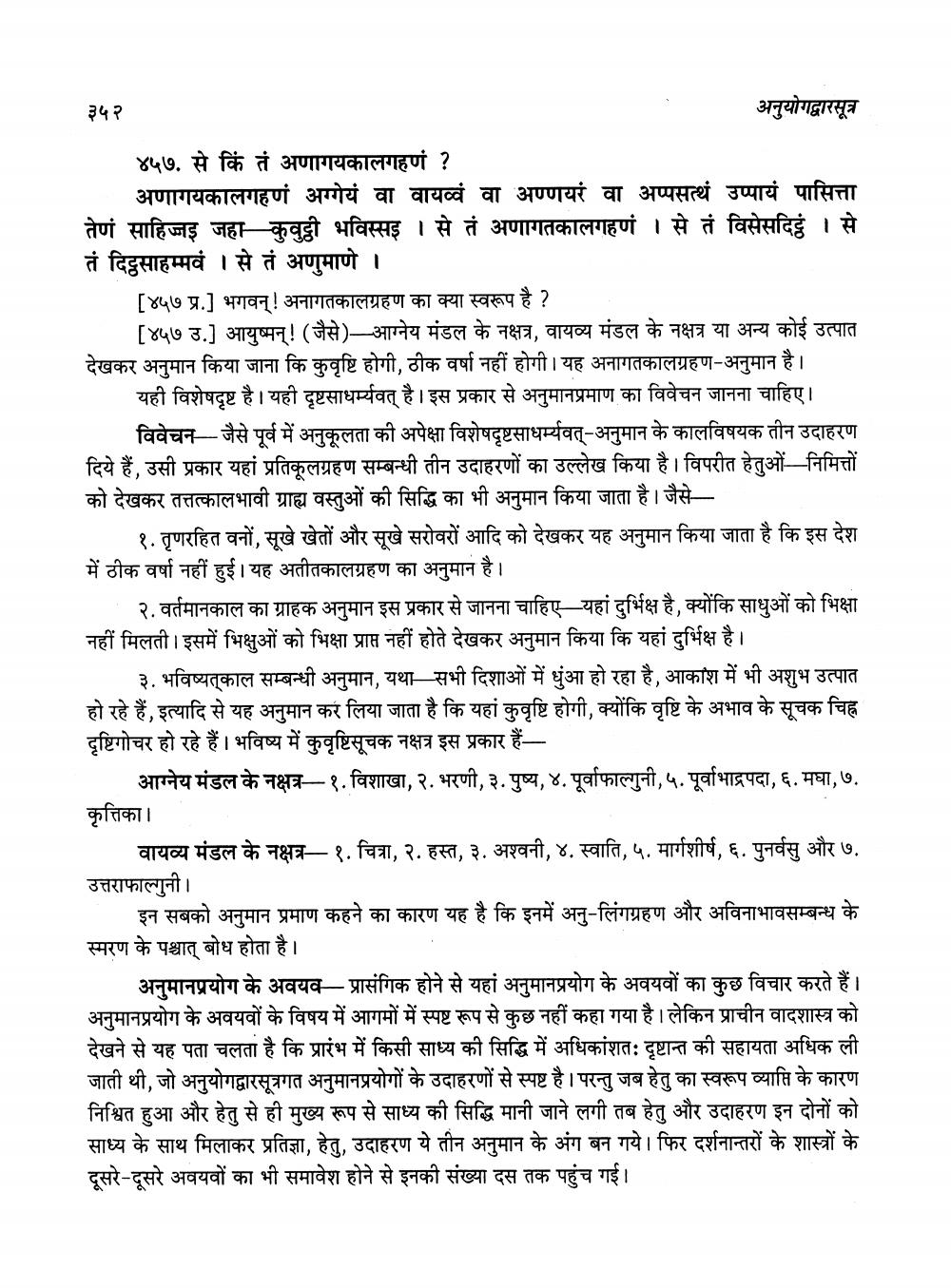________________
३५२
अनुयोगद्वारसूत्र
४५७. से किं तं अणागयकालगहणं ?
अणागयकालगहणं अग्गेयं वा वायव्वं वा अण्णयरं वा अप्पसत्थं उप्पायं पासित्ता साहिज्जइ जहा— कुवुट्ठी भविस्सइ । से तं अणागतकालगहणं । से तं विसेसदिट्टं । से तं दिट्ठसाहम्मवं । सेतं अणुमा ।
[४५७ प्र.] भगवन्! अनागतकालग्रहण का क्या स्वरूप है ?
[४५७ उ.] आयुष्मन्! (जैसे ) – आग्नेय मंडल के नक्षत्र, वायव्य मंडल के नक्षत्र या अन्य कोई उत्पात देखकर अनुमान किया जाना कि कुवृष्टि होगी, ठीक वर्षा नहीं होगी। यह अनागतकालग्रहण - अनुमान है।
यही विशेषदृष्ट है। यही दृष्टसाधर्म्यवत् है । इस प्रकार से अनुमानप्रमाण का विवेचन जानना चाहिए।
विवेचन — जैसे पूर्व में अनुकूलता की अपेक्षा विशेषदृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान के कालविषयक तीन उदाहरण दिये हैं, उसी प्रकार यहां प्रतिकूलग्रहण सम्बन्धी तीन उदाहरणों का उल्लेख किया है । विपरीत हेतुओं — निमित्तों को देखकर तत्तत्कालभावी ग्राह्य वस्तुओं की सिद्धि का भी अनुमान किया जाता है। जैसे—
१. तृणरहित वनों, सूखे खेतों और सूखे सरोवरों आदि को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि इस देश में ठीक वर्षा नहीं हुई। यह अतीतकालग्रहण का अनुमान है।
२. वर्तमानकाल का ग्राहक अनुमान इस प्रकार से जानना चाहिए—यहां दुर्भिक्ष है, क्योंकि साधुओं को भिक्षा नहीं मिलती। इसमें भिक्षुओं को भिक्षा प्राप्त नहीं होते देखकर अनुमान किया कि यहां दुर्भिक्ष है।
३. भविष्यत्काल सम्बन्धी अनुमान, यथा— सभी दिशाओं में धुंआ हो रहा है, आकाश में भी अशुभ उत्पात हो रहे हैं, इत्यादि से यह अनुमान कर लिया जाता है कि यहां कुवृष्टि होगी, क्योंकि वृष्टि के अभाव के सूचक चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भविष्य में कुवृष्टिसूचक नक्षत्र इस प्रकार हैं
आग्नेय मंडल के नक्षत्र - १. विशाखा, २. भरणी, ३. पुष्य, ४. पूर्वाफाल्गुनी, ५. पूर्वाभाद्रपदा, ६. मघा, ७.
कृत्तिका ।
वायव्य मंडल के नक्षत्र - १. चित्रा, २. हस्त, ३. अश्वनी, ४. स्वाति, ५. मार्गशीर्ष, ६. पुनर्वसु और ७. उत्तराफाल्गुनी ।
इन सबको अनुमान प्रमाण कहने का कारण यह है कि इनमें अनु-लिंगग्रहण और अविनाभावसम्बन्ध के स्मरण के पश्चात् बोध होता है।
अनुमानप्रयोग के अवयव — प्रासंगिक होने से यहां अनुमानप्रयोग के अवयवों का कुछ विचार करते हैं । अनुमानप्रयोग के अवयवों के विषय में आगमों में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन प्राचीन वादशास्त्र को देखने से यह पता चलता है कि प्रारंभ में किसी साध्य की सिद्धि में अधिकांशतः दृष्टान्त की सहायता अधिक ली जाती थी, जो अनुयोगद्वारसूत्रगत अनुमानप्रयोगों के उदाहरणों से स्पष्ट है । परन्तु जब हेतु का स्वरूप व्याप्ति के कारण निश्चित हुआ और हेतु से ही मुख्य रूप से साध्य की सिद्धि मानी जाने लगी तब हेतु और उदाहरण इन दोनों को साध्य के साथ मिलाकर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण ये तीन अनुमान के अंग बन गये। फिर दर्शनान्तरों के शास्त्रों के दूसरे - दूसरे अवयवों का भी समावेश होने से इनकी संख्या दस तक पहुंच गई।