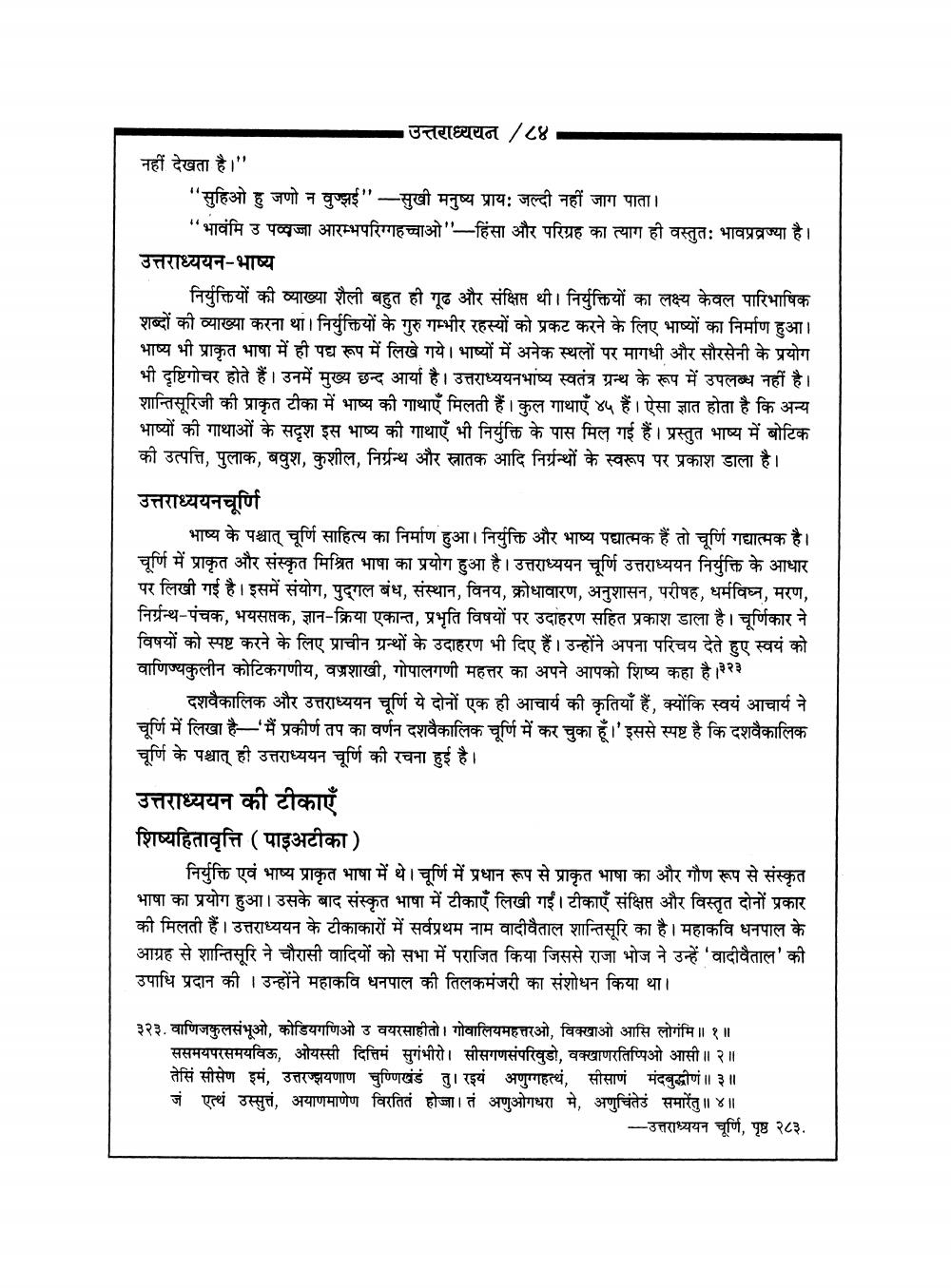________________
उत्तराध्ययन /८४नहीं देखता है।"
"सुहिओ हु जणो न वुज्झई"-सुखी मनुष्य प्रायः जल्दी नहीं जाग पाता।
"भावंमि उ पव्वज्जा आरम्भपरिग्गहच्चाओ"-हिंसा और परिग्रह का त्याग ही वस्तुतः भावप्रव्रज्या है। उत्तराध्ययन-भाष्य
नियुक्तियों की व्याख्या शैली बहुत ही गूढ और संक्षिप्त थी। नियुक्तियों का लक्ष्य केवल पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना था। नियुक्तियों के गुरु गम्भीर रहस्यों को प्रकट करने के लिए भाष्यों का निर्माण हुआ। भाष्य भी प्राकृत भाषा में ही पद्य रूप में लिखे गये। भाष्यों में अनेक स्थलों पर मागधी और सौरसेनी के प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें मुख्य छन्द आर्या है। उत्तराध्ययनभाष्य स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध नहीं है। शान्तिसूरिजी की प्राकृत टीका में भाष्य की गाथाएँ मिलती हैं। कुल गाथाएँ ४५ हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य भाष्यों की गाथाओं के सदृश इस भाष्य की गाथाएँ भी नियुक्ति के पास मिल गई हैं। प्रस्तुत भाष्य में बोटिक की उत्पत्ति, पुलाक, बवुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक आदि निर्ग्रन्थों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है।
उत्तराध्ययनचूर्णि
भाष्य के पश्चात् चूर्णि साहित्य का निर्माण हुआ। नियुक्ति और भाष्य पद्यात्मक हैं तो चूर्णि गद्यात्मक है। चूर्णि में प्राकृत और संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्तराध्ययन चूर्णि उत्तराध्ययन नियुक्ति के आधार पर लिखी गई है। इसमें संयोग, पुद्गल बंध, संस्थान, विनय, क्रोधावारण, अनुशासन, परीषह, धर्मविघ्न, मरण, निर्ग्रन्थ-पंचक, भयसप्तक, ज्ञान-क्रिया एकान्त, प्रभृति विषयों पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला है। चूर्णिकार ने विषयों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन ग्रन्थों के उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने अपना परिचय देते हुए स्वयं को वाणिज्यकुलीन कोटिकगणीय, वज्रशाखी, गोपालगणी महत्तर का अपने आपको शिष्य कहा है।३२३ ।
दशवैकालिक और उत्तराध्ययन चूर्णि ये दोनों एक ही आचार्य की कृतियाँ हैं, क्योंकि स्वयं आचार्य ने चूर्णि में लिखा है-'मैं प्रकीर्ण तप का वर्णन दशवकालिक चूर्णि में कर चुका हूँ।' इससे स्पष्ट है कि दशवैकालिक चूर्णि के पश्चात् ही उत्तराध्ययन चूर्णि की रचना हुई है। उत्तराध्ययन की टीकाएँ शिष्यहितावृत्ति (पाइअटीका)
नियुक्ति एवं भाष्य प्राकृत भाषा में थे। चूर्णि में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का और गौण रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। उसके बाद संस्कृत भाषा में टीकाएँ लिखी गईं। टीकाएँ संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार की मिलती हैं। उत्तराध्ययन के टीकाकारों में सर्वप्रथम नाम वादीवैताल शान्तिसूरि का है। महाकवि धनपाल के आग्रह से शान्तिसूरि ने चौरासी वादियों को सभा में पराजित किया जिससे राजा भोज ने उन्हें 'वादीवैताल' की उपाधि प्रदान की । उन्होंने महाकवि धनपाल की तिलकमंजरी का संशोधन किया था।
३२३. वाणिजकुलसंभूओ, कोडियगणिओ उ वयरसाहीतो। गोवालियमहत्तरओ, विक्खाओ आसि लोगंमि॥ १॥
ससमयपरसमयविऊ, ओयस्सी दित्तिमं सुगंभीरो। सीसगणसंपरिवुडो, वक्खाणरतिप्पिओ आसी॥ २॥ तेसिं सीसेण इम, उत्तरज्झयणाण चुण्णिखंडं तु। रइयं अणुग्गहत्थं, सीसाणं मंदबुद्धीणं ॥३॥ जं एत्थं उस्सुत्तं, अयाणमाणेण विरतितं होजा। तं अणुओगधरा मे, अणुचिंतेउं समारेंतु ॥ ४॥
-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ २८३.