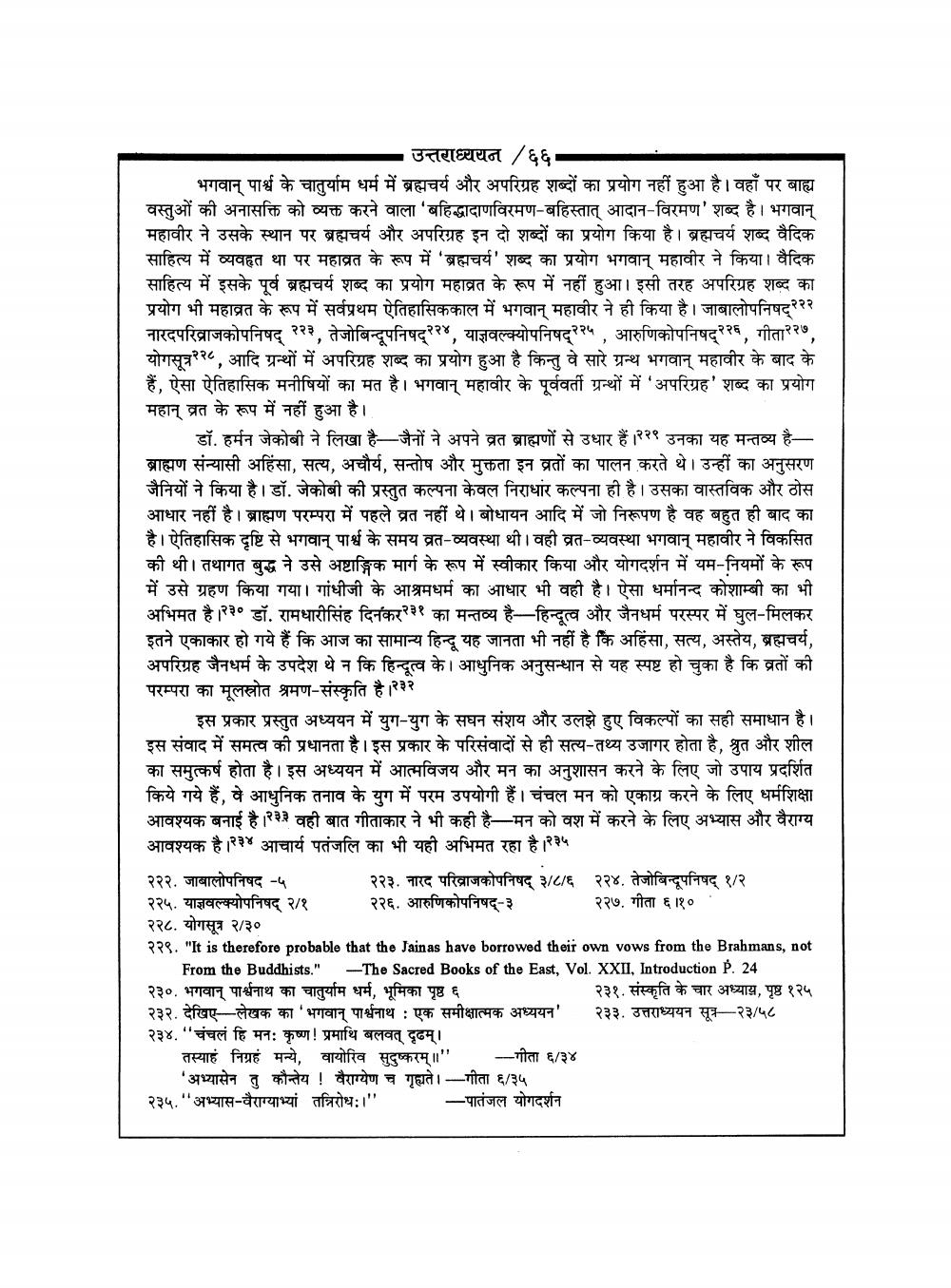________________
- उत्तराध्ययन /६६भगवान् पार्श्व के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ पर बाह्य वस्तुओं की अनासक्ति को व्यक्त करने वाला 'बहिद्धादाणविरमण-बहिस्तात् आदान-विरमण' शब्द है। भगवान् महावीर ने उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य शब्द वैदिक साहित्य में व्यवहृत था पर महाव्रत के रूप में 'ब्रह्मचर्य' शब्द का प्रयोग भगवान् महावीर ने किया। वैदिक साहित्य में इसके पूर्व ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग महाव्रत के रूप में नहीं हुआ। इसी तरह अपरिग्रह शब्द का प्रयोग भी महाव्रत के रूप में सर्वप्रथम ऐतिहासिककाल में भगवान् महावीर ने ही किया है। जाबालोपनिषद्२२२ नारदपरिव्राजकोपनिषद् २२३, तेजोबिन्दूपनिषद्२२४, याज्ञवल्क्योपनिषद्२२५ , आरुणिकोपनिषद्२२६, गीता२२७, योगसूत्र२२८, आदि ग्रन्थों में अपरिग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु वे सारे ग्रन्थ भगवान् महावीर के बाद के हैं, ऐसा ऐतिहासिक मनीषियों का मत है। भगवान् महावीर के पूर्ववर्ती ग्रन्थों में 'अपरिग्रह' शब्द का प्रयोग महान् व्रत के रूप में नहीं हुआ है।
डॉ. हर्मन जेकोबी ने लिखा है-जैनों ने अपने व्रत ब्राह्मणों से उधार हैं ।२२९ उनका यह मन्तव्य हैब्राह्मण संन्यासी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, सन्तोष और मुक्तता इन व्रतों का पालन करते थे। उन्हीं का अनुसरण जैनियों ने किया है। डॉ. जेकोबी की प्रस्तुत कल्पना केवल निराधार कल्पना ही है। उसका वास्तविक और ठोस आधार नहीं है। ब्राह्मण परम्परा में पहले व्रत नहीं थे। बोधायन आदि में जो निरूपण है वह बहुत ही बाद का है। ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान् पार्श्व के समय व्रत-व्यवस्था थी। वही व्रत-व्यवस्था भगवान् महावीर ने विकसित की थी। तथागत बुद्ध ने उसे अष्टाङ्गिक मार्ग के रूप में स्वीकार किया और योगदर्शन में यम-नियमों के रूप में उसे ग्रहण किया गया। गांधीजी के आश्रमधर्म का आधार भी वही है। ऐसा धर्मानन्द कोशाम्बी का भी अभिमत है।२३० डॉ. रामधारीसिंह दिनकर२३१ का मन्तव्य है-हिन्दूत्व और जैनधर्म परस्पर में घुल-मिलकर इतने एकाकार हो गये हैं कि आज का सामान्य हिन्दू यह जानता भी नहीं है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैनधर्म के उपदेश थे न कि हिन्दूत्व के। आधुनिक अनुसन्धान से यह स्पष्ट हो चुका है कि व्रतों की परम्परा का मूलस्रोत श्रमण-संस्कृति है।२३२
इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में युग-युग के सघन संशय और उलझे हुए विकल्पों का सही समाधान है। इस संवाद में समत्व की प्रधानता है। इस प्रकार के परिसंवादों से ही सत्य-तथ्य उजागर होता है, श्रुत और शील का समुत्कर्ष होता है। इस अध्ययन में आत्मविजय और मन का अनुशासन करने के लिए जो उपाय प्रदर्शित किये गये हैं, वे आधुनिक तनाव के युग में परम उपयोगी हैं। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए धर्मशिक्षा आवश्यक बनाई है ।२३३ वही बात गीताकार ने भी कही है-मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है।२३४ आचार्य पतंजलि का भी यही अभिमत रहा है।२३५ २२२. जाबालोपनिषद -५ २२३. नारद परिव्राजकोपनिषद् ३/८/६ २२४. तेजोबिन्दूपनिषद् १/२ २२५. याज्ञवल्क्योपनिषद् २/१ २२६. आरुणिकोपनिषद्-३
२२७. गीता ६१० २२८. योगसूत्र २/३० २२९. "It is therefore probable that the Jainas have borrowed their own vows from the Brahmans, not
From the Buddhists." -The Sacred Books of the East, Vol. XXII, Introduction P. 24 २३०. भगवान् पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म, भूमिका पृष्ठ ६
२३१. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ १२५ २३२. देखिए-लेखक का 'भगवान् पार्श्वनाथ : एक समीक्षात्मक अध्ययन' २३३. उत्तराध्ययन सूत्र-२३/५८ २३४. "चंचलं हि मनः कृष्ण! प्रमाथि बलवत् दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्॥" -गीता ६/३४
'अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते। -गीता ६/३५ २३५. "अभ्यास-वैराग्याभ्यां तनिरोधः।" -पातंजल योगदर्शन