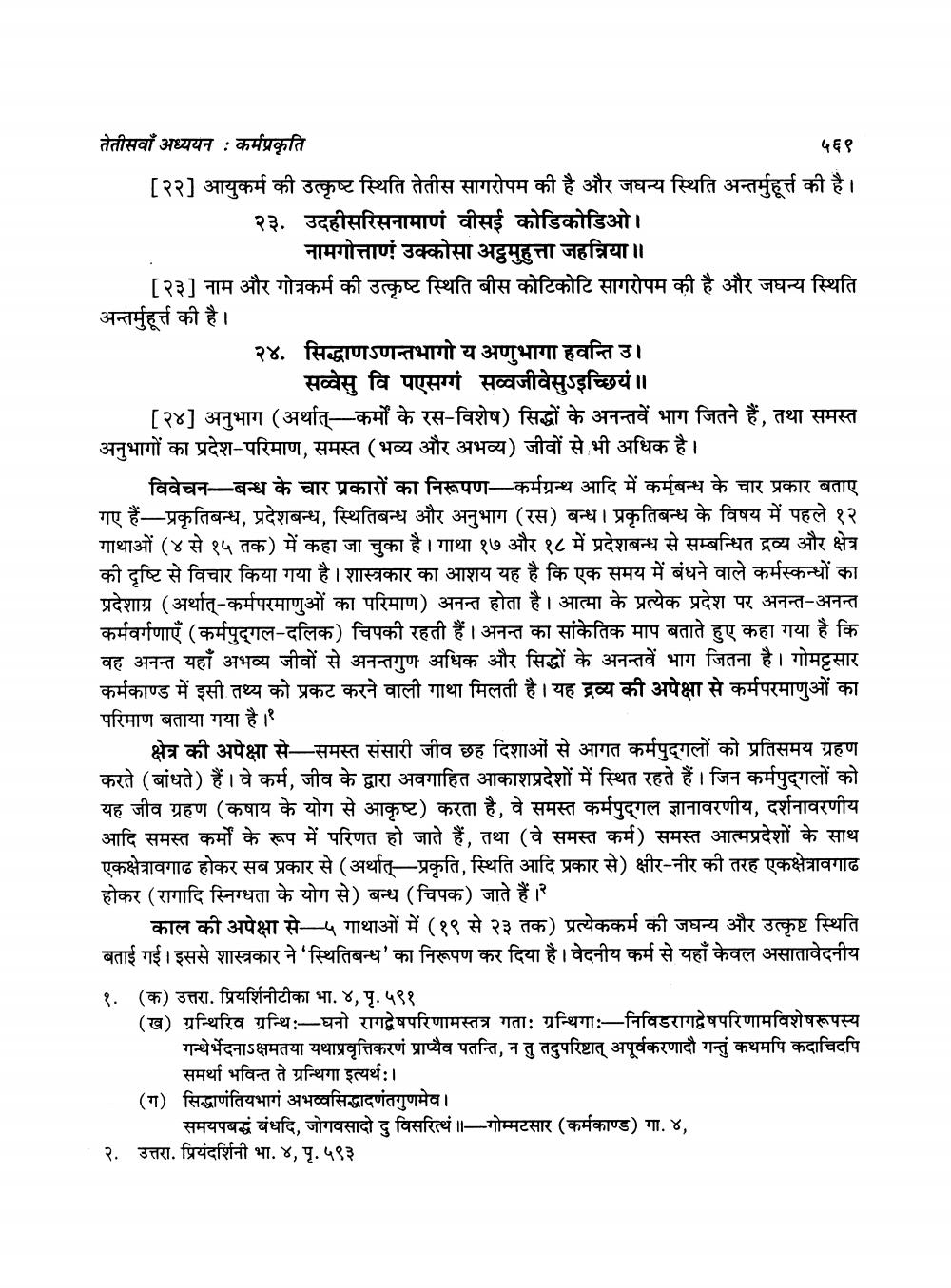________________
तेतीसवाँ अध्ययन : कर्मप्रकृति
५६९ [२२] आयुकर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है।
२३. उदहीसरिसनामाणं वीसई कोडिकोडिओ।
नामगोत्ताणं उक्कोसा अट्ठमुहुत्ता जहन्निया॥ [२३] नाम और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटिकोटि सागरोपम की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है।
२४. सिद्धाणऽणन्तभागो य अणुभागा हवन्ति ।
सव्वेसु वि पएसग्गं सव्वजीवेसुऽइच्छियं॥ [२४] अनुभाग (अर्थात् कर्मों के रस-विशेष) सिद्धों के अनन्तवें भाग जितने हैं, तथा समस्त अनुभागों का प्रदेश-परिमाण, समस्त (भव्य और अभव्य) जीवों से भी अधिक है।
विवेचन-बन्ध के चार प्रकारों का निरूपण-कर्मग्रन्थ आदि में कर्मबन्ध के चार प्रकार बताए गए हैं—प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभाग (रस) बन्ध। प्रकृतिबन्ध के विषय में पहले १२ गाथाओं (४ से १५ तक) में कहा जा चुका है। गाथा १७ और १८ में प्रदेशबन्ध से सम्बन्धित द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया गया है। शास्त्रकार का आशय यह है कि एक समय में बंधने वाले कर्मस्कन्धों का प्रदेशाग्र (अर्थात्-कर्मपरमाणुओं का परिमाण) अनन्त होता है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्मवर्गणाएँ (कर्मपुद्गल-दलिक) चिपकी रहती हैं। अनन्त का सांकेतिक माप बताते हुए कहा गया है कि वह अनन्त यहाँ अभव्य जीवों से अनन्तगुण अधिक और सिद्धों के अनन्तवें भाग जितना है। गोमट्टसार कर्मकाण्ड में इसी तथ्य को प्रकट करने वाली गाथा मिलती है। यह द्रव्य की अपेक्षा से कर्मपरमाणुओं का परिमाण बताया गया है।
क्षेत्र की अपेक्षा से समस्त संसारी जीव छह दिशाओं से आगत कर्मपुद्गलों को प्रतिसमय ग्रहण करते (बांधते) हैं। वे कर्म, जीव के द्वारा अवगाहित आकाशप्रदेशों में स्थित रहते हैं। जिन कर्मपुद्गलों को यह जीव ग्रहण (कषाय के योग से आकृष्ट) करता है, वे समस्त कर्मपुद्गल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि समस्त कर्मों के रूप में परिणत हो जाते हैं, तथा (वे समस्त कर्म) समस्त आत्मप्रदेशों के साथ एकक्षेत्रावगाढ होकर सब प्रकार से (अर्थात्-प्रकृति, स्थिति आदि प्रकार से) क्षीर-नीर की तरह एकक्षेत्रावगाढ होकर (रागादि स्निग्धता के योग से) बन्ध (चिपक) जाते हैं।
___ काल की अपेक्षा से—५ गाथाओं में (१९ से २३ तक) प्रत्येककर्म की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बताई गई। इससे शास्त्रकार ने 'स्थितिबन्ध' का निरूपण कर दिया है। वेदनीय कर्म से यहाँ केवल असातावेदनीय १. (क) उत्तरा. प्रियर्शिनीटीका भा. ४, पृ. ५९१ (ख) ग्रन्थिरिव ग्रन्थिः-घनो रागद्वेषपरिणामस्तत्र गताः ग्रन्थिगा:-निविडरागद्वेषपरिणामविशेषरूपस्य
गन्थेर्भेदनाऽक्षमतया यथाप्रवृत्तिकरणं प्राप्यैव पतन्ति, न तु तदुपरिष्टात् अपूर्वकरणादौ गन्तुं कथमपि कदाचिदपि
समर्था भविन्त ते ग्रन्थिगा इत्यर्थः। (ग) सिद्धाणंतियभागं अभव्वसिद्धादणंतगणमेव।
समयपबद्धं बंधदि, जोगवसादो दु विसरित्थं ॥-गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) गा. ४, २. उत्तरा. प्रियंदर्शिनी भा. ४, पृ.५९३