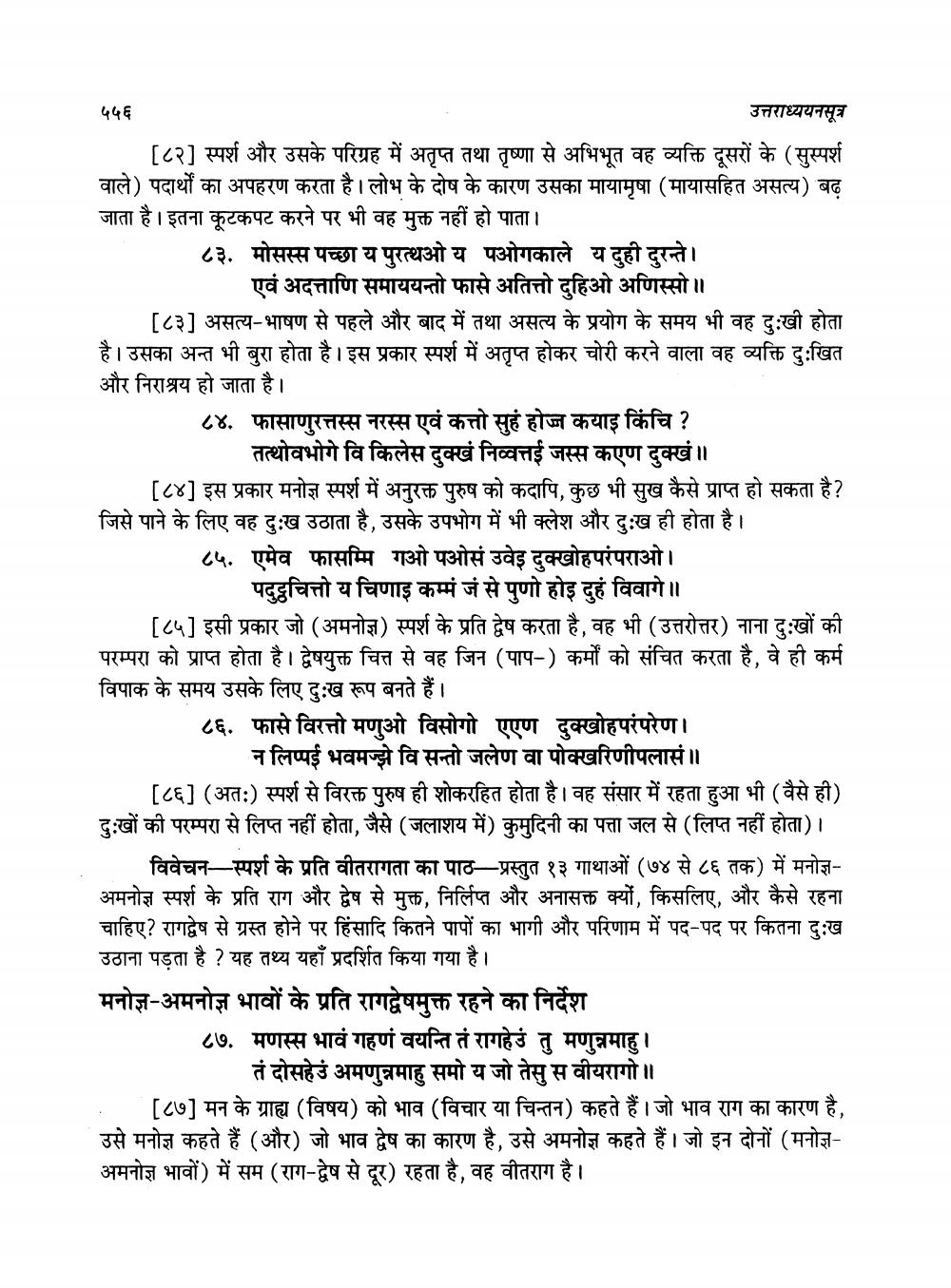________________
५५६
उत्तराध्ययनसूत्र [८२] स्पर्श और उसके परिग्रह में अतृप्त तथा तृष्णा से अभिभूत वह व्यक्ति दूसरों के (सुस्पर्श वाले) पदार्थों का अपहरण करता है। लोभ के दोष के कारण उसका मायामृषा (मायासहित असत्य) बढ़ जाता है। इतना कूटकपट करने पर भी वह मुक्त नहीं हो पाता।
८३. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य पओगकाले य दुही दुरन्ते।
__एवं अदत्ताणि समाययन्तो फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो॥ [८३] असत्य-भाषण से पहले और बाद में तथा असत्य के प्रयोग के समय भी वह दुःखी होता है। उसका अन्त भी बुरा होता है। इस प्रकार स्पर्श में अतृप्त होकर चोरी करने वाला वह व्यक्ति दुःखित और निराश्रय हो जाता है।
८४. फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि ?
तत्थोवभोगे वि किलेस दुक्खं निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं॥ [८४] इस प्रकार मनोज्ञ स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को कदापि, कुछ भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जिसे पाने के लिए वह दुःख उठाता है, उसके उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही होता है।
८५. एमेव फासम्मि गओ पओसं उवेइ दुक्खोहपरंपराओ।
पदुद्दचित्तो य चिणाइ कम्मं जं से पुणो होइ दुहं विवागे॥ [८५] इसी प्रकार जो (अमनोज्ञ) स्पर्श के प्रति द्वेष करता है, वह भी (उत्तरोत्तर) नाना दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेषयुक्त चित्त से वह जिन (पाप-) कर्मों को संचित करता है, वे ही कर्म विपाक के समय उसके लिए दु:ख रूप बनते हैं।
८६. फासे विरत्तो मणुओ विसोगो एएण दुक्खोहपरंपरेण।
न लिप्पई भवमझे वि सन्तो जलेण वा पोक्खरिणीपलासं॥ [८६] (अतः) स्पर्श से विरक्त पुरुष ही शोकरहित होता है। वह संसार में रहता हुआ भी (वैसे ही) दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता, जैसे (जलाशय में) कुमुदिनी का पत्ता जल से (लिप्त नहीं होता)।
विवेचन—स्पर्श के प्रति वीतरागता का पाठ—प्रस्तुत १३ गाथाओं (७४ से ८६ तक) में मनोज्ञअमनोज्ञ स्पर्श के प्रति राग और द्वेष से मुक्त, निर्लिप्त और अनासक्त क्यों, किसलिए, और कैसे रहना चाहिए? रागद्वेष से ग्रस्त होने पर हिंसादि कितने पापों का भागी और परिणाम में पद-पद पर कितना दुःख उठाना पड़ता है ? यह तथ्य यहाँ प्रदर्शित किया गया है। मनोज्ञ-अमनोज्ञ भावों के प्रति रागद्वेषमुक्त रहने का निर्देश
८७. मणस्स भावं गहणं वयन्ति तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु समो य जो तेसु स वीयरागो॥ .. [८७] मन के ग्राह्य (विषय) को भाव (विचार या चिन्तन) कहते हैं। जो भाव राग का कारण है, उसे मनोज्ञ कहते हैं (और) जो भाव द्वेष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते हैं। जो इन दोनों (मनोज्ञअमनोज्ञ भावों) में सम (राग-द्वेष से दूर) रहता है, वह वीतराग है।