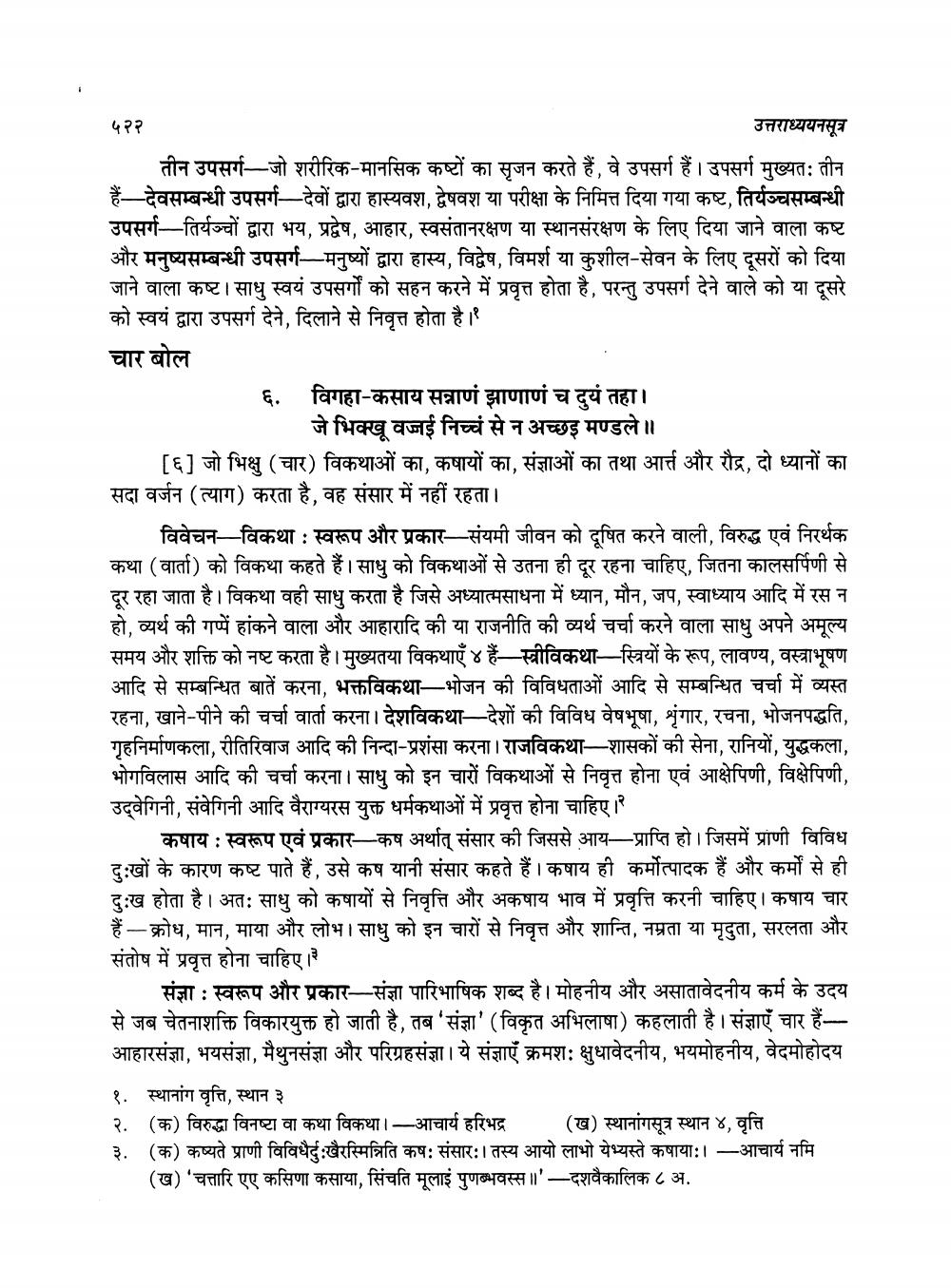________________
५२२
उत्तराध्ययनसूत्र तीन उपसर्ग-जो शरीरिक-मानसिक कष्टों का सृजन करते हैं, वे उपसर्ग हैं । उपसर्ग मुख्यतः तीन हैं—देवसम्बन्धी उपसर्ग—देवों द्वारा हास्यवश, द्वेषवश या परीक्षा के निमित्त दिया गया कष्ट, तिर्यञ्चसम्बन्धी उपसर्ग-तिर्यञ्चों द्वारा भय, प्रद्वेष, आहार, स्वसंतानरक्षण या स्थानसंरक्षण के लिए दिया जाने वाला कष्ट
और मनुष्यसम्बन्धी उपसर्ग-मनुष्यों द्वारा हास्य, विद्वेष, विमर्श या कुशील-सेवन के लिए दूसरों को दिया जाने वाला कष्ट । साधु स्वयं उपसर्गों को सहन करने में प्रवृत्त होता है, परन्तु उपसर्ग देने वाले को या दूसरे को स्वयं द्वारा उपसर्ग देने, दिलाने से निवृत्त होता है। चार बोल
६. विगहा-कसाय सन्नाणं झाणाणं च दुयं तहा।
__ जे भिक्खू वजई निच्चं से न अच्छइ मण्डले॥ [६] जो भिक्षु (चार) विकथाओं का, कषायों का, संज्ञाओं का तथा आर्त और रौद्र, दो ध्यानों का सदा वर्जन (त्याग) करता है, वह संसार में नहीं रहता।
विवेचन-विकथा : स्वरूप और प्रकार–संयमी जीवन को दूषित करने वाली, विरुद्ध एवं निरर्थक कथा (वार्ता) को विकथा कहते हैं। साधु को विकथाओं से उतना ही दूर रहना चाहिए, जितना कालसर्पिणी से दूर रहा जाता है। विकथा वही साधु करता है जिसे अध्यात्मसाधना में ध्यान, मौन, जप, स्वाध्याय आदि में रस न हो, व्यर्थ की गप्पें हांकने वाला और आहारादि की या राजनीति की व्यर्थ चर्चा करने वाला साधु अपने अमूल्य समय और शक्ति को नष्ट करता है। मुख्यतया विकथाएँ ४ हैं—स्त्रीविकथा—स्त्रियों के रूप, लावण्य, वस्त्राभूषण
आदि से सम्बन्धित बातें करना, भक्तविकथा—भोजन की विविधताओं आदि से सम्बन्धित चर्चा में व्यस्त रहना, खाने-पीने की चर्चा वार्ता करना। देशविकथा—देशों की विविध वेषभूषा, शृंगार, रचना, भोजनपद्धति, गृहनिर्माणकला, रीतिरिवाज आदि की निन्दा-प्रशंसा करना। राजविकथा-शासकों की सेना, रानियों, युद्धकला, भोगविलास आदि की चर्चा करना। साधु को इन चारों विकथाओं से निवृत्त होना एवं आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, उद्वेगिनी, संवेगिनी आदि वैराग्यरस युक्त धर्मकथाओं में प्रवृत्त होना चाहिए।
कषाय : स्वरूप एवं प्रकार—कष अर्थात् संसार की जिससे आय—प्राप्ति हो। जिसमें प्राणी विविध दु:खों के कारण कष्ट पाते हैं, उसे कष यानी संसार कहते हैं। कषाय ही कर्मोत्पादक हैं और कर्मों से ही दुःख होता है। अतः साधु को कषायों से निवृत्ति और अकषाय भाव में प्रवृत्ति करनी चाहिए। कषाय चार हैं - क्रोध, मान, माया और लोभ । साधु को इन चारों से निवृत्त और शान्ति, नम्रता या मृदुता, सरलता और संतोष में प्रवृत्त होना चाहिए।
संज्ञा : स्वरूप और प्रकार—संज्ञा पारिभाषिक शब्द है। मोहनीय और असातावेदनीय कर्म के उदय से जब चेतनाशक्ति विकारयुक्त हो जाती है, तब 'संज्ञा' (विकृत अभिलाषा) कहलाती है। संज्ञाएँ चार हैंआहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा। ये संज्ञाएँ क्रमशः क्षुधावेदनीय, भयमोहनीय, वेदमोहोदय १. स्थानांग वृत्ति, स्थान ३ २. (क) विरुद्धा विनष्टा वा कथा विकथा। -आचार्य हरिभद्र (ख) स्थानांगसूत्र स्थान ४, वृत्ति ३. (क) कष्यते प्राणी विविधैर्दुःखैरस्मिन्निति कष: संसारः। तस्य आयो लाभो येभ्यस्ते कषायाः। -आचार्य नमि
(ख) 'चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचति मूलाई पुणब्भवस्स॥'–दशवैकालिक ८ अ.