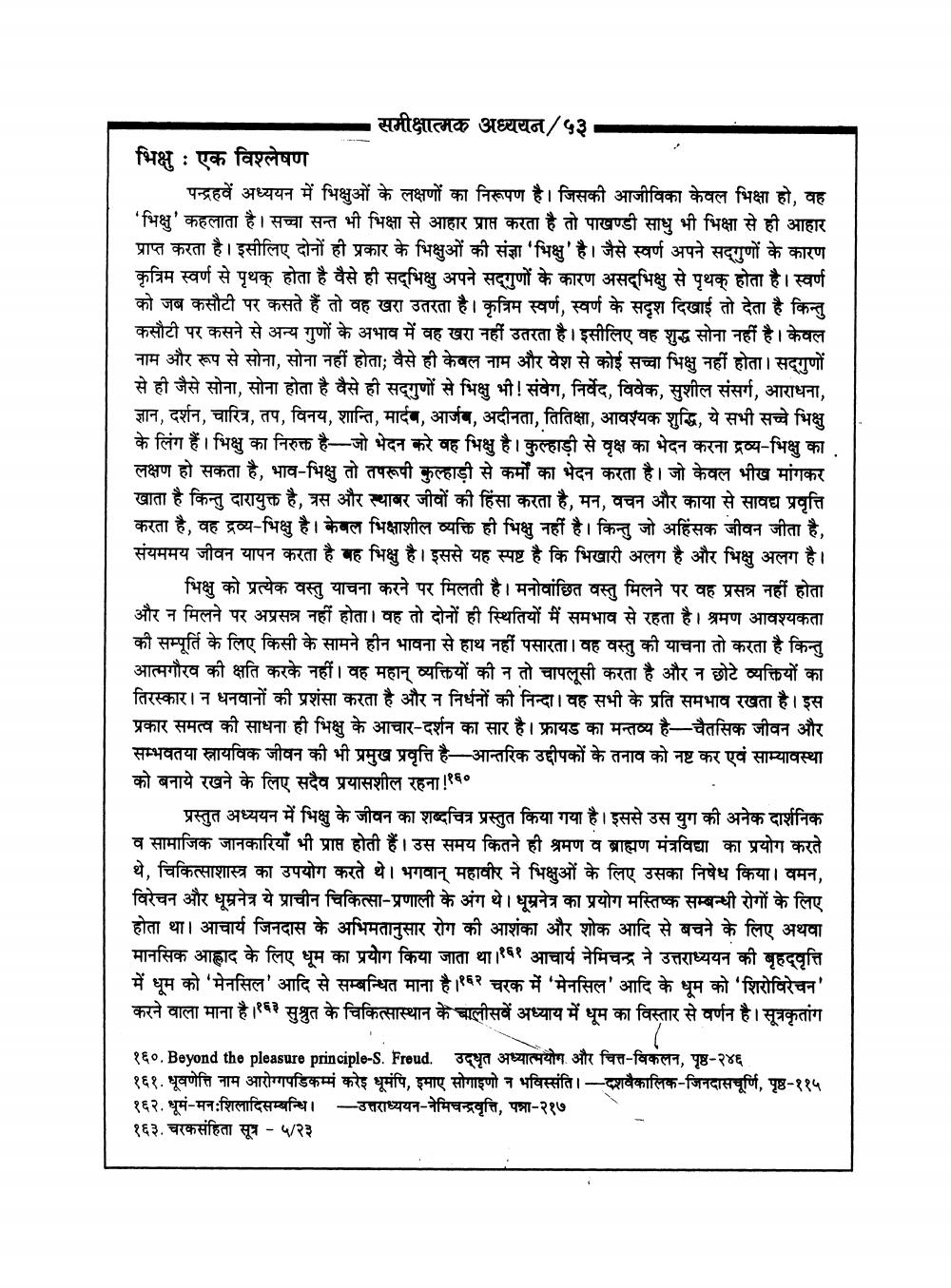________________
- समीक्षात्मक अध्ययन/५३ भिक्षु : एक विश्लेषण
पन्द्रहवें अध्ययन में भिक्षुओं के लक्षणों का निरूपण है। जिसकी आजीविका केवल भिक्षा हो, वह 'भिक्षु' कहलाता है। सच्चा सन्त भी भिक्षा से आहार प्राप्त करता है तो पाखण्डी साधु भी भिक्षा से ही आहार प्राप्त करता है। इसीलिए दोनों ही प्रकार के भिक्षुओं की संज्ञा 'भिक्ष' है। जैसे स्वर्ण अपने सदगणों के कारण कृत्रिम स्वर्ण से पृथक् होता है वैसे ही सद्भिक्षु अपने सद्गुणों के कारण असभिक्षु से पृथक् होता है। स्वर्ण को जब कसौटी पर कसते हैं तो वह खरा उतरता है। कृत्रिम स्वर्ण, स्वर्ण के सदृश दिखाई तो देता है किन्तु कसौटी पर कसने से अन्य गुणों के अभाव में वह खरा नहीं उतरता है। इसीलिए वह शुद्ध सोना नहीं है। केवल नाम और रूप से सोना, सोना नहीं होता; वैसे ही केवल नाम और वेश से कोई सच्चा भिक्षु नहीं होता। सद्गुणों से ही जैसे सोना, सोना होता है वैसे ही सद्गुणों से भिक्षु भी! संवेग, निर्वेद, विवेक, सुशील संसर्ग, आराधना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, शान्ति, मार्दव, आर्जब, अदीनता, तितिक्षा, आवश्यक शुद्धि, ये सभी सच्चे भिक्षु के लिंग हैं। भिक्षु का निरुक्त है-जो भेदन करे वह भिक्षु है। कुल्हाड़ी से वृक्ष का भेदन करना द्रव्य-भिक्षु का . लक्षण हो सकता है, भाव-भिक्षु तो तपरूपी कुल्हाड़ी से कर्मों का भेदन करता है। जो केवल भीख मांगकर खाता है किन्तु दारायुक्त है, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है, मन, वचन और काया से सावध प्रवृत्ति करता है, वह द्रव्य-भिक्षु है। केबल भिक्षाशील व्यक्ति ही भिक्षु नहीं है। किन्तु जो अहिंसक जीवन जीता है, संयममय जीवन यापन करता है वह भिक्षु है। इससे यह स्पष्ट है कि भिखारी अलग है और भिक्षु अलग है।
भिक्षु को प्रत्येक वस्तु याचना करने पर मिलती है। मनोवांछित वस्तु मिलने पर वह प्रसन्न नहीं होता और न मिलने पर अप्रसन्न नहीं होता। वह तो दोनों ही स्थितियों में समभाव से रहता है। श्रमण आवश्यकता की सम्पूर्ति के लिए किसी के सामने हीन भावना से हाथ नहीं पसारता। वह वस्तु की याचना तो करता है किन्तु आत्मगौरव की क्षति करके नहीं। वह महान् व्यक्तियों की न तो चापलूसी करता है और न छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार। न धनवानों की प्रशंसा करता है और न निर्धनों की निन्दा। वह सभी के प्रति समभाव रखता है। इस प्रकार समत्व की साधना ही भिक्षु के आचार-दर्शन का सार है। फ्रायड का मन्तव्य है-चैतसिक जीवन और सम्भवतया स्नायविक जीवन की भी प्रमुख प्रवृत्ति है—आन्तरिक उद्दीपकों के तनाव को नष्ट कर एवं साम्यावस्था को बनाये रखने के लिए सदैव प्रयासशील रहना!१६०
प्रस्तुत अध्ययन में भिक्षु के जीवन का शब्दचित्र प्रस्तुत किया गया है। इससे उस युग की अनेक दार्शनिक व सामाजिक जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। उस समय कितने ही श्रमण व ब्राह्मण मंत्रविद्या का प्रयोग करते थे, चिकित्साशास्त्र का उपयोग करते थे। भगवान् महावीर ने भिक्षुओं के लिए उसका निषेध किया। वमन, विरेचन और धूम्रनेत्र ये प्राचीन चिकित्सा-प्रणाली के अंग थे। धूम्रनेत्र का प्रयोग मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों के लिए होता था। आचार्य जिनदास के अभिमतानुसार रोग की आशंका और शोक आदि से बचने के लिए अथवा मानसिक आह्लाद के लिए धूम का प्रयोग किया जाता था।१६१ आचार्य नेमिचन्द्र ने उत्तराध्ययन की बृहवृत्ति में धूम को 'मेनसिल' आदि से सम्बन्धित माना है।१६२ चरक में 'मेनसिल' आदि के धूम को "शिरोविरेचन' करने वाला माना है।१६३ सुश्रुत के चिकित्सास्थान के चालीसवें अध्याय में धूम का विस्तार से वर्णन है। सूत्रकृतांग
१६०. Beyond the pleasure principle-s. Freud. उद्धृत अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन, पृष्ठ-२४६ १६१. धूवणेत्ति नाम आरोग्गपडिकम्मं करेइ धूमंपि, इमाए सोगाइणो न भविस्संति। -दशवैकालिक-जिनदासचूर्णि, पृष्ठ-११५ १६२. धूम-मनःशिलादिसम्बन्धि। -उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्रवृत्ति, पन्ना-२१७ १६३. चरकसंहिता सूत्र - ५/२३