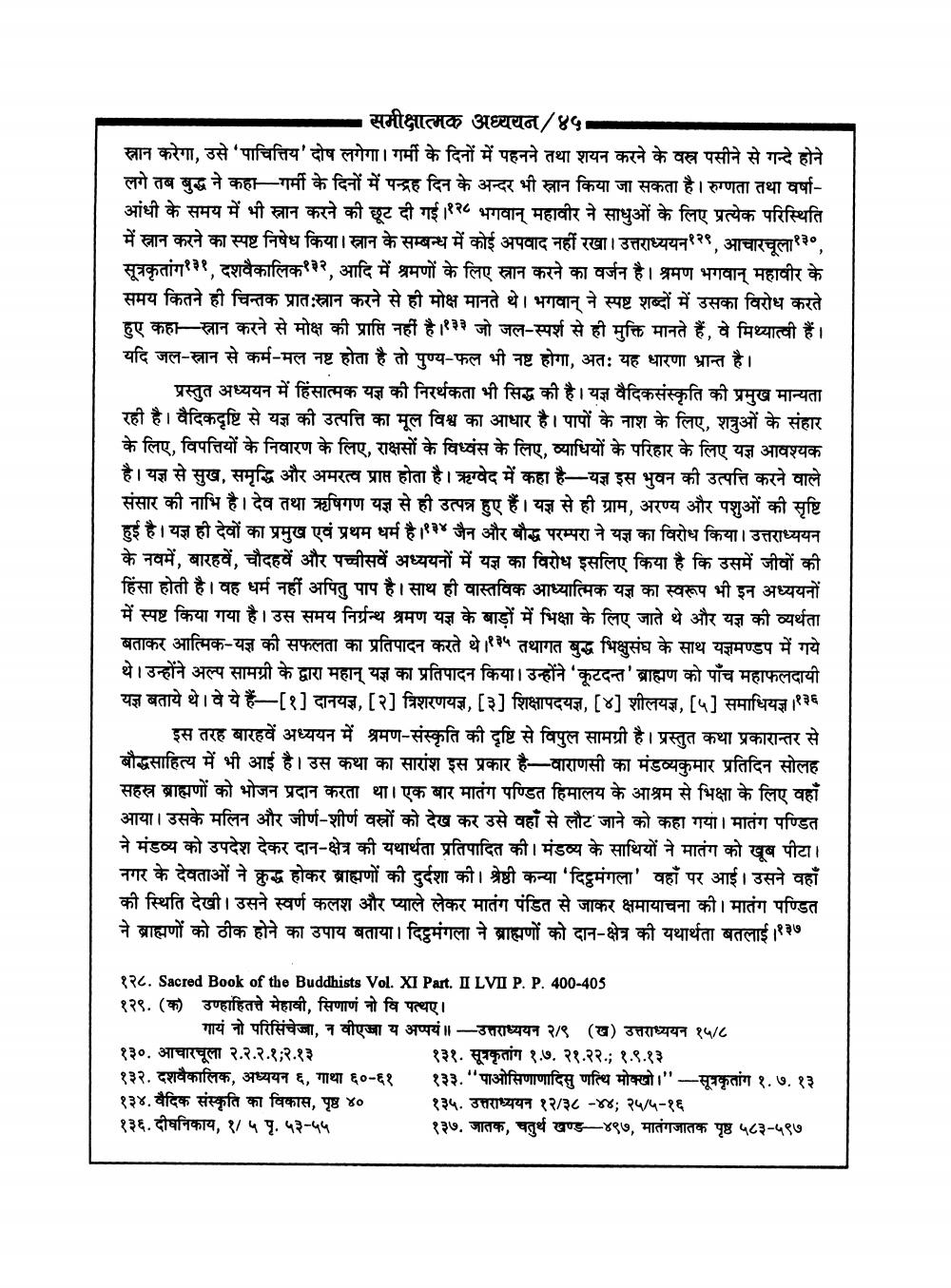________________
समीक्षात्मक अध्ययन/४५. स्नान करेगा, उसे 'पाचित्तिय' दोष लगेगा। गर्मी के दिनों में पहनने तथा शयन करने के वस्त्र पसीने से गन्दे होने लगे तब बुद्ध ने कहा-गर्मी के दिनों में पन्द्रह दिन के अन्दर भी स्नान किया जा सकता है। रुग्णता तथा वर्षाआंधी के समय में भी स्नान करने की छूट दी गई।१२८ भगवान् महावीर ने साधुओं के लिए प्रत्येक परिस्थिति में स्नान करने का स्पष्ट निषेध किया। स्नान के सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं रखा। उत्तराध्ययन१२९, आचारचूला१३०, सूत्रकृतांग१३१, दशवकालिक ३२, आदि में श्रमणों के लिए स्नान करने का वर्जन है। श्रमण भगवान् महावीर के समय कितने ही चिन्तक प्रात:स्नान करने से ही मोक्ष मानते थे। भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध करते हुए कहा-स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है।१३३ जो जल-स्पर्श से ही मुक्ति मानते हैं, वे मिथ्यात्वी हैं। यदि जल-स्नान से कर्म-मल नष्ट होता है तो पुण्य-फल भी नष्ट होगा, अतः यह धारणा भ्रान्त है।
प्रस्तुत अध्ययन में हिंसात्मक यज्ञ की निरर्थकता भी सिद्ध की है। यज्ञ वैदिकसंस्कृति की प्रमुख मान्यता रही है। वैदिकदृष्टि से यज्ञ की उत्पत्ति का मूल विश्व का आधार है। पापों के नाश के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए, विपत्तियों के निवारण के लिए, राक्षसों के विध्वंस के लिए, व्याधियों के परिहार के लिए यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ से सुख, समृद्धि और अमरत्व प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा है-यज्ञ इस भुवन की उत्पत्ति करने वाले संसार की नाभि है। देव तथा ऋषिगण यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं। यज्ञ से ही ग्राम, अरण्य और पशुओं की सृष्टि हुई है। यज्ञ ही देवों का प्रमुख एवं प्रथम धर्म है।९३४ जैन और बौद्ध परम्परा ने यज्ञ का विरोध किया। उत्तराध्ययन के नवमें, बारहवें, चौदहवें और पच्चीसवें अध्ययनों में यज्ञ का विरोध इसलिए किया है कि उसमें जीवों की हिंसा होती है। वह धर्म नहीं अपितु पाप है। साथ ही वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ का स्वरूप भी इन अध्ययनों में स्पष्ट किया गया है। उस समय निर्ग्रन्थ श्रमण यज्ञ के बाड़ों में भिक्षा के लिए जाते थे और यज्ञ की व्यर्थता बताकर आत्मिक-यज्ञ की सफलता का प्रतिपादन करते थे।३५ तथागत बुद्ध भिक्षुसंघ के साथ यज्ञमण्डप में गये थे। उन्होंने अल्प सामग्री के द्वारा महान् यज्ञ का प्रतिपादन किया। उन्होंने 'कूटदन्त' ब्राह्मण को पाँच महाफलदायी यज्ञ बताये थे। वे ये हैं-[१] दानयज्ञ, [२] त्रिशरणयज्ञ, [३] शिक्षापदयज्ञ, [४] शीलयज्ञ, [५] समाधियज्ञ।१३६
इस तरह बारहवें अध्ययन में श्रमण-संस्कृति की दृष्टि से विपुल सामग्री है। प्रस्तुत कथा प्रकारान्तर से बौद्धसाहित्य में भी आई है। उस कथा का सारांश इस प्रकार है-वाराणसी का मंडव्यकुमार प्रतिदिन सोलह सहस्र ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता था। एक बार मातंग पण्डित हिमालय के आश्रम से भिक्षा के लिए वहाँ आया। उसके मलिन और जीर्ण-शीर्ण वस्रों को देख कर उसे वहाँ से लौट जाने को कहा गया। मातंग पण्डित ने मंडव्य को उपदेश देकर दान-क्षेत्र की यथार्थता प्रतिपादित की। मंडव्य के साथियों ने मातंग को खूब पीटा। नगर के देवताओं ने क्रुद्ध होकर ब्राह्मणों की दुर्दशा की। श्रेष्ठी कन्या 'दिट्ठमंगला' वहाँ पर आई। उसने वहाँ की स्थिति देखी। उसने स्वर्ण कलश और प्याले लेकर मातंग पंडित से जाकर क्षमायाचना की। मातंग पण्डित ने ब्राह्मणों को ठीक होने का उपाय बताया। दिद्वमंगला ने ब्राह्मणों को दान-क्षेत्र की यथार्थता बतलाई।१३७
१२८. Sacred Book of the Buddhists Vol. XI Part. II LVII P.P.400-405 १२९. (क) उण्हाहितत्ते मेहावी, सिणाणं नो वि पत्थए।
गायं नो परिसिंचेज्जा, न वीएज्जा य अप्पयं। -उत्तराध्ययन २/९ (ख) उत्तराध्ययन १५/८ १३०. आचारचूला २.२.२.१२.१३
१३१. सूत्रकृतांग १.७. २१.२२.; १.९.१३ १३२. दशवैकालिक, अध्ययन ६, गाथा ६०-६१ १३३. "पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो।" -सूत्रकृतांग १.७. १३ १३४. वैदिक संस्कृति का विकास, पृष्ठ ४० १३५. उत्तराध्ययन १२/३८ -४४; २५/५-१६ १३६. दीघनिकाय, १/५ पृ. ५३-५५
१३७. जातक, चतुर्थ खण्ड-४९७, मातंगजातक पृष्ठ ५८३-५९७