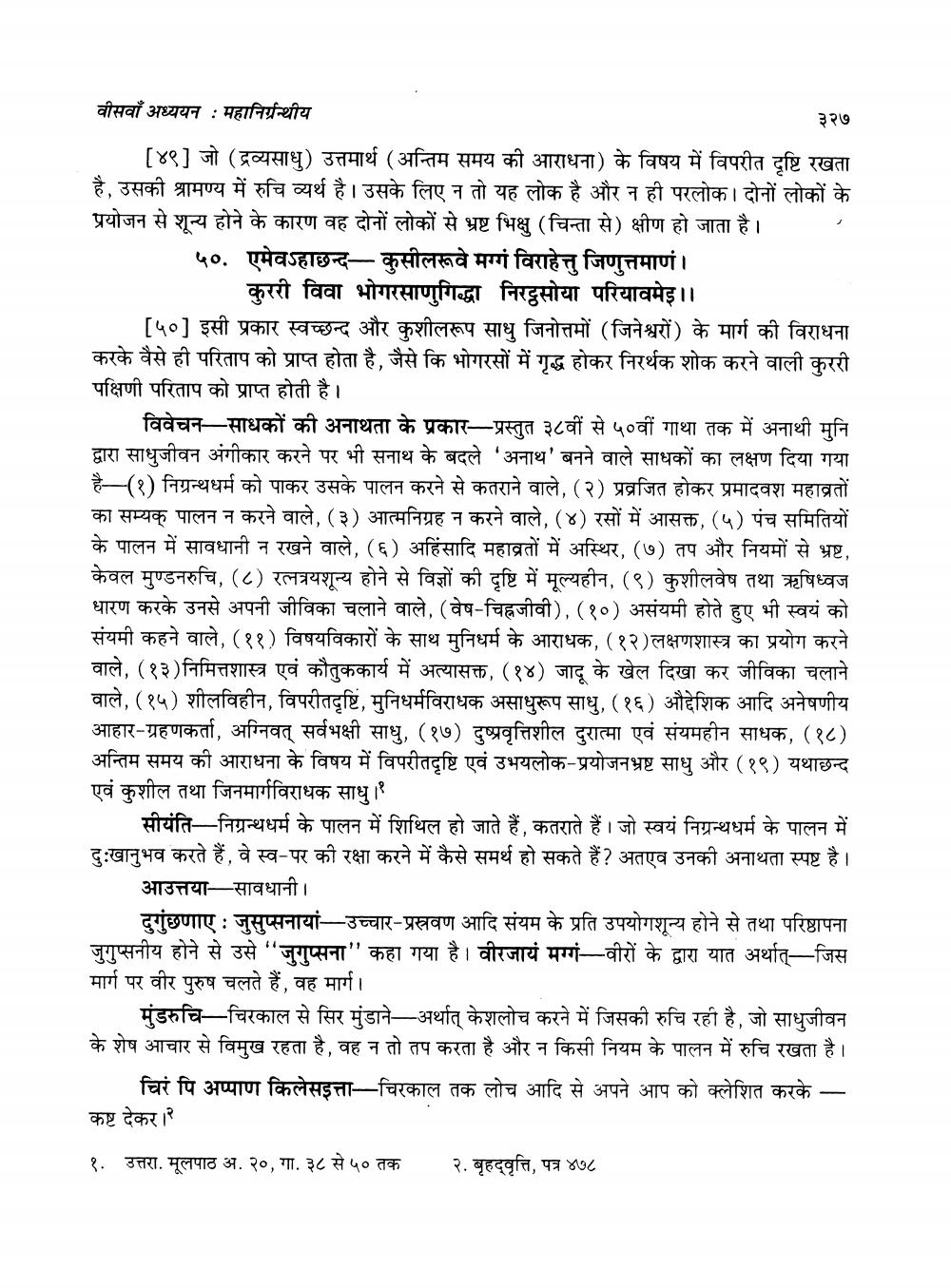________________
वीसवाँ अध्ययन : महानिर्ग्रन्थीय
३२७
[४९] जो (द्रव्यसाधु) उत्तमार्थ (अन्तिम समय की आराधना) के विषय में विपरीत दृष्टि रखता है, उसकी श्रामण्य में रुचि व्यर्थ है। उसके लिए न तो यह लोक है और न ही परलोक। दोनों लोकों के प्रयोजन से शून्य होने के कारण वह दोनों लोकों से भ्रष्ट भिक्षु (चिन्ता से) क्षीण हो जाता है।
५०. एमेवऽहाछन्द- कुसीलरूवे मग्गं विराहेत्तु जिणुत्तमाणं।
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा निरट्ठसोया परियावमेइ।। [५०] इसी प्रकार स्वच्छन्द और कुशीलरूप साधु जिनोत्तमों (जिनेश्वरों) के मार्ग की विराधना करके वैसे ही परिताप को प्राप्त होता है, जैसे कि भोगरसों में गृद्ध होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी पक्षिणी परिताप को प्राप्त होती है।
विवेचन—साधकों की अनाथता के प्रकार—प्रस्तुत ३८वीं से ५०वीं गाथा तक में अनाथी मुनि द्वारा साधुजीवन अंगीकार करने पर भी सनाथ के बदले 'अनाथ' बनने वाले साधकों का लक्षण दिया गया है—(१) निग्रन्थधर्म को पाकर उसके पालन करने से कतराने वाले, (२) प्रव्रजित होकर प्रमादवश महाव्रतों का सम्यक् पालन न करने वाले, (३) आत्मनिग्रह न करने वाले, (४) रसों में आसक्त, (५) पंच समितियों के पालन में सावधानी न रखने वाले, (६) अहिंसादि महाव्रतों में अस्थिर, (७) तप और नियमों से भ्रष्ट, केवल मुण्डनरुचि, (८) रत्नत्रयशून्य होने से विज्ञों की दृष्टि में मूल्यहीन, (९) कुशीलवेष तथा ऋषिध्वज धारण करके उनसे अपनी जीविका चलाने वाले, (वेष-चिह्नजीवी), (१०) असंयमी होते हुए भी स्वयं को संयमी कहने वाले, (११) विषयविकारों के साथ मुनिधर्म के आराधक, (१२)लक्षणशास्त्र का प्रयोग करने वाले, (१३)निमित्तशास्त्र एवं कौतुककार्य में अत्यासक्त, (१४) जादू के खेल दिखा कर जीविका चलाने वाले, (१५) शीलविहीन, विपरीतदृष्टि, मुनिधर्मविराधक असाधुरूप साधु, (१६) औद्देशिक आदि अनेषणीय आहार-ग्रहणकर्ता, अग्निवत् सर्वभक्षी साधु, (१७) दुष्प्रवृत्तिशील दुरात्मा एवं संयमहीन साधक, (१८) अन्तिम समय की आराधना के विषय में विपरीतदृष्टि एवं उभयलोक-प्रयोजनभ्रष्ट साधु और (१९) यथाछन्द एवं कुशील तथा जिनमार्गविराधक साधु ।'
सीयंति-निग्रन्थधर्म के पालन में शिथिल हो जाते हैं, कतराते हैं। जो स्वयं निग्रन्थधर्म के पालन में दुःखानुभव करते हैं, वे स्व-पर की रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? अतएव उनकी अनाथता स्पष्ट है।
आउत्तया—सावधानी।
दुगुंछणाए : जुसुप्सनायां-उच्चार-प्रस्रवण आदि संयम के प्रति उपयोगशून्य होने से तथा परिष्ठापना जुगुप्सनीय होने से उसे "जुगुप्सना" कहा गया है। वीरजायं मग्गं–वीरों के द्वारा यात अर्थात्-जिस मार्ग पर वीर पुरुष चलते हैं, वह मार्ग।
मुंडरुचि-चिरकाल से सिर मुंडाने- अर्थात् केशलोच करने में जिसकी रुचि रही है, जो साधुजीवन के शेष आचार से विमुख रहता है, वह न तो तप करता है और न किसी नियम के पालन में रुचि रखता है।
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता-चिरकाल तक लोच आदि से अपने आप को क्लेशित करके - कष्ट देकर।
१. उत्तरा. मूलपाठ अ. २०, गा. ३८ से ५० तक
२. बृहद्वृत्ति, पत्र ४७८