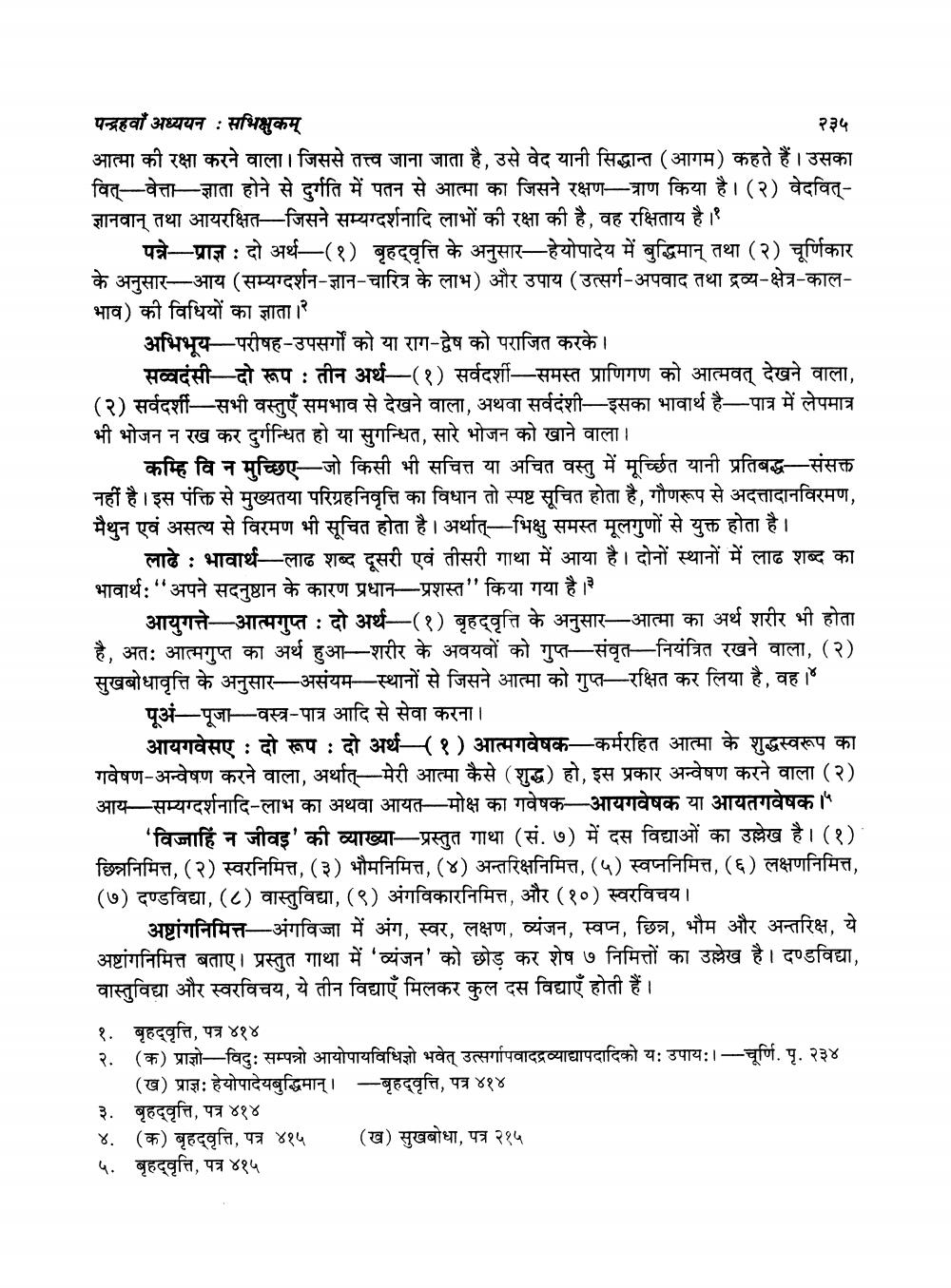________________
पन्द्रहवाँ अध्ययन : सभिक्षुकम्
२३५
आत्मा की रक्षा करने वाला। जिससे तत्त्व जाना जाता है, उसे वेद यानी सिद्धान्त (आगम) कहते हैं । उसका वित्― वेत्ता — ज्ञाता होने से दुर्गति में पतन से आत्मा का जिसने रक्षण - त्राण किया है। (२) वेदवित्ज्ञानवान् तथा आयरक्षित — जिसने सम्यग्दर्शनादि लाभों की रक्षा की है, वह रक्षिताय है ।
पन्ने — प्राज्ञ : दो अर्थ – (१) बृहद्वृत्ति के अनुसार — हेयोपादेय में बुद्धिमान् तथा (२) चूर्णिकार के :अनुसार — आय (सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र के लाभ) और उपाय ( उत्सर्ग-अपवाद तथा द्रव्य-क्षेत्र-कालभाव) की विधियों का ज्ञाता । २
अभिभूय परीषह - उपसर्गों को या राग-द्वेष को पराजित करके ।
सव्वदंसी- दो रूप : तीन अर्थ - (१) सर्वदर्शी – समस्त प्राणिगण को आत्मवत् देखने वाला, (२) सर्वदर्शी—सभी वस्तुएँ समभाव से देखने वाला, अथवा सर्वदंशी — इसका भावार्थ हैभी भोजन न रख कर दुर्गन्धित हो या सुगन्धित, सारे भोजन को खाने वाला।
- पात्र में लेपमात्र
कम्हि वि न मुच्छिए— जो किसी भी सचित्त या अचित वस्तु में मूर्च्छित यानी प्रतिबद्ध - संसक्त नहीं है। इस पंक्ति से मुख्यतया परिग्रहनिवृत्ति का विधान तो स्पष्ट सूचित होता है, गौणरूप से अदत्तादानविरमण, मैथुन एवं असत्य से विरमण भी सूचित होता है । अर्थात् — भिक्षु समस्त मूलगुणों से युक्त होता है ।
लाढे : भावार्थ - लाढ शब्द दूसरी एवं तीसरी गाथा में आया है। दोनों स्थानों में लाढ शब्द का भावार्थ: " अपने सदनुष्ठान के कारण प्रधान—प्रशस्त " किया गया है । ३
आयुगत्ते — आत्मगुप्त : दो अर्थ – (१) बृहद्वृत्ति के अनुसार — आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, अतः आत्मगुप्त का अर्थ हुआ - शरीर के अवयवों को गुप्त — संवृत — नियंत्रित रखने वाला, (२) सुखबोधावृत्ति के अनुसार — असंयम—स्थानों से जिसने आत्मा को गुप्त — रक्षित कर लिया है, वह । ४
पूअं — पूजा — वस्त्र - पात्र आदि से सेवा करना ।
आयगवेसए : दो रूप : दो अर्थ - ( १ ) आत्मगवेषक — कर्मरहित आत्मा के शुद्धस्वरूप का गवेषण - अन्वेषण करने वाला, अर्थात् — मेरी आत्मा कैसे (शुद्ध) हो, इस प्रकार अन्वेषण करने वाला (२) आय—— सम्यग्दर्शनादिद- लाभ का अथवा आयत — मोक्ष का गवेषक आयगवेषक या आयतगवेषक ।
'विज्जाहिं न जीवइ' की व्याख्या - प्रस्तुत गाथा (सं. ७) में दस विद्याओं का उल्लेख है । (१) छिन्ननिमित्त, (२) स्वरनिमित्त, (३) भौमनिमित्त, (४) अन्तरिक्षनिमित्त, (५) स्वननिमित्त, (६) लक्षणनिमित्त, (७) दण्डविद्या, (८) वास्तुविद्या, (९) अंगविकारनिमित्त, और (१०) स्वरविचय ।
अष्टांगनिमित्त — अंगविज्जा में अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौम और अन्तरिक्ष, ये अष्टांगनिमित्त बताए । प्रस्तुत गाथा में 'व्यंजन' को छोड़ कर शेष ७ निमित्तों का उल्लेख है । दण्डविद्या, वास्तुविद्या और स्वरविचय, ये तीन विद्याएँ मिलकर कुल दस विद्याएँ होती हैं ।
१. बृहद्वृत्ति, पत्र ४१४
२. (क) प्राज्ञो विदुः सम्पन्नो आयोपायविधिज्ञो भवेत् उत्सर्गापवादद्रव्याद्यापदादिको यः उपायः । - चूर्णि पृ. २३४ —बृहद्वृत्ति, पत्र ४१४
(ख) प्राज्ञ: हेयोपादेयबुद्धिमान् ।
(ख) सुखबोधा, पत्र २१५
३. बृहद्वृत्ति, पत्र ४१४
४. (क) बृहद्वृत्ति, पत्र ४१५ ५. बृहद्वृत्ति, पत्र ४१५