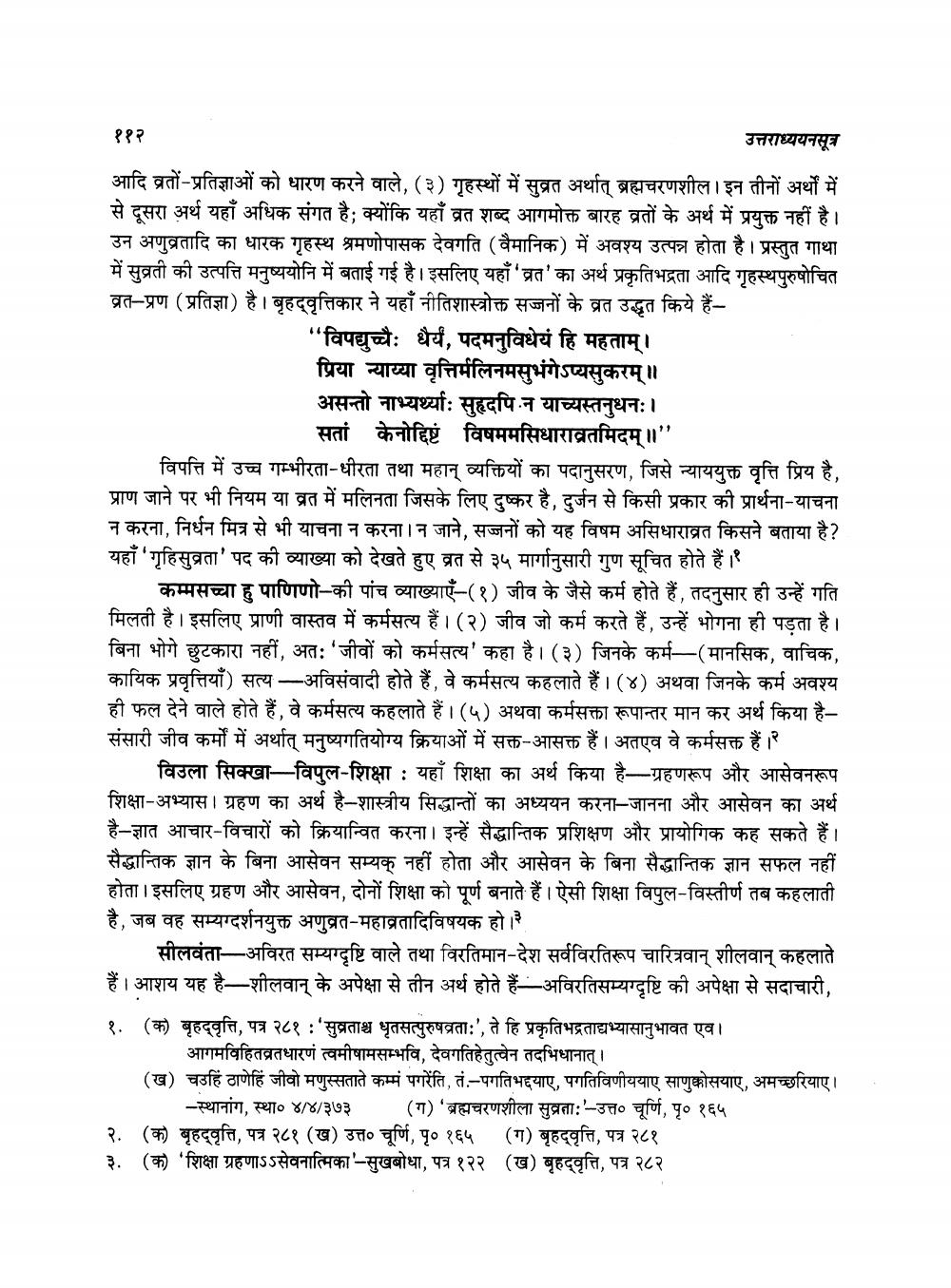________________
११२
उत्तराध्ययनसूत्र
आदि व्रतों-प्रतिज्ञाओं को धारण करने वाले, (३) गृहस्थों में सुव्रत अर्थात् ब्रह्मचरणशील। इन तीनों अर्थों में से दूसरा अर्थ यहाँ अधिक संगत है; क्योंकि यहाँ व्रत शब्द आगमोक्त बारह व्रतों के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। उन अणुव्रतादि का धारक गृहस्थ श्रमणोपासक देवगति (वैमानिक) में अवश्य उत्पन्न होता है। प्रस्तुत गाथा में सुव्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बताई गई है। इसलिए यहाँ 'व्रत' का अर्थ प्रकृतिभद्रता आदि गृहस्थपुरुषोचित व्रत-प्रण (प्रतिज्ञा) है। बृहवृत्तिकार ने यहाँ नीतिशास्त्रोक्त सज्जनों के व्रत उद्धृत किये हैं
"विपधुच्चैः धैर्य, पदमनुविधेयं हि महताम्। प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभंगेऽप्यसुकरम्॥ असन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यस्तनुधनः।
सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्॥" विपत्ति में उच्च गम्भीरता-धीरता तथा महान् व्यक्तियों का पदानुसरण, जिसे न्याययुक्त वृत्ति प्रिय है, प्राण जाने पर भी नियम या व्रत में मलिनता जिसके लिए दुष्कर है, दुर्जन से किसी प्रकार की प्रार्थना-याचना न करना, निर्धन मित्र से भी याचना न करना। न जाने, सज्जनों को यह विषम असिधाराव्रत किसने बताया है? यहाँ 'गृहिसुव्रता' पद की व्याख्या को देखते हुए व्रत से ३५ मार्गानुसारी गुण सूचित होते हैं।
___कम्मसच्चा हु पाणिणो की पांच व्याख्याएँ-(१) जीव के जैसे कर्म होते हैं, तदनुसार ही उन्हें गति मिलती है। इसलिए प्राणी वास्तव में कर्मसत्य हैं । (२) जीव जो कर्म करते हैं, उन्हें भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे छुटकारा नहीं, अत: 'जीवों को कर्मसत्य' कहा है। (३) जिनके कर्म-(मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियाँ) सत्य -अविसंवादी होते हैं, वे कर्मसत्य कहलाते हैं। (४) अथवा जिनके कर्म अवश्य ही फल देने वाले होते हैं, वे कर्मसत्य कहलाते हैं। (५) अथवा कर्मसक्ता रूपान्तर मान कर अर्थ किया हैसंसारी जीव कर्मों में अर्थात् मनुष्यगतियोग्य क्रियाओं में सक्त-आसक्त हैं । अतएव वे कर्मसक्त हैं।२
विउला सिक्खा–विपुल-शिक्षा : यहाँ शिक्षा का अर्थ किया है—ग्रहणरूप और आसेवनरूप शिक्षा-अभ्यास । ग्रहण का अर्थ है-शास्त्रीय सिद्धान्तों का अध्ययन करना-जानना और आसेवन का अर्थ है-ज्ञात आचार-विचारों को क्रियान्वित करना। इन्हें सैद्धान्तिक प्रशिक्षण और प्रायोगिक कह सकते हैं। सैद्धान्तिक ज्ञान के बिना आसेवन सम्यक् नहीं होता और आसेवन के बिना सैद्धान्तिक ज्ञान सफल नहीं होता। इसलिए ग्रहण और आसेवन, दोनों शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं। ऐसी शिक्षा विपुल-विस्तीर्ण तब कहलाती है, जब वह सम्यग्दर्शनयुक्त अणुव्रत-महाव्रतादिविषयक हो।
सीलवंता-अविरत सम्यग्दृष्टि वाले तथा विरतिमान-देश सर्वविरतिरूप चारित्रवान् शीलवान् कहलाते हैं। आशय यह है-शीलवान् के अपेक्षा से तीन अर्थ होते हैं-अविरतिसम्यग्दृष्टि की अपेक्षा से सदाचारी, १. (क) बृहवृत्ति, पत्र २८१ : 'सुव्रताश्च धृतसत्पुरुषव्रताः', ते हि प्रकृतिभद्रताद्यभ्यासानुभावत एव।
आगमविहितव्रतधारणं त्वमीषामसम्भवि, देवगतिहेतुत्वेन तदभिधानात्। (ख) चउहिं ठाणेहिं जीवो मणुस्सताते कम्मं पगरेंति, तं.-पगतिभद्दयाए, पगतिविणीययाए साणुकोसयाए, अमच्छरियाए।
-स्थानांग, स्था० ४/४/३७३ (ग) ब्रह्मचरणशीला सुव्रता:'-उत्त० चूर्णि, पृ० १६५ २. (क) बृहद्वृत्ति, पत्र २८१ (ख) उत्त० चूर्णि, पृ० १६५ (ग) बृहवृत्ति, पत्र २८१ ३. (क) 'शिक्षा ग्रहणाऽऽसेवनात्मिका'-सुखबोधा, पत्र १२२ (ख) बृहद्वृत्ति, पत्र २८२