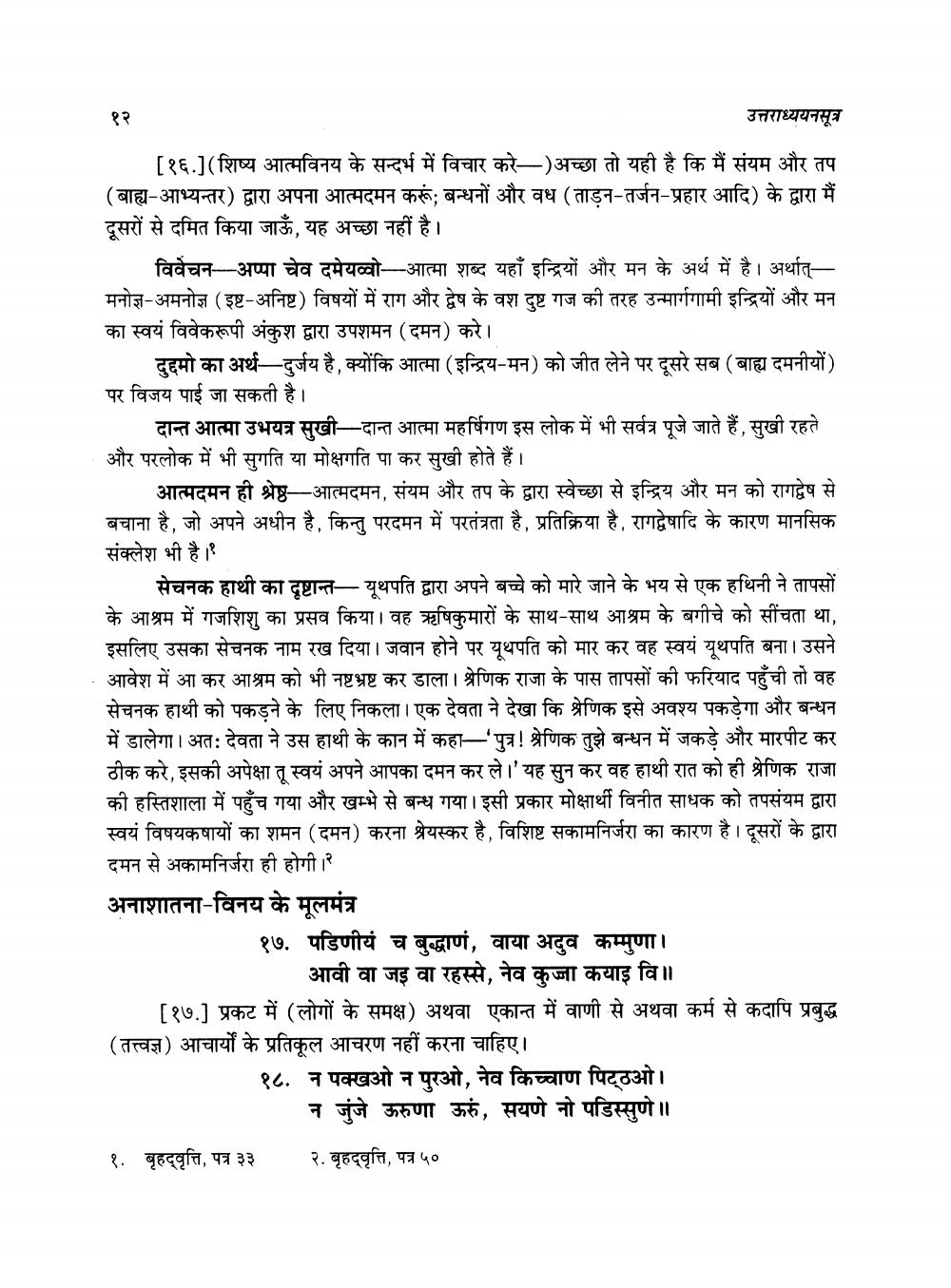________________
उत्तराध्ययनसूत्र
[१६.] (शिष्य आत्मविनय के सन्दर्भ में विचार करे) अच्छा तो यही है कि मैं संयम और तप (बाह्य-आभ्यन्तर) द्वारा अपना आत्मदमन करूं; बन्धनों और वध (ताड़न - तर्जन - प्रहार आदि) के द्वारा दूसरों से दमित किया जाऊँ, यह अच्छा नहीं है।
१२
विवेचन- -अप्पा चेव दमेयव्वो-आत्मा शब्द यहाँ इन्द्रियों और मन के अर्थ में है। अर्थात्— मनोज्ञ-अमनोज्ञ (इष्ट-अनिष्ट) विषयों में राग और द्वेष के वश दुष्ट गज की तरह उन्मार्गगामी इन्द्रियों और मन का स्वयं विवेकरूपी अंकुश द्वारा उपशमन (दमन) करे।
दुद्दमो का अर्थ - दुर्जय है, क्योंकि आत्मा (इन्द्रिय-मन) को जीत लेने पर दूसरे सब (बाह्य दमनीयों) पर विजय पाई जा सकती है।
दान्त आत्मा उभयत्र सुखी — दान्त आत्मा महर्षिगण इस लोक में भी सर्वत्र पूजे जाते हैं, सुखी रहते और परलोक में भी सुगति या मोक्षगति पा कर सुखी होते हैं
I
आत्मदमन ही श्रेष्ठ— आत्मदमन, संयम और तप के द्वारा स्वेच्छा से इन्द्रिय और मन को रागद्वेष से बचाना है, जो अपने अधीन है, किन्तु परदमन में परतंत्रता है, प्रतिक्रिया है, रागद्वेषादि के कारण मानसिक संक्लेश भी है।
सेचनक हाथी का दृष्टान्त — यूथपति द्वारा अपने बच्चे को मारे जाने के भय से एक हथिनी ने तापसों आश्रम में गजशिशु का प्रसव किया। वह ऋषिकुमारों के साथ-साथ आश्रम के बगीचे को सींचता था, इसलिए उसका सेचनक नाम रख दिया। जवान होने पर यूथपति को मार कर वह स्वयं यूथपति बना । उसने आवेश में आकर आश्रम को भी नष्टभ्रष्ट कर डाला। श्रेणिक राजा के पास तापसों की फरियाद पहुँची तो वह सेचनक हाथी को पकड़ने के लिए निकला। एक देवता ने देखा कि श्रेणिक इसे अवश्य पकड़ेगा और बन्धन में डालेगा। अतः देवता ने उस हाथी के कान में कहा - 'पुत्र ! श्रेणिक तुझे बन्धन में जकड़े और मारपीट कर ठीक करे, इसकी अपेक्षा तू स्वयं अपने आपका दमन कर ले।' यह सुन कर वह हाथी रात को ही श्रेणिक राजा की हस्तिशाला में पहुँच गया और खम्भे से बन्ध गया। इसी प्रकार मोक्षार्थी विनीत साधक को तपसंयम द्वारा स्वयं विषयकषायों का शमन (दमन) करना श्रेयस्कर है, विशिष्ट सकामनिर्जरा का कारण है। दूसरों के द्वारा दमन से अकामनिर्जरा ही होगी । २
अनाशातना - विनय के मूलमंत्र
१७.
पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा । आवी वा जड़ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ॥
[१७] प्रकट में (लोगों के समक्ष ) अथवा एकान्त में वाणी से अथवा कर्म से कदापि प्रबुद्ध (तत्त्वज्ञ) आचार्यों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए।
१८. न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ । न जुंजे ऊरुणा ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥
२. बृहद्वृत्ति, पत्र ५०
१. बृहद्वृत्ति, पत्र ३३