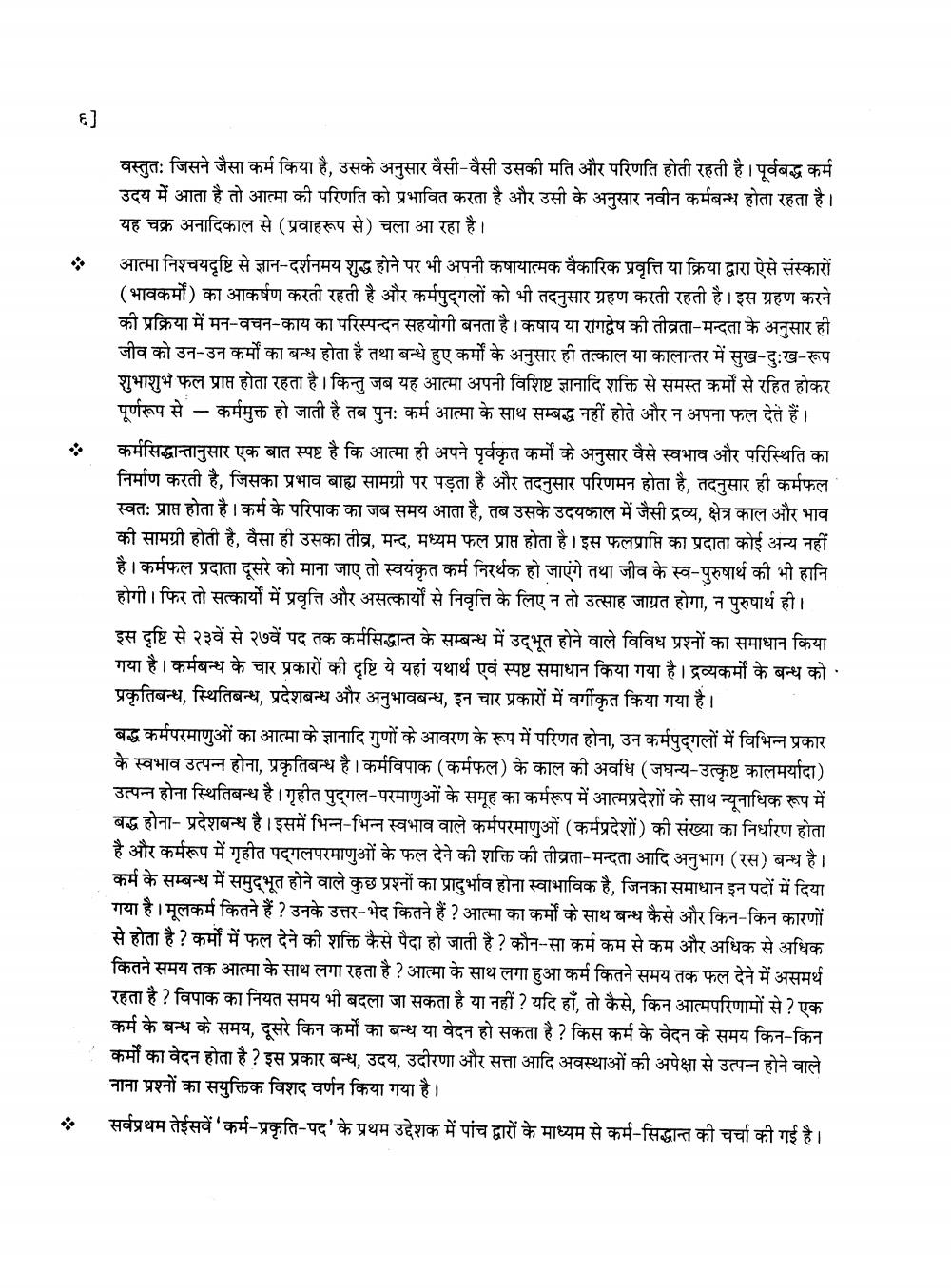________________
६]
वस्तुतः जिसने जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार वैसी वैसी उसकी मति और परिणति होती रहती है। पूर्वबद्ध कर्म उदय में आता है तो आत्मा की परिणति को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार नवीन कर्मबन्ध होता रहता है। यह चक्र अनादिकाल से ( प्रवाहरूप से चला आ रहा है।
-
आत्मा निश्चयदृष्टि से ज्ञान दर्शनमय शुद्ध होने पर भी अपनी कषायात्मक वैकारिक प्रवृत्ति या क्रिया द्वारा ऐसे संस्कारों (भावकर्मों) का आकर्षण करती रहती है और कर्मपुद्गलों को भी तदनुसार ग्रहण करती रहती है। इस ग्रहण करने की प्रक्रिया में मन-वचन-काय का परिस्पन्दन सहयोगी बनता है। कषाय या रागद्वेष की तीव्रता मन्दता के अनुसार ही जीव को उन-उन कर्मों का बन्ध होता है तथा बन्धे हुए कर्मों के अनुसार ही तत्काल या कालान्तर में सुख-दुःख-रूप शुभाशुभ फल प्राप्त होता रहता है। किन्तु जब यह आत्मा अपनी विशिष्ट ज्ञानादि शक्ति से समस्त कर्मों से रहित होकर पूर्णरूप से • कर्ममुक्त हो जाती है तब पुनः कर्म आत्मा के साथ सम्बद्ध नहीं होते और न अपना फल देते हैं। कर्मसिद्धान्तानुसार एक बात स्पष्ट है कि आत्मा ही अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार वैसे स्वभाव और परिस्थिति का निर्माण करती है, जिसका प्रभाव बाह्य सामग्री पर पड़ता है और तदनुसार परिणमन होता है, तदनुसार ही कर्मफल स्वतः प्राप्त होता है। कर्म के परिपाक का जब समय आता है, तब उसके उदयकाल में जैसी द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की सामग्री होती है, वैसा ही उसका तीव्र, मन्द, मध्यम फल प्राप्त होता है। इस फलप्राप्ति का प्रदाता कोई अन्य नहीं है । कर्मफल प्रदाता दूसरे को माना जाए तो स्वयंकृत कर्म निरर्थक हो जाएंगे तथा जीव के स्व-पुरुषार्थ की भी हानि होगी। फिर तो सत्कार्यों में प्रवृत्ति और असत्कार्यों से निवृत्ति के लिए न तो उत्साह जाग्रत होगा, न पुरुषार्थ ही ।
इस दृष्टि से २३वें से २७वें पद तक कर्मसिद्धान्त के सम्बन्ध में उद्भूत होने वाले विविध प्रश्नों का समाधान किया गया है। कर्मबन्ध के चार प्रकारों की दृष्टि ये यहां यथार्थ एवं स्पष्ट समाधान किया गया है। द्रव्यकर्मों के बन्ध को प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, प्रदेशबन्ध और अनुभावबन्ध, इन चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
.
बद्ध कर्मपरमाणुओं का आत्मा के ज्ञानादि गुणों के आवरण के रूप में परिणत होना, उन कर्मपुद्गलों में विभिन्न प्रकार के स्वभाव उत्पन्न होना, प्रकृतिबन्ध है। कर्मविपाक (कर्मफल) के काल की अवधि ( जघन्य उत्कृष्ट कालमर्यादा) उत्पन्न होना स्थितिबन्ध है। गृहीत पुद्गल परमाणुओं के समूह का कर्मरूप में आत्मप्रदेशों के साथ न्यूनाधिक रूप में बद्ध होना- प्रदेशबन्ध है । इसमें भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले कर्मपरमाणुओं (कर्मप्रदेशों) की संख्या का निर्धारण होता है और कर्मरूप में गृहीत पद्गलपरमाणुओं के फल देने की शक्ति की तीव्रता - मन्दता आदि अनुभाग (रस) बन्ध है। कर्म के सम्बन्ध में समुद्भूत होने वाले कुछ प्रश्नों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है, जिनका समाधान इन पदों में दिया गया है। मूलकर्म कितने हैं? उनके उत्तर-भेद कितने हैं ? आत्मा का कर्मों के साथ बन्ध कैसे और किन-किन कारणों से होता है ? कर्मों में फल देने की शक्ति कैसे पैदा हो जाती है ? कौन-सा कर्म कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय तक आत्मा के साथ लगा रहता है ? आत्मा के साथ लगा हुआ कर्म कितने समय तक फल देने में असमर्थ रहता है ? विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं ? यदि हाँ, तो कैसे, किन आत्मपरिणामों से ? एक कर्म के बन्ध के समय दूसरे किन कर्मों का बन्ध या वेदन हो सकता है ? किस कर्म के वेदन के समय किन-किन कर्मों का वेदन होता है ? इस प्रकार बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता आदि अवस्थाओं की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले नाना प्रश्नों का सयुक्तिक विशद वर्णन किया गया है।
सर्वप्रथम तेईसवें 'कर्म-प्रकृति-पद' के प्रथम उद्देशक में पांच द्वारों के माध्यम से कर्म सिद्धान्त की चर्चा की गई है।