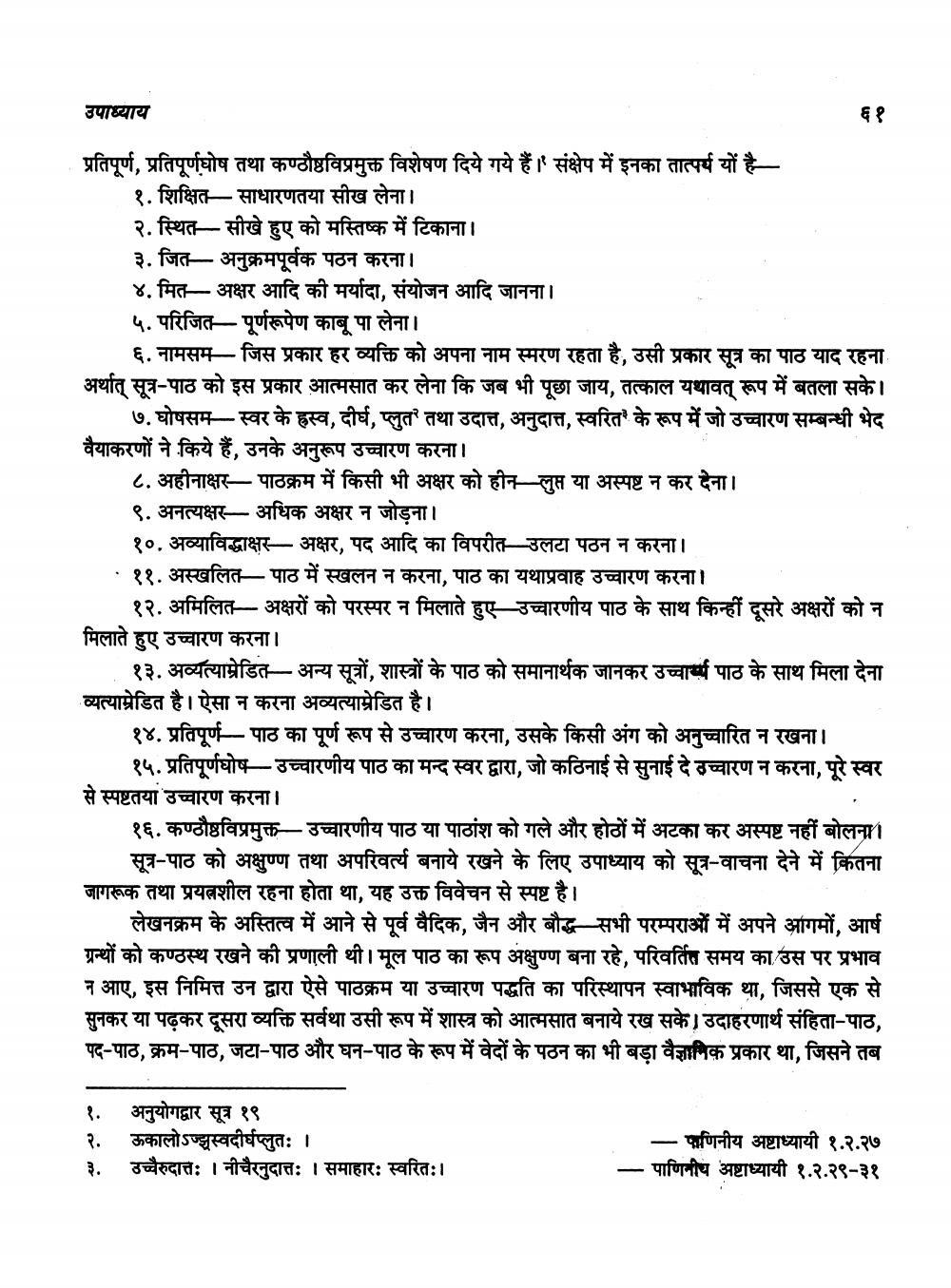________________
उपाध्याय
प्रतिपूर्ण, प्रतिपूर्णघोष तथा कण्ठोष्ठविप्रमुक्त विशेषण दिये गये हैं। संक्षेप में इनका तात्पर्य यों है
१. शिक्षित- साधारणतया सीख लेना। २. स्थित- सीखे हुए को मस्तिष्क में टिकाना। ३. जित- अनुक्रमपूर्वक पठन करना। ४. मित- अक्षर आदि की मर्यादा, संयोजन आदि जानना। ५. परिजित- पूर्णरूपेण काबू पा लेना।
६. नामसम-जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपना नाम स्मरण रहता है, उसी प्रकार सूत्र का पाठ याद रहना अर्थात् सूत्र-पाठ को इस प्रकार आत्मसात कर लेना कि जब भी पूछा जाय, तत्काल यथावत् रूप में बतला सके।
७. घोषसम-स्वर के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तथा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित' के रूप में जो उच्चारण सम्बन्धी भेद वैयाकरणों ने किये हैं, उनके अनुरूप उच्चारण करना।
८. अहीनाक्षर- पाठक्रम में किसी भी अक्षर को हीन-लुप्त या अस्पष्ट न कर देना। ९. अनत्यक्षर- अधिक अक्षर न जोड़ना। १०. अव्याविद्धाक्षर- अक्षर, पद आदि का विपरीत-उलटा पठन न करना। . ११. अस्खलित- पाठ में स्खलन न करना, पाठ का यथाप्रवाह उच्चारण करना।
१२. अमिलित- अक्षरों को परस्पर न मिलाते हुए उच्चारणीय पाठ के साथ किन्हीं दूसरे अक्षरों को न मिलाते हुए उच्चारण करना।
१३. अव्यत्यानेडित- अन्य सूत्रों, शास्त्रों के पाठ को समानार्थक जानकर उच्चार्य पाठ के साथ मिला देना व्यत्यानेडित है। ऐसा न करना अव्यत्यानेडित है।
१४. प्रतिपूर्ण- पाठ का पूर्ण रूप से उच्चारण करना, उसके किसी अंग को अनुच्चारित न रखना।
१५. प्रतिपूर्णघोष– उच्चारणीय पाठ का मन्द स्वर द्वारा, जो कठिनाई से सुनाई दे उच्चारण न करना, पूरे स्वर से स्पष्टतया उच्चारण करना।
१६. कण्ठोष्ठविप्रमुक्त- उच्चारणीय पाठ या पाठांश को गले और होठों में अटका कर अस्पष्ट नहीं बोलना।
सूत्र-पाठ को अक्षुण्ण तथा अपरिवर्त्य बनाये रखने के लिए उपाध्याय को सूत्र-वाचना देने में कितना जागरूक तथा प्रयत्नशील रहना होता था, यह उक्त विवेचन से स्पष्ट है।
लेखनक्रम के अस्तित्व में आने से पूर्व वैदिक, जैन और बौद्ध-सभी परम्पराओं में अपने आगमों, आर्ष ग्रन्थों को कण्ठस्थ रखने की प्रणाली थी। मूल पाठ का रूप अक्षुण्ण बना रहे, परिवर्तित समय का उस पर प्रभाव न आए, इस निमित्त उन द्वारा ऐसे पाठक्रम या उच्चारण पद्धति का परिस्थापन स्वाभाविक था, जिससे एक से सुनकर या पढ़कर दूसरा व्यक्ति सर्वथा उसी रूप में शास्त्र को आत्मसात बनाये रख सके। उदाहरणार्थ संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ और घन-पाठ के रूप में वेदों के पठन का भी बड़ा वैज्ञानिक प्रकार था, जिसने तब
१. अनुयोगद्वार सूत्र १९ २. ऊकालोऽज्यस्वदीर्घप्लुतः । ३. उच्चैरुदात्तः । नीचैरनुदात्तः । समाहारः स्वरितः।
-पाणिनीय अष्टाध्यायी १.२.२७ - पाणिनीय अष्टाध्यायी १.२.२९-३१