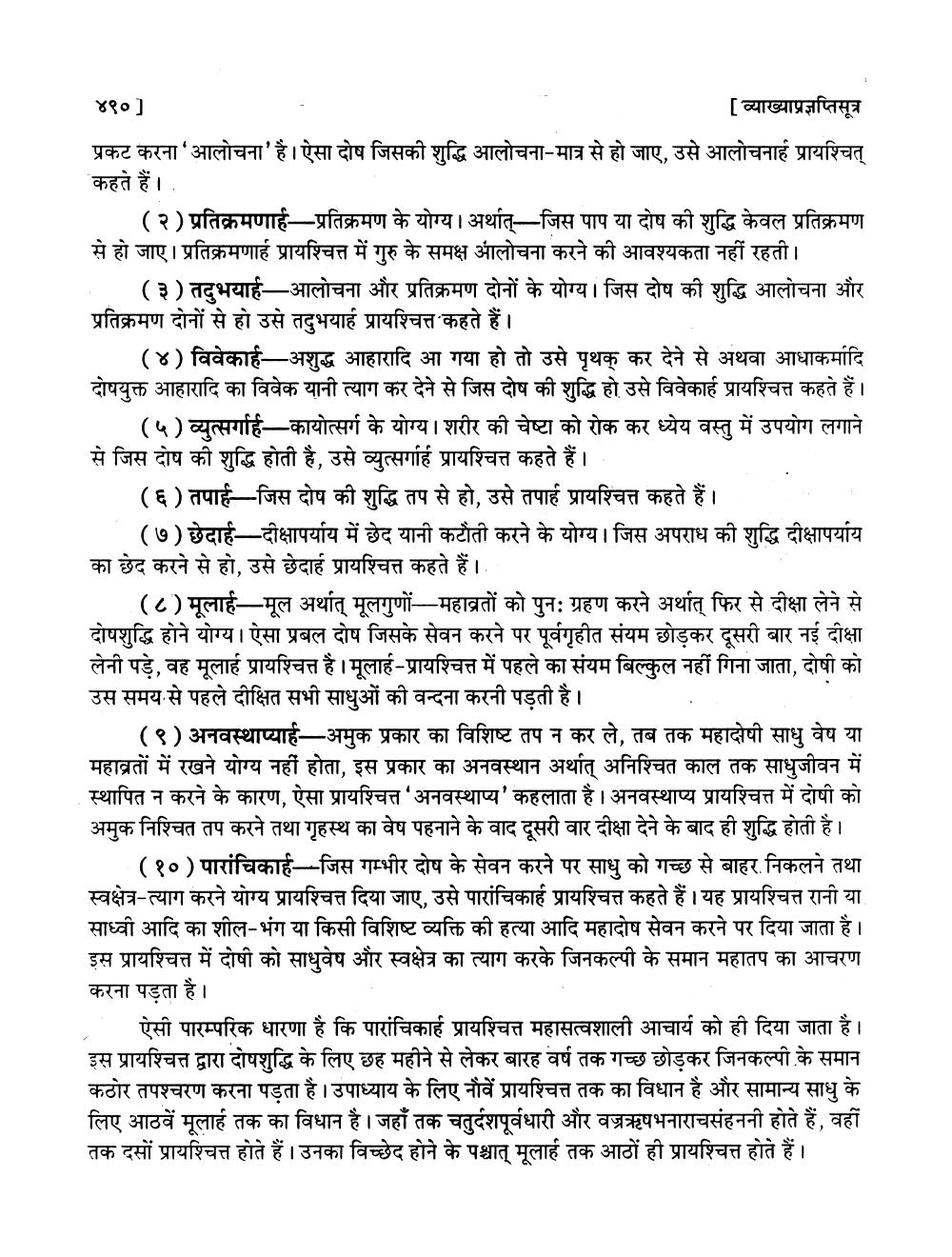________________
[ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र
४९० ]
प्रकट करना 'आलोचना' है। ऐसा दोष जिसकी शुद्धि आलोचना मात्र से हो जाए, उसे आलोचनार्ह प्रायश्चित् कहते हैं।
(२) प्रतिक्रमणार्ह — प्रतिक्रमण के योग्य । अर्थात् — जिस पाप या दोष की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण से हो जाए। प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त में गुरु के समक्ष आलोचना करने की आवश्यकता नहीं रहती ।
( ३ ) तदुभयार्ह—आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य । जिस दोष की शुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से हो उसे तदुभयार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं ।
(४) विवेकार्ह — अशुद्ध आहारादि आ गया हो तो उसे पृथक् कर देने से अथवा आधाकर्मादि दोषयुक्त आहारादि का विवेक यानी त्याग कर देने से जिस दोष की शुद्धि हो उसे विवेकार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं । ( ५ ) व्युत्सर्गार्ह—कायोत्सर्ग के योग्य । शरीर की चेष्टा को रोक कर ध्येय वस्तु में उपयोग लगाने से जिस दोष की शुद्धि होती हैं, उसे व्युत्सर्गार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं ।
(६) तपाई — जिस दोष की शुद्धि तप से हो, उसे तपार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं ।
(७) छेदार्ह— दीक्षापर्याय में छेद यानी कटौती करने के योग्य । जिस अपराध की शुद्धि दीक्षापर्याय का छेद करने से हो, उसे छेदार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं ।
(८) मूलाई — मूल अर्थात् मूलगुणों - महाव्रतों को पुनः ग्रहण करने अर्थात् फिर से दीक्षा लेने से दोषशुद्धि होने योग्य। ऐसा प्रबल दोष जिसके सेवन करने पर पूर्वगृहीत संयम छोड़कर दूसरी बार नई दीक्षा लेनी पड़े, वह मूलार्ह प्रायश्चित्त है। मूलाई प्रायश्चित्त में पहले का संयम बिल्कुल नहीं गिना जाता, दोषी को उस समय से पहले दीक्षित सभी साधुओं की वन्दना करनी पड़ती है।
( ९ ) अनवस्थाप्यार्ह — अमुक प्रकार का विशिष्ट तप न कर ले, तब तक महादोषी साधु वेष या महाव्रतों में रखने योग्य नहीं होता, इस प्रकार का अनवस्थान अर्थात् अनिश्चित काल तक साधुजीवन में स्थापित न करने के कारण, ऐसा प्रायश्चित्त 'अनवस्थाप्य' कहलाता है। अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त में दोषी को अमुक निश्चित तप करने तथा गृहस्थ का वेष पहनाने के वाद दूसरी वार दीक्षा देने के बाद ही शुद्धि होती है।
(१०) पारांचिकाई -- जिस गम्भीर दोष के सेवन करने पर साधु को गच्छ से बाहर निकलने तथा स्वक्षेत्र-त्याग करने योग्य प्रायश्चित्त दिया जाए, उसे पारांचिकार्ह प्रायश्चित्त कहते हैं। यह प्रायश्चित्त रानी या साध्वी आदि का शील भंग या किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या आदि महादोष सेवन करने पर दिया जाता है । इस प्रायश्चित्त में दोषी को साधुवेष और स्वक्षेत्र का त्याग करके जिनकल्पी के समान महातप का आचरण करना पड़ता है।
ऐसी पारम्परिक धारणा है कि पारांचिकार्ह प्रायश्चित्त महासत्वशाली आचार्य को ही दिया जाता है। इस प्रायश्चित्त द्वारा दोषशुद्धि के लिए छह महीने से लेकर बारह वर्ष तक गच्छ छोड़कर जिनकल्पी के समान कठोर तपश्चरण करना पड़ता है । उपाध्याय के लिए नौवें प्रायश्चित्त तक का विधान है और सामान्य साधु के लिए आठवें मूलार्ह तक का विधान है। जहाँ तक चतुर्दशपूर्वधारी और वज्रऋषभनाराचसंहननी होते हैं, वहीँ तक दसों प्रायश्चित्त होते हैं। उनका विच्छेद होने के पश्चात् मूलार्ह तक आठों ही प्रायश्चित्त होते हैं ।