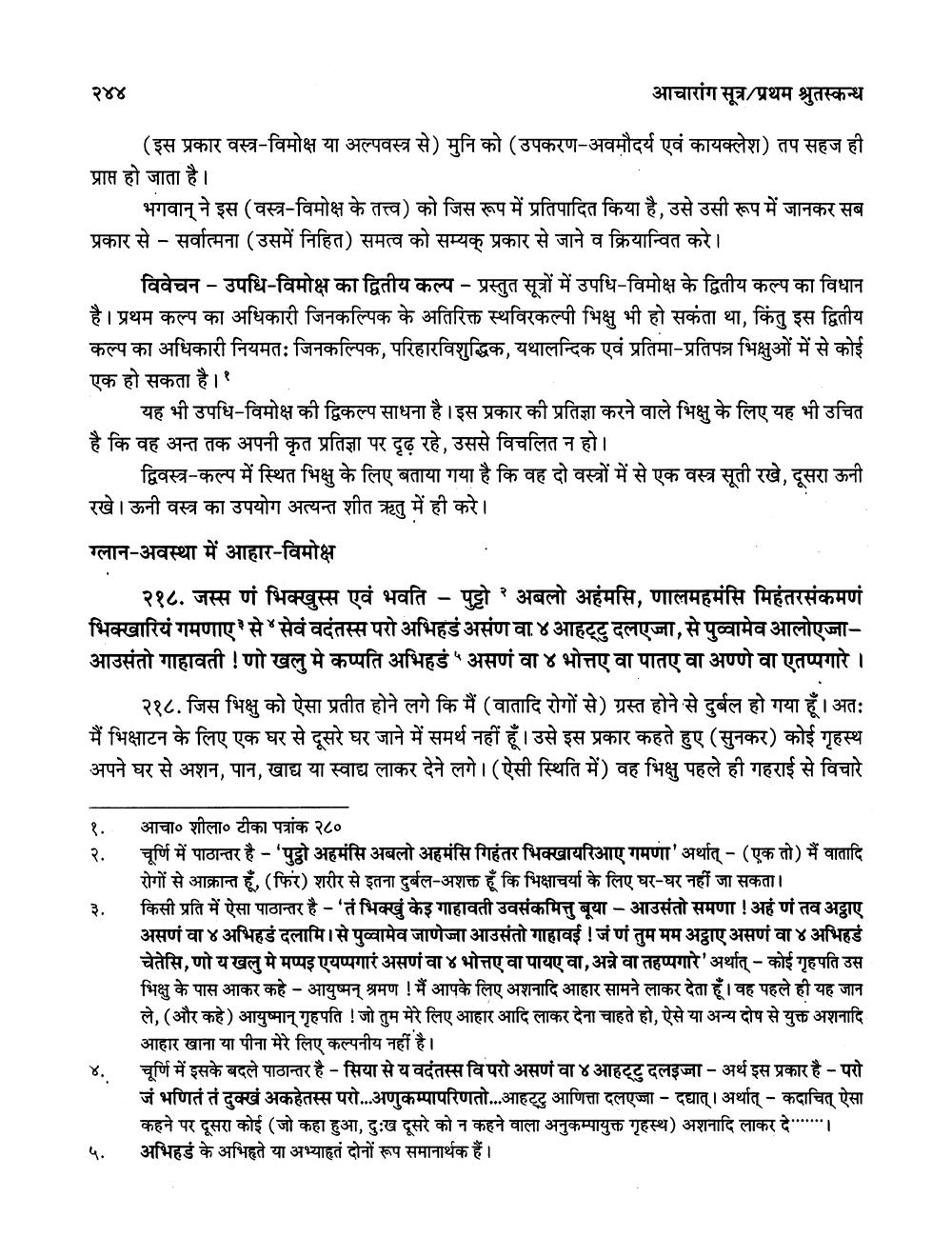________________
२४४
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध
(इस प्रकार वस्त्र-विमोक्ष या अल्पवस्त्र से) मुनि को (उपकरण-अवमौदर्य एवं कायक्लेश) तप सहज ही प्राप्त हो जाता है।
भगवान् ने इस (वस्त्र-विमोक्ष के तत्त्व) को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से - सर्वात्मना (उसमें निहित) समत्व को सम्यक् प्रकार से जाने व क्रियान्वित करे।
विवेचन - उपधि-विमोक्ष का द्वितीय कल्प - प्रस्तुत सूत्रों में उपधि-विमोक्ष के द्वितीय कल्प का विधान है। प्रथम कल्प का अधिकारी जिनकल्पिक के अतिरिक्त स्थविरकल्पी भिक्षु भी हो सकता था, किंतु इस द्वितीय कल्प का अधिकारी नियमतः जिनकल्पिक, परिहारविशुद्धिक, यथालन्दिक एवं प्रतिमा-प्रतिपन्न भिक्षुओं में से कोई एक हो सकता है।
यह भी उपधि-विमोक्ष की द्विकल्प साधना है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाले भिक्षु के लिए यह भी उचित है कि वह अन्त तक अपनी कृत प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, उससे विचलित न हो।
द्विवस्त्र-कल्प में स्थित भिक्षु के लिए बताया गया है कि वह दो वस्त्रों में से एक वस्त्र सूती रखे, दूसरा ऊनी रखे। ऊनी वस्त्र का उपयोग अत्यन्त शीत ऋतु में ही करे। ग्लान-अवस्था में आहार-विमोक्ष
२१८. जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति - पुट्टो २ अबलो अहंमसि, णालमहमंसि मिहंतरसंकमणं भिक्खारियं गमणाए से सेवं वदंतस्स परो अभिहडं असंण वा. ४ आहटु दलएजा, से पुत्वामेव आलोएज्जाआउसंतो गाहावती ! णो खलु मे कप्पति अभिहडं ५ असणं वा ४ भोत्तए वा पातए वा अण्णे वा एतप्पगारे ।
२१८. जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होने लगे कि मैं (वातादि रोगों से) ग्रस्त होने से दुर्बल हो गया हूँ। अतः मैं भिक्षाटन के लिए एक घर से दूसरे घर जाने में समर्थ नहीं हूँ। उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्थ अपने घर से अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर देने लगे। (ऐसी स्थिति में) वह भिक्षु पहले ही गहराई से विचारे
२.
आचा० शीला० टीका पत्रांक २८० चूर्णि में पाठान्तर है - 'पुट्ठो अहमंसि अबलो अहमंसि गिहतर भिक्खायरिआए गमणा' अर्थात् - (एक तो) मैं वातादि रोगों से आक्रान्त हूँ, (फिर) शरीर से इतना दुर्बल-अशक्त हूँ कि भिक्षाचर्या के लिए घर-घर नहीं जा सकता। किसी प्रति में ऐसा पाठान्तर है - 'तं भिक्खं केइ गाहावती उवसंकमित्तु बूया -आउसंतो समणा ! अहं णं तव अट्ठाए असणं वा ४ अभिहडं दलामि। से पुव्वामेव जाणेजा आउसंतो गाहावई !जंणं तुम मम अट्ठाए असणं वा ४ अभिहडं चेतेसि,णो यखलु मे मप्पइ एयप्पगारं असणं वा ४ भोत्तए वा पायए वा,अन्ने वा तहप्पगारे' अर्थात् - कोई गृहपति उस भिक्षु के पास आकर कहे - आयुष्मन् श्रमण ! मैं आपके लिए अशनादि आहार सामने लाकर देता हूँ। वह पहले ही यह जान ले, (और कहे) आयुष्मान् गृहपति ! जो तुम मेरे लिए आहार आदि लाकर देना चाहते हो, ऐसे या अन्य दोष से युक्त अशनादि आहार खाना या पीना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। चूर्णि में इसके बदले पाठान्तर है - सिया से य वदंतस्स विपरो असणं वा ४ आहट्ट दलइज्जा- अर्थ इस प्रकार है - परो जं भणितं तं दुक्खं अकहेतस्स परो...अणुकम्पापरिणतो...आहट्ट आणित्ता दलएज्जा - दद्यात् । अर्थात् - कदाचित् ऐसा कहने पर दूसरा कोई (जो कहा हुआ, दुःख दूसरे को न कहने वाला अनुकम्पायुक्त गृहस्थ) अशनादि लाकर दे । अभिहडं के अभिहते या अभ्याहृतं दोनों रूप समानार्थक हैं।