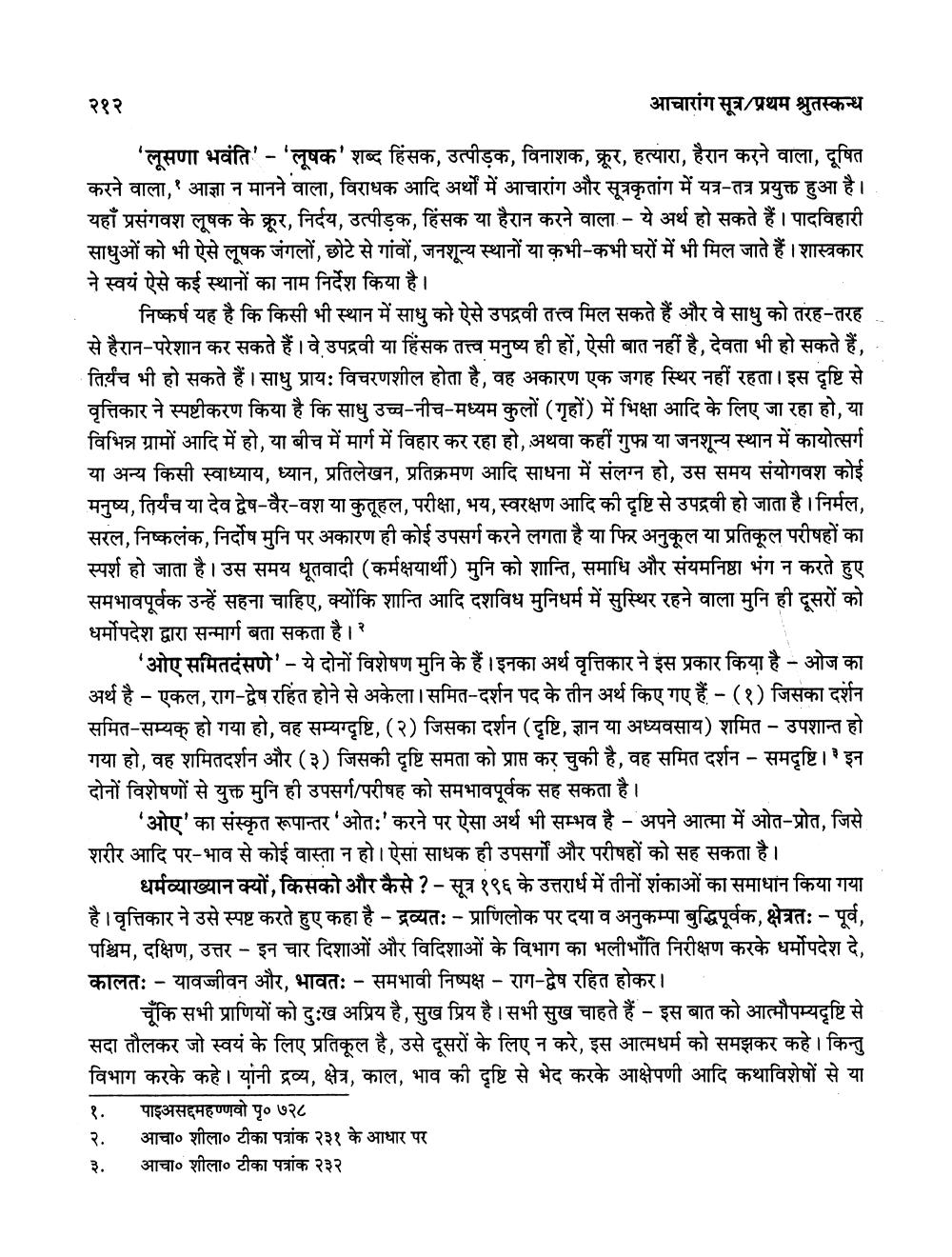________________
२१२
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध ___ 'लूसणा भवंति' - 'लूषक' शब्द हिंसक, उत्पीड़क, विनाशक, क्रूर, हत्यारा, हैरान करने वाला, दूषित करने वाला, आज्ञा न मानने वाला, विराधक आदि अर्थों में आचारांग और सूत्रकृतांग में यत्र-तत्र प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगवश लूषक के क्रूर, निर्दय, उत्पीड़क, हिंसक या हैरान करने वाला - ये अर्थ हो सकते हैं। पादविहारी साधुओं को भी ऐसे लूषक जंगलों, छोटे से गांवों, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरों में भी मिल जाते हैं । शास्त्रकार ने स्वयं ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है।
निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान में साधु को ऐसे उपद्रवी तत्त्व मिल सकते हैं और वे साधु को तरह-तरह से हैरान-परेशान कर सकते हैं । वे उपद्रवी या हिंसक तत्त्व मनुष्य ही हों, ऐसी बात नहीं है, देवता भी हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं। साधु प्रायः विचरणशील होता है, वह अकारण एक जगह स्थिर नहीं रहता। इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलों (गृहों) में भिक्षा आदि के लिए जा रहा हो, या विभिन्न ग्रामों आदि में हो, या बीच में मार्ग में विहार कर रहा हो, अथवा कहीं गुफा या जनशून्य स्थान में कायोत्सर्ग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि साधना में संलग्न हो, उस समय संयोगवश कोई मनुष्य, तिर्यंच या देव द्वेष-वैर-वश या कुतूहल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण आदि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मल, सरल, निष्कलंक, निर्दोष मुनि पर अकारण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर अनुकूल या प्रतिकूल परीषहों का स्पर्श हो जाता है। उस समय धूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि और संयमनिष्ठा भंग न करते हुए समभावपूर्वक उन्हें सहना चाहिए, क्योंकि शान्ति आदि दशविध मुनिधर्म में सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरों को धर्मोपदेश द्वारा सन्मार्ग बता सकता है। ___'ओए समितदंसणे' - ये दोनों विशेषण मुनि के हैं। इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है - ओज का अर्थ है - एकल, राग-द्वेष रहित होने से अकेला । समित-दर्शन पद के तीन अर्थ किए गए हैं - (१) जिसका दर्शन समित-सम्यक् हो गया हो, वह सम्यग्दृष्टि, (२) जिसका दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अध्यवसाय) शमित - उपशान्त हो गया हो, वह शमितदर्शन और (३) जिसकी दृष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित दर्शन - समदृष्टि । ३ इन दोनों विशेषणों से युक्त मुनि ही उपसर्ग/परीषह को समभावपूर्वक सह सकता है।
___ 'ओए' का संस्कृत रूपान्तर 'ओतः' करने पर ऐसा अर्थ भी सम्भव है - अपने आत्मा में ओत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्ता न हो। ऐसा साधक ही उपसर्गों और परीषहों को सह सकता है।
धर्मव्याख्यान क्यों, किसको और कैसे? - सूत्र १९६ के उत्तरार्ध में तीनों शंकाओं का समाधान किया गया है । वृत्तिकार ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा है - द्रव्यतः - प्राणिलोक पर दया व अनुकम्पा बुद्धिपूर्वक, क्षेत्रतः - पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर - इन चार दिशाओं और विदिशाओं के विभाग का भलीभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, कालतः - यावज्जीवन और, भावतः - समभावी निष्पक्ष - राग-द्वेष रहित होकर।
चूँकि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख चाहते हैं - इस बात को आत्मौपम्यदृष्टि से सदा तौलकर जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, उसे दूसरों के लिए न करे, इस आत्मधर्म को समझकर कहे। किन्तु विभाग करके कहे। यांनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से भेद करके आक्षेपणी आदि कथाविशेषों से या
पाइअसद्दमहण्णवो पृ०७२८ २. आचा० शीला० टीका पत्रांक २३१ के आधार पर
आचा० शीला० टीका पत्रांक २३२