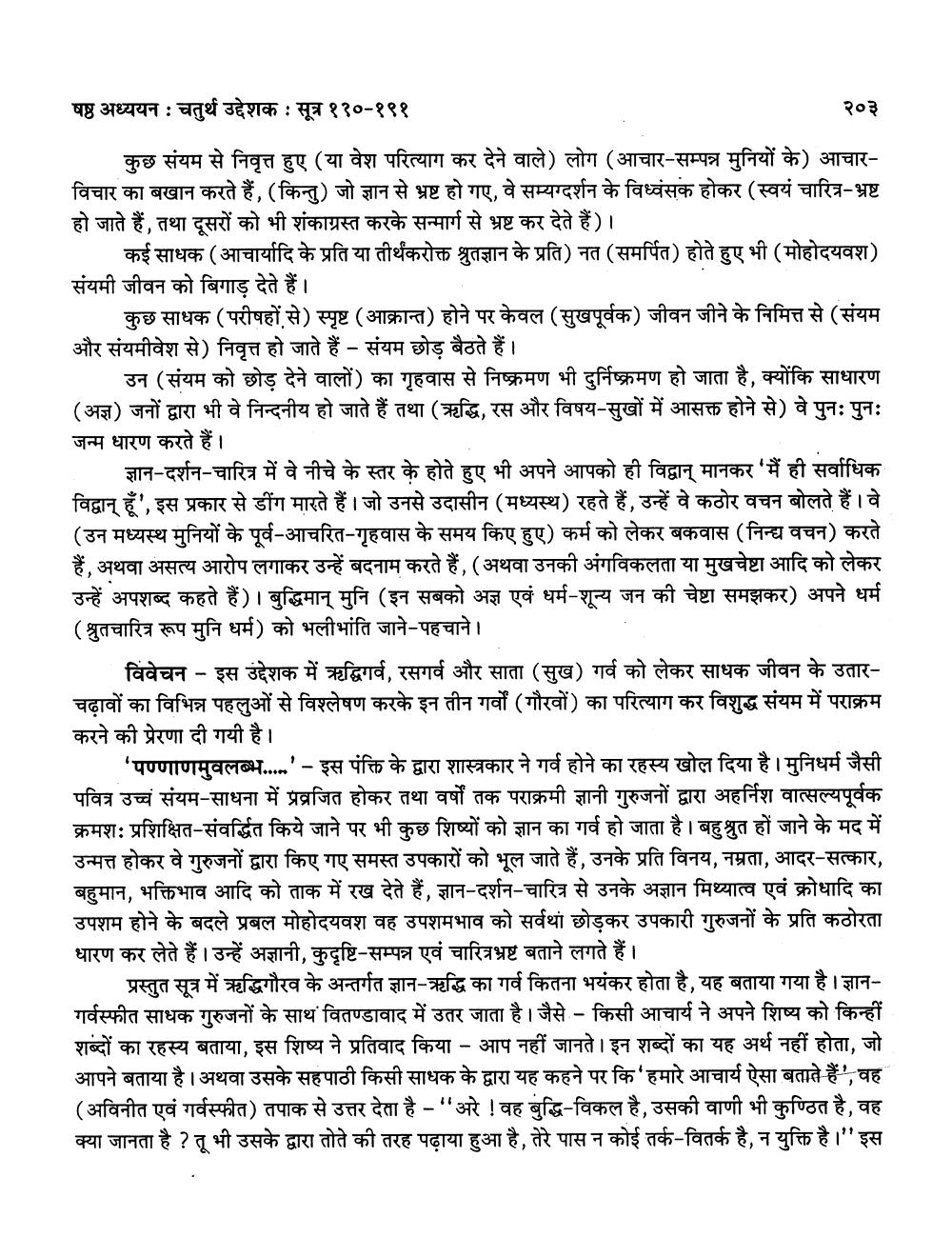________________
षष्ठ अध्ययन : चतुर्थ उद्देशक : सूत्र ११०-१९१
२०३
कुछ संयम से निवृत्त हुए (या वेश परित्याग कर देने वाले) लोग (आचार-सम्पन्न मुनियों के) आचारविचार का बखान करते हैं, (किन्तु) जो ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, वे सम्यग्दर्शन के विध्वंसक होकर (स्वयं चारित्र-भ्रष्ट हो जाते हैं, तथा दूसरों को भी शंकाग्रस्त करके सन्मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं)।
कई साधक (आचार्यादि के प्रति या तीर्थंकरोक्त श्रुतज्ञान के प्रति) नत (समर्पित) होते हुए भी (मोहोदयवश) संयमी जीवन को बिगाड़ देते हैं।
कुछ साधक (परीषहों से) स्पृष्ट (आक्रान्त) होने पर केवल (सुखपूर्वक) जीवन जीने के निमित्त से (संयम और संयमीवेश से) निवृत्त हो जाते हैं - संयम छोड़ बैठते हैं।
उन (संयम को छोड़ देने वालों) का गृहवास से निष्क्रमण भी दुर्निष्क्रमण हो जाता है, क्योंकि साधारण (अज्ञ) जनों द्वारा भी वे निन्दनीय हो जाते हैं तथा (ऋद्धि, रस और विषय-सुखों में आसक्त होने से) वे पुनः पुनः जन्म धारण करते हैं।
ज्ञान-दर्शन-चारित्र में वे नीचे के स्तर के होते हुए भी अपने आपको ही विद्वान् मानकर 'मैं ही सर्वाधिक विद्वान् हूँ', इस प्रकार से डींग मारते हैं। जो उनसे उदासीन (मध्यस्थ) रहते हैं, उन्हें वे कठोर वचन बोलते हैं । वे (उन मध्यस्थ मुनियों के पूर्व-आचरित-गृहवास के समय किए हुए) कर्म को लेकर बकवास (निन्द्य वचन) करते हैं, अथवा असत्य आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते हैं, (अथवा उनकी अंगविकलता या मुखचेष्टा आदि को लेकर उन्हें अपशब्द कहते हैं)। बुद्धिमान् मुनि (इन सबको अज्ञ एवं धर्म-शून्य जन की चेष्टा समझकर) अपने धर्म (श्रुतचारित्र रूप मुनि धर्म) को भलीभांति जाने-पहचाने।
विवेचन - इस उद्देशक में ऋद्धिगर्व, रसगर्व और साता (सुख) गर्व को लेकर साधक जीवन के उतारचढ़ावों का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करके इन तीन गौं (गौरवों) का परित्याग कर विशुद्ध संयम में पराक्रम करने की प्रेरणा दी गयी है।
'पण्णाणमुवलब्भ...' - इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने गर्व होने का रहस्य खोल दिया है। मुनिधर्म जैसी पवित्र उच्च संयम-साधना में प्रव्रजित होकर तथा वर्षों तक पराक्रमी ज्ञानी गुरुजनों द्वारा अहर्निश वात्सल्यपूर्वक क्रमशः प्रशिक्षित-संवर्द्धित किये जाने पर भी कुछ शिष्यों को ज्ञान का गर्व हो जाता है। बहुश्रुत हों जाने के मद में उन्मत्त होकर वे गुरुजनों द्वारा किए गए समस्त उपकारों को भूल जाते हैं, उनके प्रति विनय, नम्रता, आदर-सत्कार, बहुमान, भक्तिभाव आदि को ताक में रख देते हैं, ज्ञान-दर्शन-चारित्र से उनके अज्ञान मिथ्यात्व एवं क्रोधादि का उपशम होने के बदले प्रबल मोहोदयवश वह उपशमभाव को सर्वथा छोड़कर उपकारी गुरुजनों के प्रति कठोरता धारण कर लेते हैं। उन्हें अज्ञानी, कुदृष्टि-सम्पन्न एवं चारित्रभ्रष्ट बताने लगते हैं।
प्रस्तुत सूत्र में ऋद्धिगौरव के अन्तर्गत ज्ञान-ऋद्धि का गर्व कितना भयंकर होता है, यह बताया गया है। ज्ञानगर्वस्फीत साधक गुरुजनों के साथ वितण्डावाद में उतर जाता है। जैसे - किसी आचार्य ने अपने शिष्य को किन्हीं शब्दों का रहस्य बताया, इस शिष्य ने प्रतिवाद किया - आप नहीं जानते। इन शब्दों का यह अर्थ नहीं होता, जो आपने बताया है । अथवा उसके सहपाठी किसी साधक के द्वारा यह कहने पर कि हमारे आचार्य ऐसा बताते हैं, वह (अविनीत एवं गर्वस्फीत) तपाक से उत्तर देता है - "अरे ! वह बुद्धि-विकल है, उसकी वाणी भी कुण्ठित है, वह क्या जानता है ? तू भी उसके द्वारा तोते की तरह पढ़ाया हुआ है, तेरे पास न कोई तर्क-वितर्क है, न युक्ति है।" इस