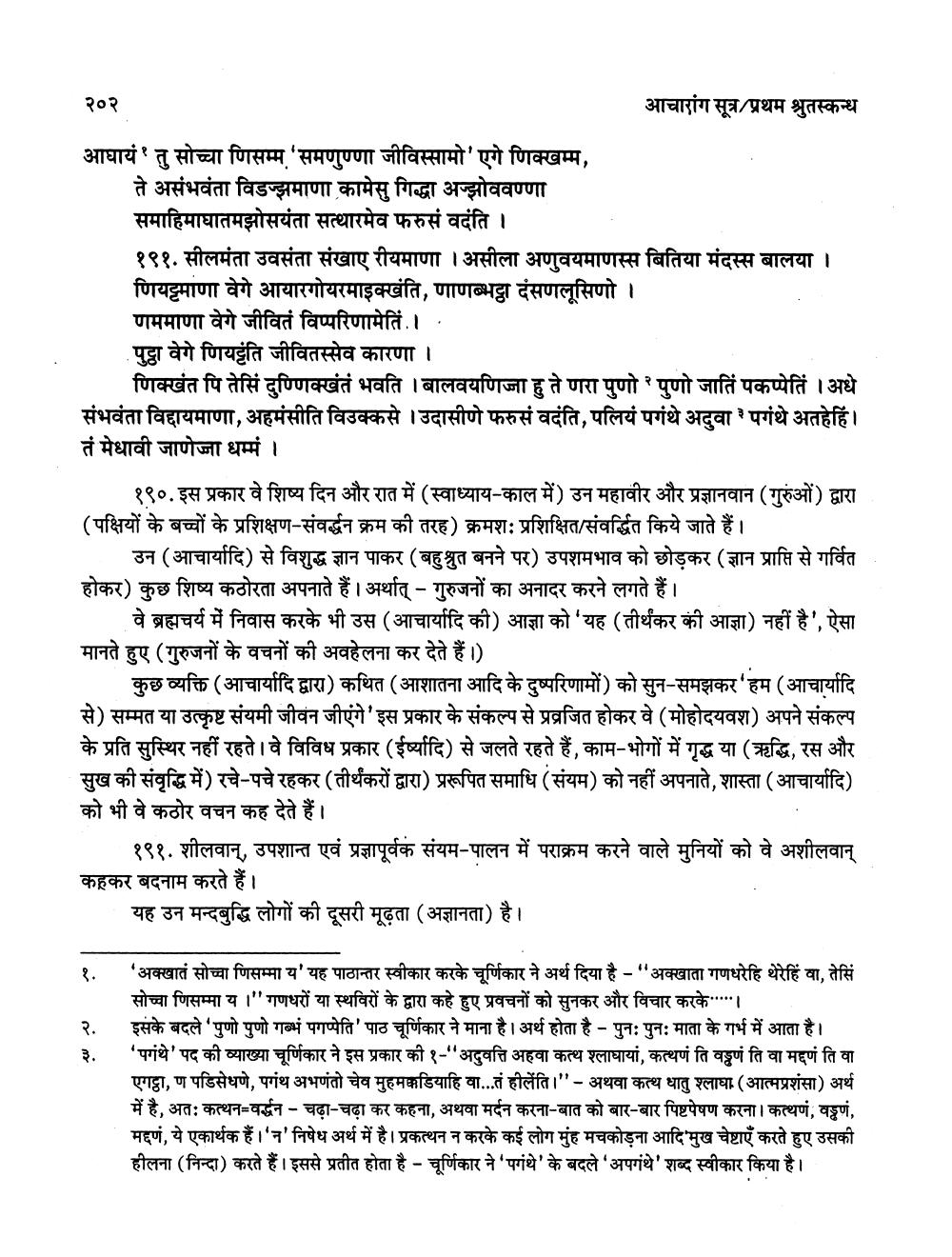________________
२०२
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध
आघायं तु सोच्चा णिसम्म 'समणुण्णा जीविस्सामो' एगे णिक्खम्म,
ते असंभवंता विडज्झमाणा कामेसु गिद्धा अज्झोववण्णा समाहिमाघातमझोसयंता सत्थारमेव फरुसं वदंति ।। १९१. सीलमंता उवसंता संखाए रीयमाणा । असीला अणुवयमाणस्स बितिया मंदस्स बालया। णियट्टमाणा वेगे आयारगोयरमाइक्खंति, णाणब्भट्ठा दंसणलूसिणो । णममाणा वेगे जीवितं विप्परिणामेतिं.। . पुट्ठा वेगे णियटृति जीवितस्सेव कारणा ।
णिक्खंत पि तेसिं दुण्णिक्खंतं भवति । बालवयणिज्जा हु ते णरा पुणो पुणो जातिं पकप्पेति । अधे संभवंता विद्दायमाणा, अहमंसीति विउक्कसे । उदासीणे फरुसंवदंति, पलियं पगंथे अदुवा पगंथे अतहेहिं। तं मेधावी जाणेज्जा धम्मं ।
१९०. इस प्रकार वे शिष्य दिन और रात में (स्वाध्याय-काल में) उन महावीर और प्रज्ञानवान (गुरुंओं) द्वारा (पक्षियों के बच्चों के प्रशिक्षण-संवर्द्धन क्रम की तरह) क्रमशः प्रशिक्षित/संवर्द्धित किये जाते हैं।
__उन (आचार्यादि) से विशुद्ध ज्ञान पाकर (बहुश्रुत बनने पर) उपशमभाव को छोड़कर (ज्ञान प्राप्ति से गर्वित होकर) कुछ शिष्य कठोरता अपनाते हैं । अर्थात् - गुरुजनों का अनादर करने लगते हैं।
वे ब्रह्मचर्य में निवास करके भी उस (आचार्यादि की) आज्ञा को 'यह (तीर्थंकर की आज्ञा) नहीं है', ऐसा मानते हुए (गुरुजनों के वचनों की अवहेलना कर देते हैं।)
कुछ व्यक्ति (आचार्यादि द्वारा) कथित (आशातना आदि के दुष्परिणामों) को सुन-समझकर हम (आचार्यादि से) सम्मत या उत्कृष्ट संयमी जीवन जीएंगे' इस प्रकार के संकल्प से प्रव्रजित होकर वे (मोहोदयवश) अपने संकल्प के प्रति सुस्थिर नहीं रहते। वे विविध प्रकार (ईर्ष्यादि) से जलते रहते हैं, काम-भोगों में गृद्ध या (ऋद्धि, रस और सुख की संवृद्धि में) रचे-पचे रहकर (तीर्थंकरों द्वारा) प्ररूपित समाधि (संयम) को नहीं अपनाते, शास्ता (आचार्यादि) को भी वे कठोर वचन कह देते हैं।
१९१. शीलवान्, उपशान्त एवं प्रज्ञापूर्वक संयम-पालन में पराक्रम करने वाले मुनियों को वे अशीलवान् कहकर बदनाम करते हैं। __यह उन मन्दबुद्धि लोगों की दूसरी मूढ़ता (अज्ञानता) है।
I an
sm
'अक्खातं सोच्चा णिसम्मा य' यह पाठान्तर स्वीकार करके चूर्णिकार ने अर्थ दिया है - "अक्खाता गणधरेहि थेरेहिं वा, तेसिं सोच्चा णिसम्मा य ।" गणधरों या स्थविरों के द्वारा कहे हुए प्रवचनों को सुनकर और विचार करके । इसके बदले 'पुणो पुणो गब्भं पगप्पेति' पाठ चूर्णिकार ने माना है। अर्थ होता है - पुनः पुनः माता के गर्भ में आता है। 'पगंथे' पद की व्याख्या चूर्णिकार ने इस प्रकार की १-"अदुवत्ति अहवा कत्थ श्लाघायां, कत्थणं ति वड्डणं ति वा मद्दणं ति वा एगट्ठा, ण पडिसेधणे, पगंथ अभणंतो चेव मुहमक्कडियाहि वा...तं हीलेंति।" - अथवा कत्थ धातु श्लाघा (आत्मप्रशंसा) अर्थ में है, अतः कत्थन-वर्द्धन - चढ़ा-चढ़ा कर कहना, अथवा मर्दन करना-बात को बार-बार पिष्टपेषण करना। कत्थणं, वणं, मद्दणं, ये एकार्थक हैं। 'न' निषेध अर्थ में है। प्रकत्थन न करके कई लोग मुंह मचकोड़ना आदि मुख चेष्टाएँ करते हुए उसकी हीलना (निन्दा) करते हैं। इससे प्रतीत होता है - चूर्णिकार ने 'पगंथे' के बदले 'अपगंथे' शब्द स्वीकार किया है।