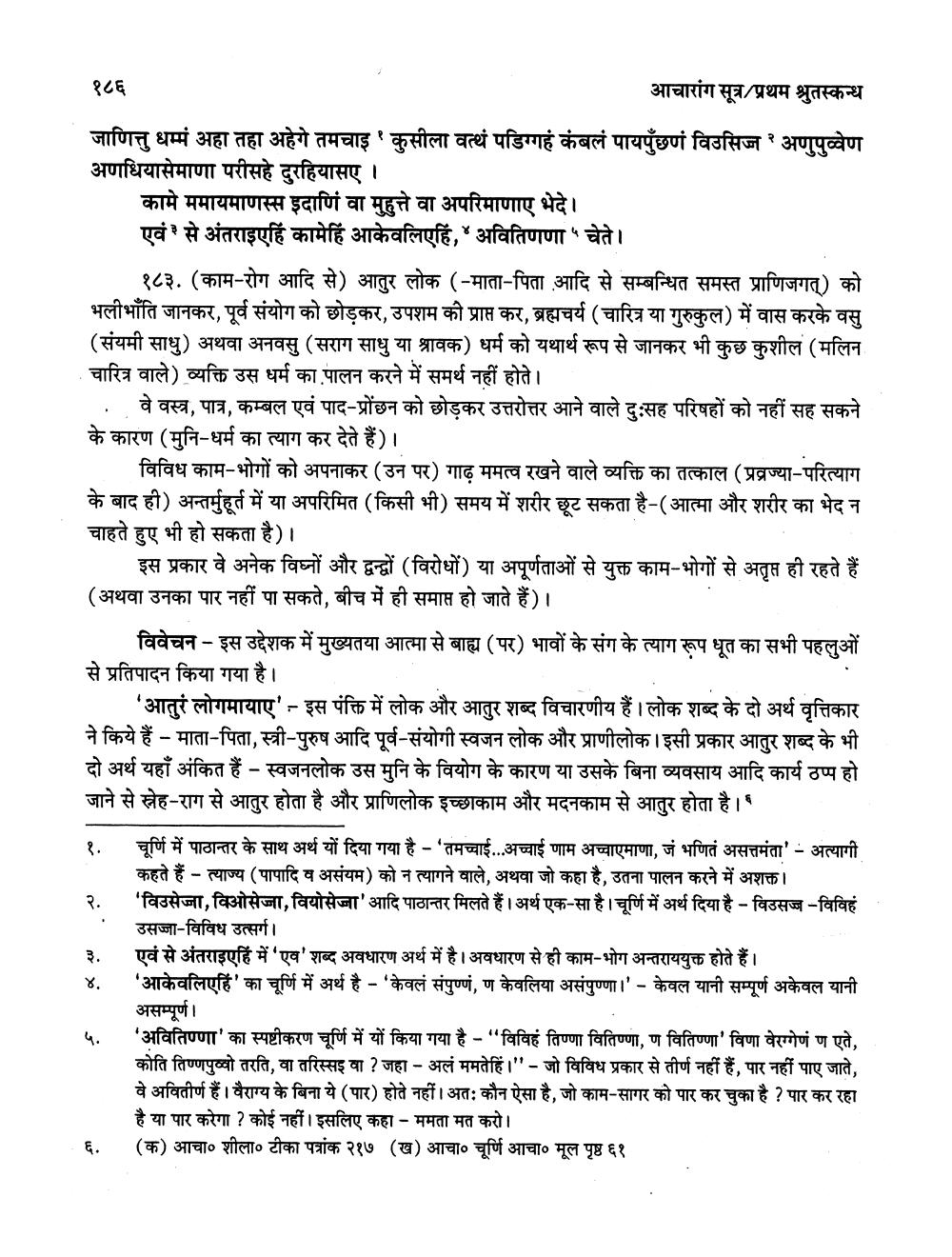________________
१८६
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध जाणित्तु धम्मं अहा तहा अहेगे तमचाइ ' कुसीला वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं विउसिज २ अणुपुव्वेण अणधियासेमाणा परीसहे दुरहियासए ।
कामे ममायमाणस्स इदाणिं वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे। एवं से अंतराइएहिं कामेहिं आकेवलिएहिं, अवितिणणा ५ चेते।
१८३. (काम-रोग आदि से) आतुर लोक (-माता-पिता आदि से सम्बन्धित समस्त प्राणिजगत्) को भलीभाँति जानकर, पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर, ब्रह्मचर्य (चारित्र या गुरुकुल) में वास करके वसु (संयमी साधु) अथवा अनवसु (सराग साधु या श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील (मलिन चारित्र वाले) व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते। . वे वस्त्र, पात्र, कम्बल एवं पाद-प्रोंछन को छोड़कर उत्तरोत्तर आने वाले दुःसह परिषहों को नहीं सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते हैं)।
विविध काम-भोगों को अपनाकर (उन पर) गाढ़ ममत्व रखने वाले व्यक्ति का तत्काल (प्रव्रज्या-परित्याग के बाद ही) अन्तर्मुहूर्त में या अपरिमित (किसी भी) समय में शरीर छूट सकता है-(आत्मा और शरीर का भेद न चाहते हुए भी हो सकता है)।
इस प्रकार वे अनेक विघ्नों और द्वन्द्वों (विरोधों) या अपूर्णताओं से युक्त काम-भोगों से अतृप्त ही रहते हैं (अथवा उनका पार नहीं पा सकते, बीच में ही समाप्त हो जाते हैं)।
विवेचन - इस उद्देशक में मुख्यतया आत्मा से बाह्य (पर) भावों के संग के त्याग रूप धूत का सभी पहलुओं से प्रतिपादन किया गया है।
'आतुरं लोगमायाए' - इस पंक्ति में लोक और आतुर शब्द विचारणीय हैं । लोक शब्द के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं - माता-पिता, स्त्री-पुरुष आदि पूर्व-संयोगी स्वजन लोक और प्राणीलोक । इसी प्रकार आतुर शब्द के भी दो अर्थ यहाँ अंकित हैं - स्वजनलोक उस मुनि के वियोग के कारण या उसके बिना व्यवसाय आदि कार्य ठप्प हो जाने से स्नेह-राग से आतुर होता है और प्राणिलोक इच्छाकाम और मदनकाम से आतुर होता है।
चूर्णि में पाठान्तर के साथ अर्थ यों दिया गया है - 'तमच्चाई...अच्चाई णाम अच्चाएमाणा, जं भणितं असत्तमंता' - अत्यागी कहते हैं - त्याज्य (पापादि व असंयम) को न त्यागने वाले, अथवा जो कहा है, उतना पालन करने में अशक्त। 'विउसेजा,विओसेज्जा, वियोसेज्जा' आदि पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ एक-सा है। चूर्णि में अर्थ दिया है - विउसज्ज -विविहं उसज्जा-विविध उत्सर्ग। एवं से अंतराइएहिं में 'एव' शब्द अवधारण अर्थ में है। अवधारण से ही काम-भोग अन्तराययुक्त होते हैं। 'आकेवलिएहिं' का चूर्णि में अर्थ है - 'केवलं संपुण्णं, ण केवलिया असंपुण्णा।' - केवल यानी सम्पूर्ण अकेवल यानी असम्पूर्ण। 'अवितिण्णा' का स्पष्टीकरण चूर्णि में यों किया गया है - "विविहं तिण्णा वितिण्णा, ण वितिण्णा' विणा वेरग्गेणं ण एते, कोति तिण्णपुव्वो तरति, वा तरिस्सइ वा? जहा - अलं ममतेहिं।" - जो विविध प्रकार से तीर्ण नहीं हैं, पार नहीं पाए जाते, वे अवितीर्ण हैं। वैराग्य के बिना ये (पार) होते नहीं। अतः कौन ऐसा है, जो काम-सागर को पार कर चुका है ? पार कर रहा है या पार करेगा? कोई नहीं। इसलिए कहा - ममता मत करो। (क) आचा० शीला० टीका पत्रांक २१७ (ख) आचा० चूर्णि आचा० मूल पृष्ठ ६१
६.