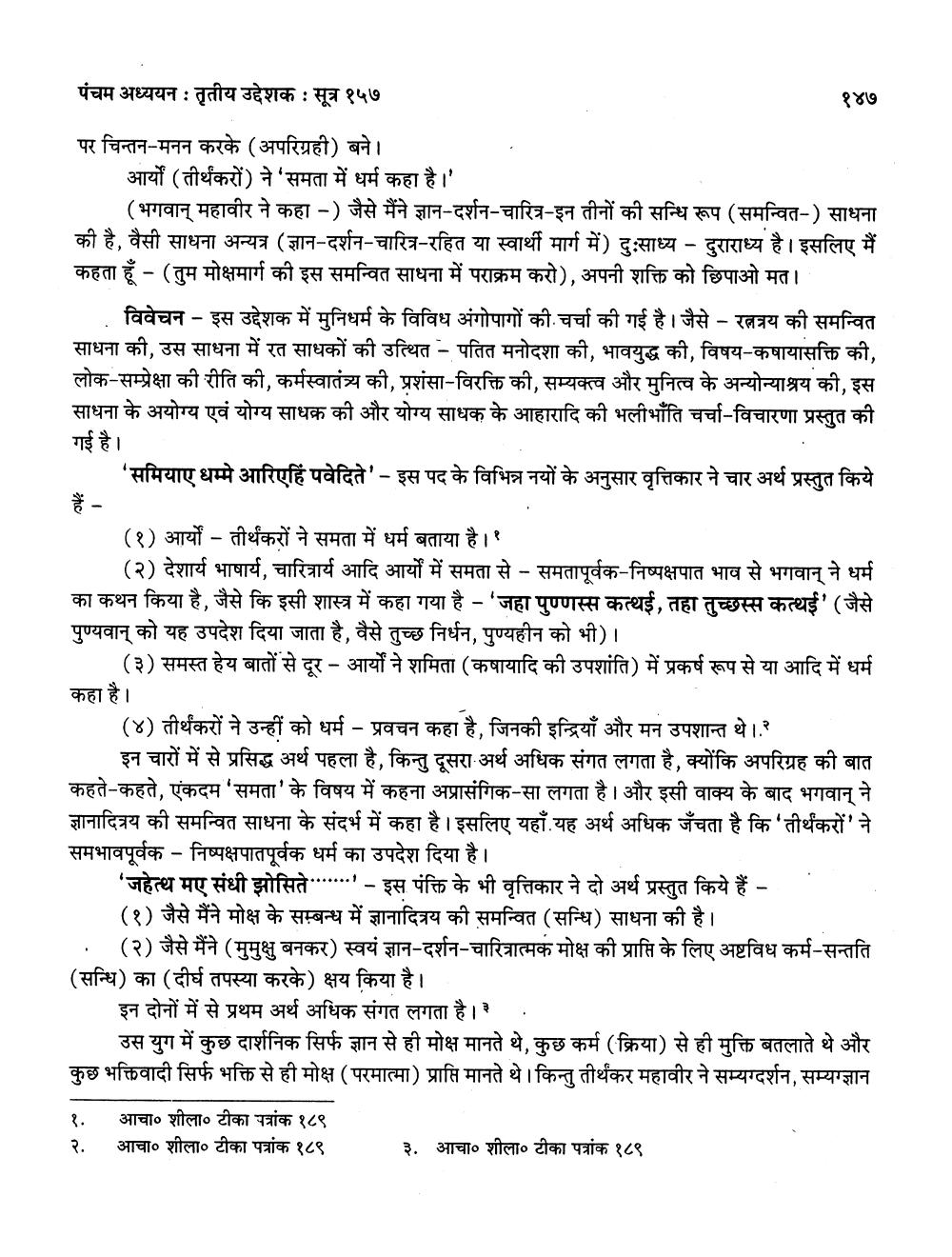________________
पंचम अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सूत्र १५७
१४७
पर चिन्तन-मनन करके (अपरिग्रही) बने।
आर्यों (तीर्थंकरों) ने 'समता में धर्म कहा है।' __(भगवान् महावीर ने कहा -) जैसे मैंने ज्ञान-दर्शन-चारित्र-इन तीनों की सन्धि रूप (समन्वित-) साधना की है, वैसी साधना अन्यत्र (ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रहित या स्वार्थी मार्ग में) दुःसाध्य - दुराराध्य है। इसलिए मैं कहता हूँ - (तुम मोक्षमार्ग की इस समन्वित साधना में पराक्रम करो), अपनी शक्ति को छिपाओ मत।
विवेचन - इस उद्देशक में मुनिधर्म के विविध अंगोपागों की चर्चा की गई है। जैसे - रत्नत्रय की समन्वित साधना की, उस साधना में रत साधकों की उत्थित - पतित मनोदशा की, भावयुद्ध की, विषय-कषायासक्ति की, लोक-सम्प्रेक्षा की रीति की, कर्मस्वातंत्र्य की, प्रशंसा-विरक्ति की, सम्यक्त्व और मुनित्व के अन्योन्याश्रय की, इस साधना के अयोग्य एवं योग्य साधक की और योग्य साधक के आहारादि की भलीभाँति चर्चा-विचारणा प्रस्तुत की गई है।
समियाए धम्मे आरिएहिं पवेदिते' - इस पद के विभिन्न नयों के अनुसार वृत्तिकार ने चार अर्थ प्रस्तुत किये
(१) आर्यों - तीर्थंकरों ने समता में धर्म बताया है।'
(२) देशार्य भाषार्य, चारित्रार्य आदि आर्यों में समता से - समतापूर्वक-निष्पक्षपात भाव से भगवान् ने धर्म का कथन किया है, जैसे कि इसी शास्त्र में कहा गया है - 'जहा पुण्णस्स कत्थई, तहा तुच्छस्स कत्थई' (जैसे पुण्यवान् को यह उपदेश दिया जाता है, वैसे तुच्छ निर्धन, पुण्यहीन को भी)।
(३) समस्त हेय बातों से दूर - आर्यों ने शमिता (कषायादि की उपशांति) में प्रकर्ष रूप से या आदि में धर्म कहा है।
(४) तीर्थंकरों ने उन्हीं को धर्म - प्रवचन कहा है, जिनकी इन्द्रियाँ और मन उपशान्त थे।.२
इन चारों में से प्रसिद्ध अर्थ पहला है, किन्तु दूसरा अर्थ अधिक संगत लगता है, क्योंकि अपरिग्रह की बात कहते-कहते, एकदम 'समता' के विषय में कहना अप्रासंगिक-सा लगता है। और इसी वाक्य के बाद भगवान् ने ज्ञानादित्रय की समन्वित साधना के संदर्भ में कहा है। इसलिए यहाँ.यह अर्थ अधिक ऊंचता है कि 'तीर्थंकरों' ने समभावपूर्वक - निष्पक्षपातपूर्वक धर्म का उपदेश दिया है।
'जहेत्थ मए संधी झोसिते.......' - इस पंक्ति के भी वृत्तिकार ने दो अर्थ प्रस्तुत किये हैं -
(१) जैसे मैंने मोक्ष के सम्बन्ध में ज्ञानादित्रय की समन्वित (सन्धि) साधना की है। . (२) जैसे मैंने (मुमुक्षु बनकर) स्वयं ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टविध कर्म-सन्तति (सन्धि) का (दीर्घ तपस्या करके) क्षय किया है।
इन दोनों में से प्रथम अर्थ अधिक संगत लगता है। ३ .
उस युग में कुछ दार्शनिक सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मानते थे, कुछ कर्म (क्रिया) से ही मुक्ति बतलाते थे और कुछ भक्तिवादी सिर्फ भक्ति से ही मोक्ष (परमात्मा) प्राप्ति मानते थे। किन्तु तीर्थंकर महावीर ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
१.
आचा० शीला० टीका पत्रांक १८९ आचा० शीला० टीका पत्रांक १८९
३. आचा० शीला० टीका पत्रांक १८९