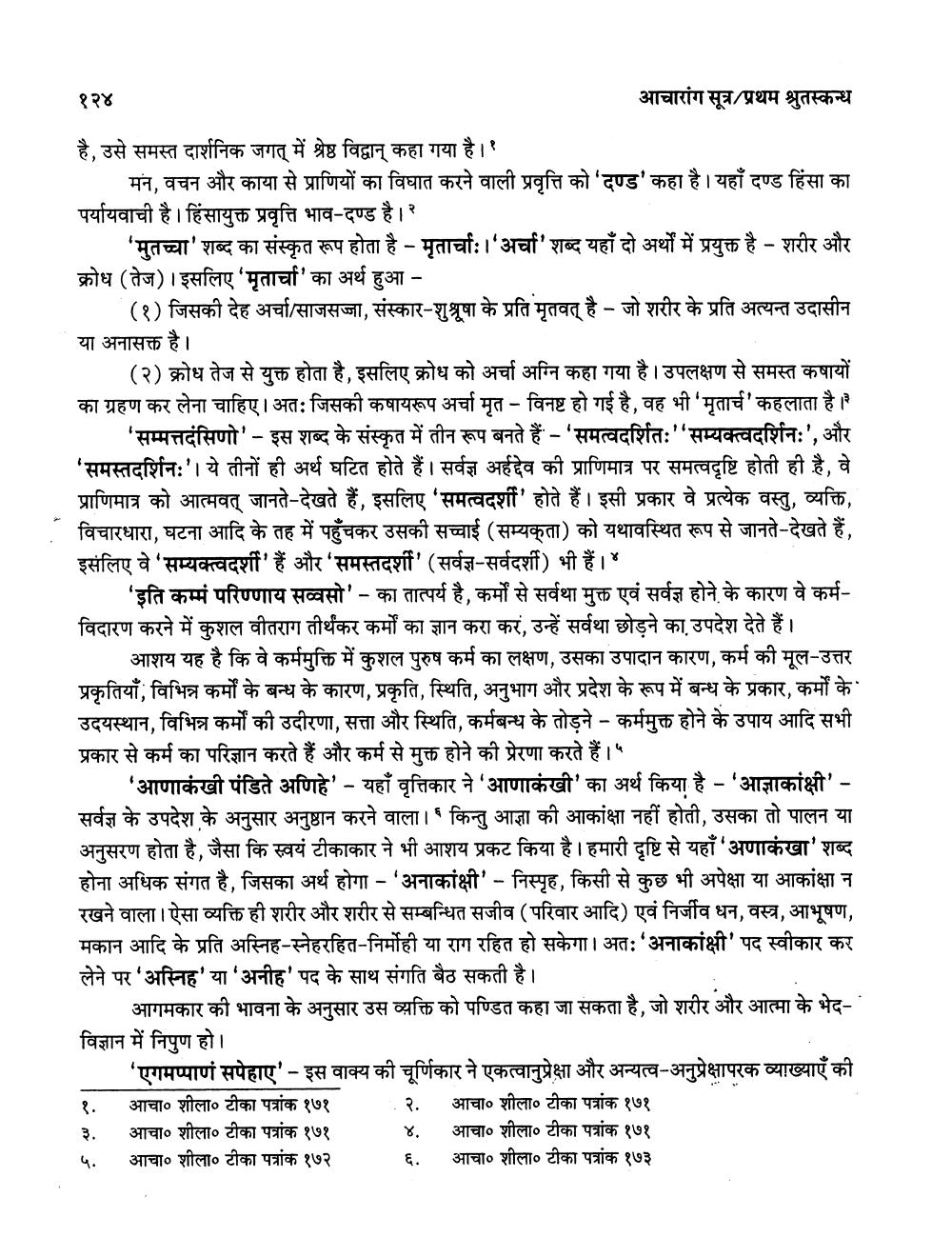________________
१२४
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध है, उसे समस्त दार्शनिक जगत् में श्रेष्ठ विद्वान् कहा गया है।' ___मन, वचन और काया से प्राणियों का विघात करने वाली प्रवृत्ति को 'दण्ड' कहा है। यहाँ दण्ड हिंसा का पर्यायवाची है। हिंसायुक्त प्रवृत्ति भाव-दण्ड है। २ ____ 'मुतच्चा' शब्द का संस्कृत रूप होता है - मृतार्चाः। अर्चा' शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त है - शरीर और क्रोध (तेज)। इसलिए 'मृतार्चा' का अर्थ हुआ -
(१) जिसकी देह अर्चा/साजसज्जा, संस्कार-शुश्रूषा के प्रति मृतवत् है - जो शरीर के प्रति अत्यन्त उदासीन या अनासक्त है।
(२) क्रोध तेज से युक्त होता है, इसलिए क्रोध को अर्चा अग्नि कहा गया है। उपलक्षण से समस्त कषायों का ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः जिसकी कषायरूप अर्चा मृत - विनष्ट हो गई है, वह भी 'मृतार्च' कहलाता है।
___'सम्मत्तदंसिणो' - इस शब्द के संस्कृत में तीन रूप बनते हैं - 'समत्वदर्शितः''सम्यक्त्वदर्शिनः', और 'समस्तदर्शिनः'। ये तीनों ही अर्थ घटित होते हैं। सर्वज्ञ अर्हदेव की प्राणिमात्र पर समत्वदृष्टि होती ही है, वे प्राणिमात्र को आत्मवत् जानते-देखते हैं, इसलिए 'समत्वदर्शी' होते हैं। इसी प्रकार वे प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, घटना आदि के तह में पहुँचकर उसकी सच्चाई (सम्यक्ता) को यथावस्थित रूप से जानते-देखते हैं, इसलिए वे 'सम्यक्त्वदर्शी' हैं और 'समस्तदर्शी' (सर्वज्ञ-सर्वदर्शी) भी हैं।
_ 'इति कम्मं परिण्णाय सव्वसो' - का तात्पर्य है, कर्मों से सर्वथा मुक्त एवं सर्वज्ञ होने के कारण वे कर्मविदारण करने में कुशल वीतराग तीर्थंकर कर्मों का ज्ञान करा कर, उन्हें सर्वथा छोड़ने का उपदेश देते हैं। ___आशय यह है कि वे कर्ममुक्ति में कुशल पुरुष कर्म का लक्षण, उसका उपादान कारण, कर्म की मूल-उत्तर प्रकृतियाँ, विभिन्न कर्मों के बन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के रूप में बन्ध के प्रकार, कर्मों के उदयस्थान, विभिन्न कर्मों की उदीरणा, सत्ता और स्थिति, कर्मबन्ध के तोड़ने - कर्ममुक्त होने के उपाय आदि सभी प्रकार से कर्म का परिज्ञान करते हैं और कर्म से मुक्त होने की प्रेरणा करते हैं। ५
___'आणाकंखी पंडिते अणिहे' - यहाँ वृत्तिकार ने 'आणाकंखी' का अर्थ किया है - 'आज्ञाकांक्षी' - सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करने वाला। किन्तु आज्ञा की आकांक्षा नहीं होती, उसका तो पालन या अनुसरण होता है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने भी आशय प्रकट किया है। हमारी दृष्टि से यहाँ 'अणाकंखा' शब्द होना अधिक संगत है, जिसका अर्थ होगा - 'अनाकांक्षी' - निस्पृह, किसी से कुछ भी अपेक्षा या आकांक्षा न रखने वाला। ऐसा व्यक्ति ही शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव (परिवार आदि) एवं निर्जीव धन, वस्त्र, आभूषण, मकान आदि के प्रति अस्निह-स्नेहरहित-निर्मोही या राग रहित हो सकेगा। अतः 'अनाकांक्षी' पद स्वीकार कर लेने पर 'अस्निह' या 'अनीह' पद के साथ संगति बैठ सकती है।
आगमकार की भावना के अनुसार उस व्यक्ति को पण्डित कहा जा सकता है, जो शरीर और आत्मा के भेदविज्ञान में निपुण हो।
'एगमप्पाणं सपेहाए' - इस वाक्य की चूर्णिकार ने एकत्वानुप्रेक्षा और अन्यत्व-अनुप्रेक्षापरक व्याख्याएँ की आचा० शीला० टीका पत्रांक १७१
__ आचा० शीला० टीका पत्रांक १७१ ३. आचा० शीला० टीका पत्रांक १७१
आचा० शीला० टीका पत्रांक १७१ आचा० शीला० टीका पत्रांक १७२
आचा० शीला० टीका पत्रांक १७३
&