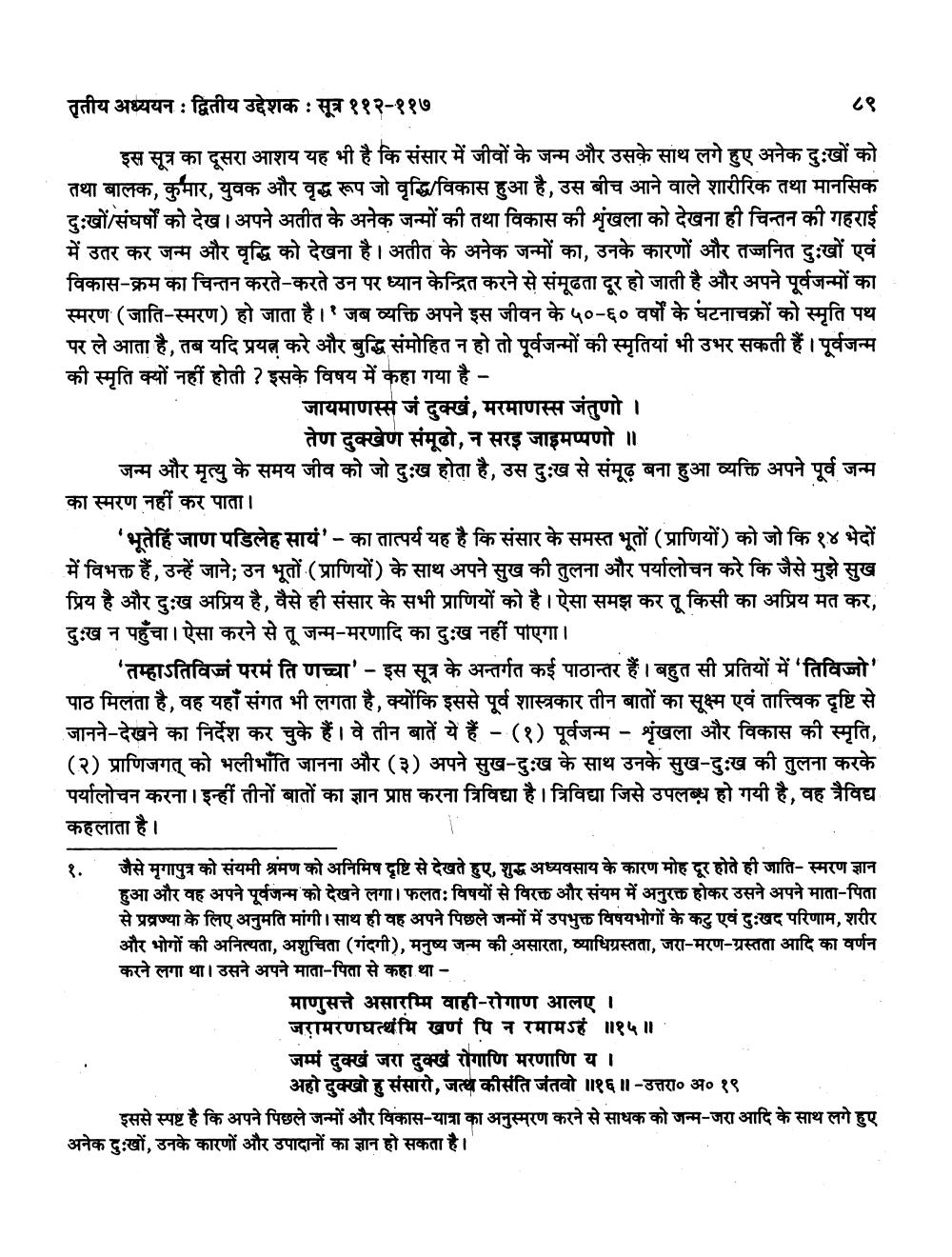________________
तृतीय अध्ययन : द्वितीय उद्देशक : सूत्र ११२-११७
इस सूत्र का दूसरा आशय यह भी है कि संसार में जीवों के जन्म और उसके साथ लगे हुए अनेक दुःखों को तथा बालक, कुमार, युवक और वृद्ध रूप जो वृद्धि/विकास हुआ है, उस बीच आने वाले शारीरिक तथा मानसिक दुःखों/संघर्षों को देख। अपने अतीत के अनेक जन्मों की तथा विकास की श्रृंखला को देखना ही चिन्तन की गहराई में उतर कर जन्म और वृद्धि को देखना है। अतीत के अनेक जन्मों का, उनके कारणों और तजनित दुःखों एवं विकास-क्रम का चिन्तन करते-करते उन पर ध्यान केन्द्रित करने से संमूढता दूर हो जाती है और अपने पूर्वजन्मों का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है। जब व्यक्ति अपने इस जीवन के ५०-६० वर्षों के घंटनाचक्रों को स्मृति पथ पर ले आता है, तब यदि प्रयत्न करे और बुद्धि संमोहित न हो तो पूर्वजन्मों की स्मृतियां भी उभर सकती हैं। पूर्वजन्म की स्मृति क्यों नहीं होती ? इसके विषय में कहा गया है -
जायमाणस्स जं दुक्खं, मरमाणस्स जंतुणो ।
तेण दुक्खेण संमूढो, न सरइ जाइमप्पणो ॥ जन्म और मृत्यु के समय जीव को जो दुःख होता है, उस दुःख से संमूढ़ बना हुआ व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं कर पाता।
'भूतेहिं जाण पडिलेह सायं' - का तात्पर्य यह है कि संसार के समस्त भूतों (प्राणियों) को जो कि १४ भेदों में विभक्त हैं, उन्हें जाने; उन भूतों (प्राणियों) के साथ अपने सुख की तुलना और पर्यालोचन करे कि जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को है। ऐसा समझ कर तू किसी का अप्रिय मत कर, दुःख न पहुँचा। ऐसा करने से तू जन्म-मरणादि का दुःख नहीं पाएगा।
'तम्हाऽतिविजं परमं ति णच्चा' - इस सूत्र के अन्तर्गत कई पाठान्तर हैं। बहुत सी प्रतियों में 'तिविजो' पाठ मिलता है, वह यहाँ संगत भी लगता है, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रकार तीन बातों का सूक्ष्म एवं तात्त्विक दृष्टि से जानने-देखने का निर्देश कर चुके हैं। वे तीन बातें ये हैं - (१) पूर्वजन्म - श्रृंखला और विकास की स्मृति, (२) प्राणिजगत् को भलीभाँति जानना और (३) अपने सुख-दुःख के साथ उनके सुख-दुःख की तुलना करके पर्यालोचन करना। इन्हीं तीनों बातों का ज्ञान प्राप्त करना त्रिविद्या है । त्रिविद्या जिसे उपलब्ध हो गयी है, वह विद्य कहलाता है।
जैसे मृगापुत्र को संयमी श्रमण को अनिमिष दृष्टि से देखते हुए, शुद्ध अध्यवसाय के कारण मोह दूर होते ही जाति-स्मरण ज्ञान हुआ और वह अपने पूर्वजन्म को देखने लगा। फलतः विषयों से विरक्त और संयम में अनुरक्त होकर उसने अपने माता-पिता से प्रव्रज्या के लिए अनुमति मांगी। साथ ही वह अपने पिछले जन्मों में उपभुक्त विषयभोगों के कटु एवं दुःखद परिणाम, शरीर और भोगों की अनित्यता, अशुचिता (गंदगी), मनुष्य जन्म की असारता, व्याधिग्रस्तता, जरा-मरण-ग्रस्तता आदि का वर्णन करने लगा था। उसने अपने माता-पिता से कहा था -
माणुसत्ते असारम्मि वाही-रोगाण आलए । जरामरणपत्थंमि खणं पिन रमामऽहं ॥१५॥ जम्मं दक्खं जरा दक्खं रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥१६॥-उत्तरा० अ० १९ इससे स्पष्ट है कि अपने पिछले जन्मों और विकास-यात्रा का अनुस्मरण करने से साधक को जन्म-जरा आदि के साथ लगे हुए अनेक दुःखों, उनके कारणों और उपादानों का ज्ञान हो सकता है।