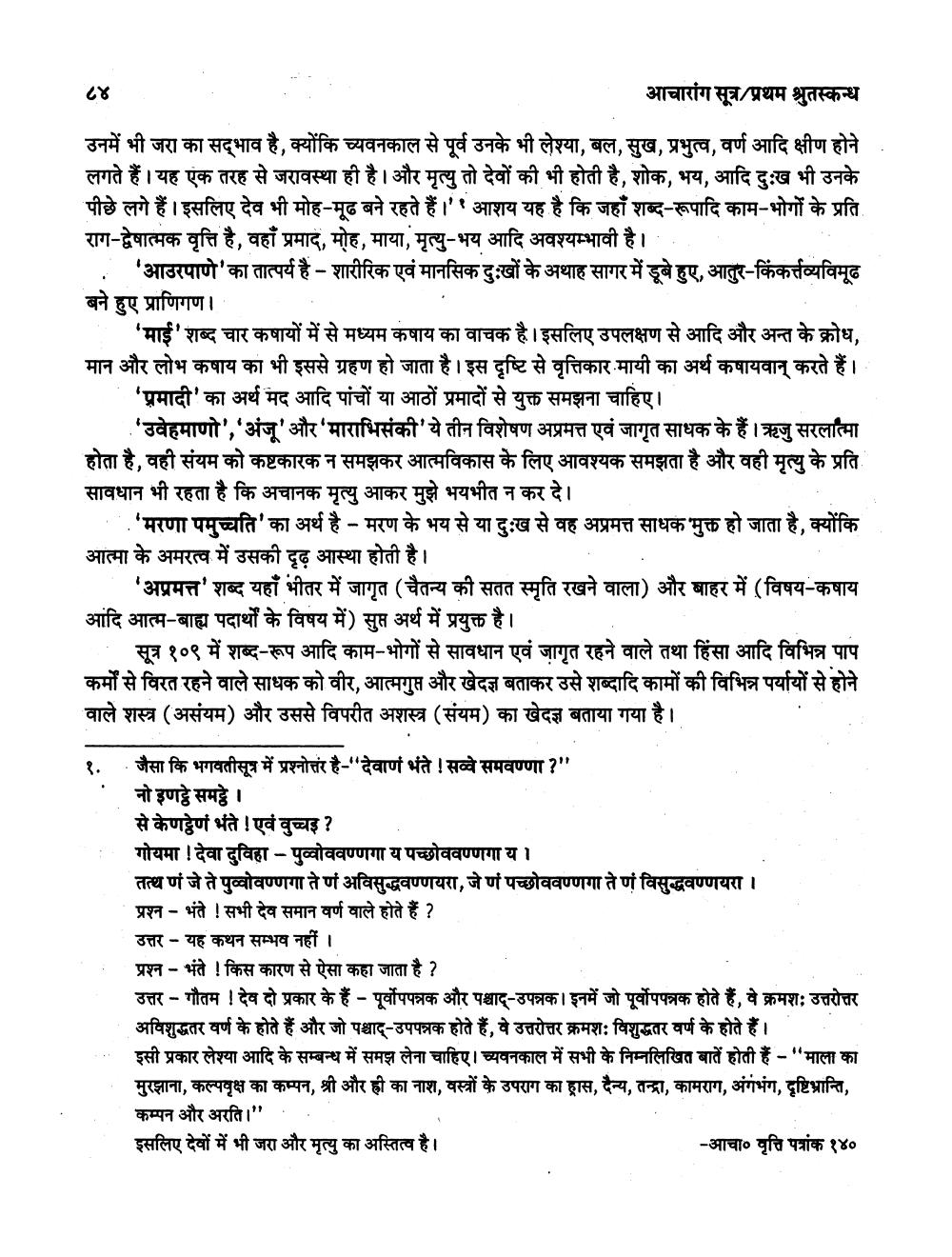________________
८४
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध उनमें भी जरा का सद्भाव है, क्योंकि च्यवनकाल से पूर्व उनके भी लेश्या, बल, सुख, प्रभुत्व, वर्ण आदि क्षीण होने लगते हैं। यह एक तरह से जरावस्था ही है। और मृत्यु तो देवों की भी होती है, शोक, भय, आदि दुःख भी उनके पीछे लगे हैं। इसलिए देव भी मोह-मूढ बने रहते हैं।'' आशय यह है कि जहाँ शब्द-रूपादि काम-भोगों के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वहाँ प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि अवश्यम्भावी है।
. 'आउरपाणे' का तात्पर्य है - शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के अथाह सागर में डूबे हुए, आतुर-किंकर्तव्यविमूढ बने हुए प्राणिगण।
'माई' शब्द चार कषायों में से मध्यम कषाय का वाचक है। इसलिए उपलक्षण से आदि और अन्त के क्रोध, मान और लोभ कषाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि से वृत्तिकार मायी का अर्थ कषायवान् करते हैं। - 'प्रमादी' का अर्थ मद आदि पांचों या आठों प्रमादों से युक्त समझना चाहिए।
'उवेहमाणो', अंजू' और 'माराभिसंकी' ये तीन विशेषण अप्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। ऋजु सरलात्मा होता है, वही संयम को कष्टकारक न समझकर आत्मविकास के लिए आवश्यक समझता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अचानक मृत्यु आकर मुझे भयभीत न कर दे।
..'मरणा पमुच्चति' का अर्थ है - मरण के भय से या दुःख से वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अमरत्व में उसकी दृढ़ आस्था होती है।
- 'अप्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर में (विषय-कषाय आदि आत्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) सुप्त अर्थ में प्रयुक्त है।
- सूत्र १०९ में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिंसा आदि विभिन्न पाप कर्मों से विरत रहने वाले साधक को वीर, आत्मगुप्त और खेदज्ञ बताकर उसे शब्दादि कामों की विभिन्न पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असंयम) और उससे विपरीत अशस्त्र (संयम) का खेदज्ञ बताया गया है। १. . जैसा कि भगवतीसूत्र में प्रश्नोत्तर है-"देवाणं भंते ! सव्वे समवण्णा?"
नो इणढे समढे। से केणटेणं भंते ! एवं वुच्चइ ? गोयमा ! देवा दुविहा-पुव्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगाय। तत्थ णं जे ते पुव्वोवण्णगा ते णं अविसुद्धवण्णयरा,जेणं पच्छोववण्णगा ते णं विसुद्धवण्णयरा । प्रश्न - भंते ! सभी देव समान वर्ण वाले होते हैं ? उत्तर - यह कथन सम्भव नहीं । प्रश्न - भंते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? उत्तर - गौतम ! देव दो प्रकार के हैं - पूर्वोपपन्नक और पश्चाद्-उपन्नक। इनमें जो पूर्वोपपत्रक होते हैं, वे क्रमश: उत्तरोत्तर
अविशद्धतर वर्ण के होते हैं और जो पश्चाद-उपपन्नक होते हैं, वे उत्तरोत्तर क्रमशः विशद्धतर वर्ण के होते हैं। ... इसी प्रकार लेश्या आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। च्यवनकाल में सभी के निम्नलिखित बातें होती हैं - "माला का
मुरझाना, कल्पवृक्ष का कम्पन, श्री और ह्री का नाश, वस्त्रों के उपराग का ह्रास, दैन्य, तन्द्रा, कामराग, अंगभंग, दृष्टिभ्रान्ति, कम्पन और अरति।" .. इसलिए देवों में भी जरा और मृत्यु का अस्तित्व है।
-आचा० वृत्ति पत्रांक १४०